 Duration: Feb 18, 2024 - Dec 31, 2024
Duration: Feb 18, 2024 - Dec 31, 2024
Validity: Till the Exam
Live Lectures
Counselling and guidance at offline centers
One to One telephonic mentorship
Seminars / Topper's Talk at offline center
कैंसर जीनोमिक्स
कैंसर के इलाज से संबंधित सरकारी पहल
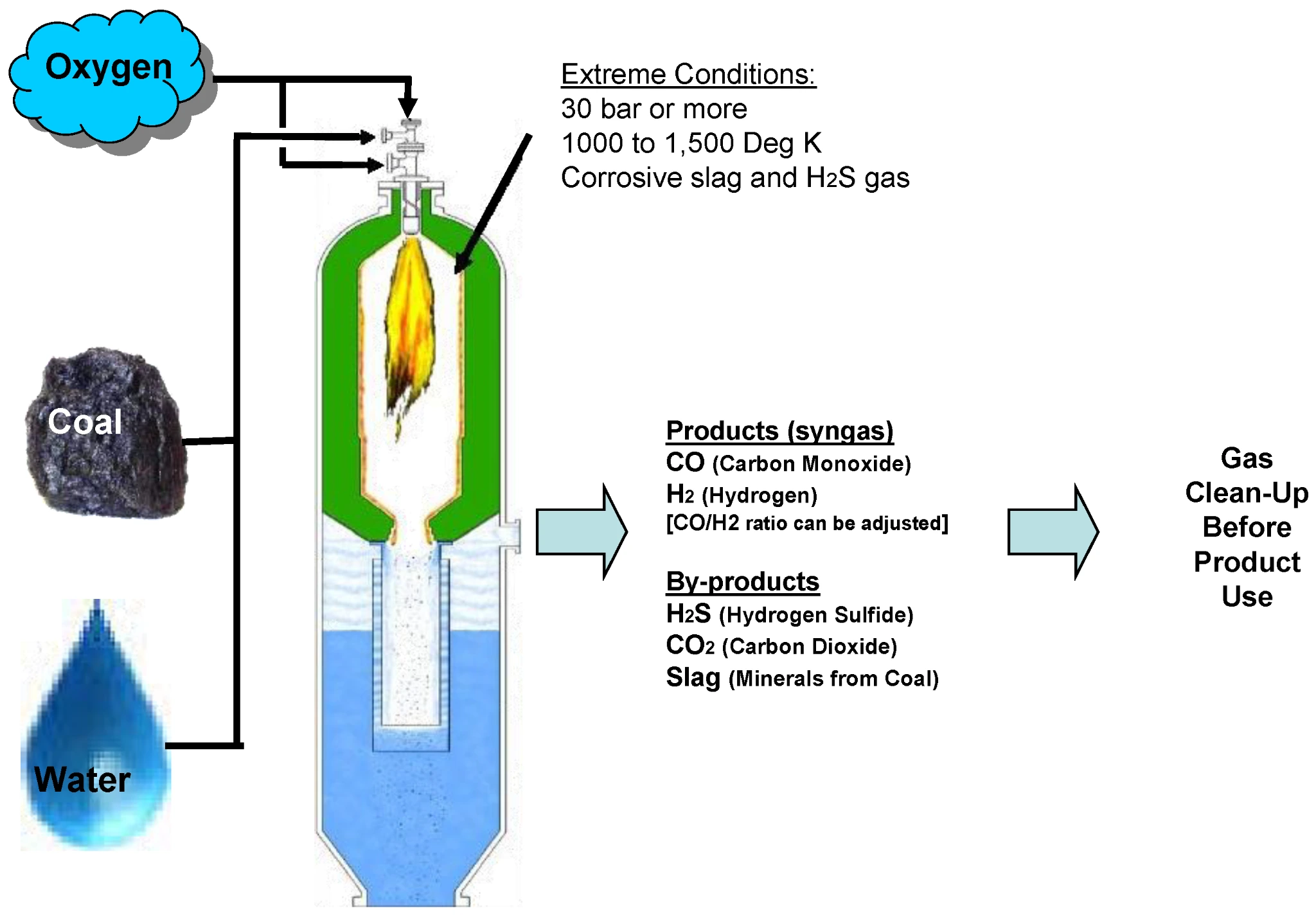
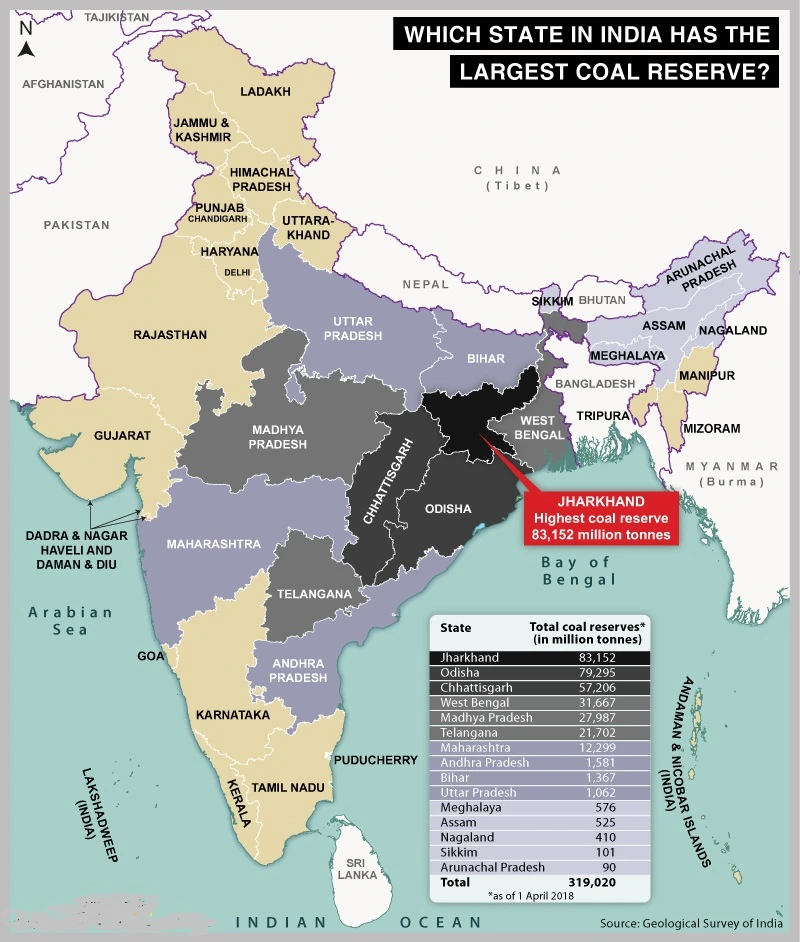 कोयला गैसीकरण क्या है?
कोयला गैसीकरण क्या है?
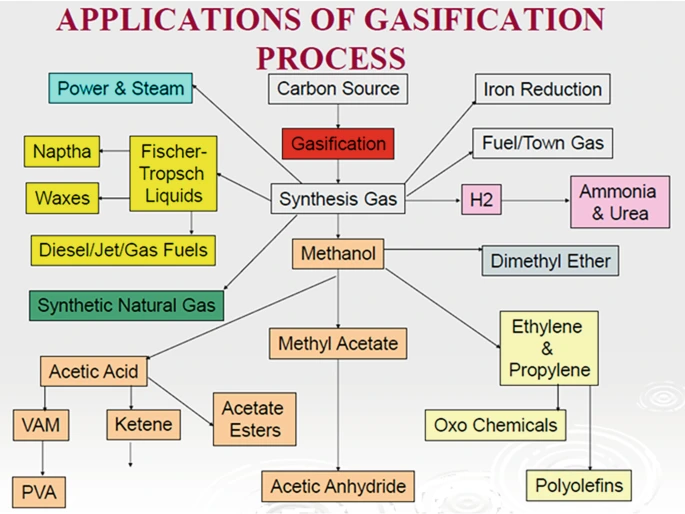 कोयला गैसीकरण की आवश्यकता
कोयला गैसीकरण की आवश्यकता

![]() MPSC Rajyaseva Prelims Full Length Test Series 2024
MPSC Rajyaseva Prelims Full Length Test Series 2024
Hinglish
299
499
((For Full Batch))
![]() 40% OFF
40% OFF
<div class="new-fform">
</div>
