![]() Lokesh Pal
Lokesh Pal
![]() November 10, 2025 04:26
November 10, 2025 04:26
![]() 270
270
![]() 0
0
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने “वंदे मातरम्” के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर संचालित होने वाले समारोहों का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अमर गीत को “देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा का शाश्वत प्रतीक” बताया।
![]()

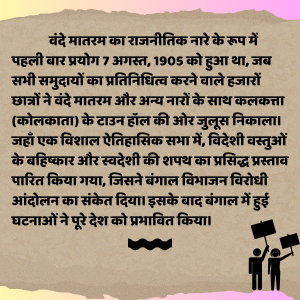
वंदे मातरम् भारतीय राष्ट्रवाद की आत्मा है, जिसमें भक्ति, एकता और शक्ति का मिश्रण है। भारत अपनी 150वीं वर्षगाँठ मना रहा है, यह एक अभिवादन और आह्वान दोनों है – सेवा, सद्भाव और स्थिरता के माध्यम से मातृभूमि का सम्मान करना।
<div class="new-fform">
</div>

Latest Comments