![]() Lokesh Pal
Lokesh Pal
![]() October 16, 2025 02:59
October 16, 2025 02:59
![]() 370
370
![]() 0
0
हाल ही में, नीति आयोग ने ‘भारत की ब्लू इकोनॉमी: गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्यपालन के दोहन के लिए रणनीति’ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की।
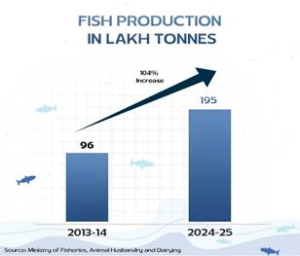

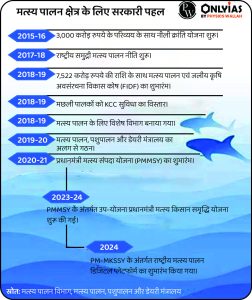


भारत की नीली अर्थव्यवस्था सतत् विकास, पारिस्थितिकी संतुलन और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है, जो अनुच्छेद-48A (राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का आदेश देती है) और SDG 14 (जल के नीचे जीवन) और SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) के साथ संरेखित है ताकि एक लचीला और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित समुद्री भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।
<div class="new-fform">
</div>

Latest Comments