![]() Lokesh Pal
Lokesh Pal
![]() May 16, 2025 03:19
May 16, 2025 03:19
![]() 310
310
![]() 0
0
ऑपरेशन सिंदूर ने मुख्य रूप से स्वदेशी हथियार प्रणालियों का उपयोग करके सटीक तथा बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान संचालित करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया।
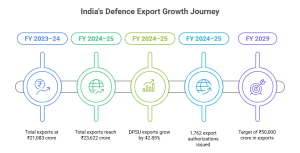
भारत द्वारा रक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाइसेंस प्राप्त उत्पादन से वास्तविक नवाचार की ओर बढ़ने पर आधारित है। ऑपरेशन सिंदूर स्वदेशी प्रणालियों की शक्तियों की पुष्टि करता है, लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने और भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण नेतृत्त्वकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए प्रणालीगत सुधार, तीव्र प्रमाणीकरण और गहन सार्वजनिक-निजी सामंजस्य आवश्यक है।
<div class="new-fform">
</div>

Latest Comments