![]() Lokesh Pal
Lokesh Pal
![]() May 13, 2025 02:38
May 13, 2025 02:38
![]() 1439
1439
![]() 0
0
वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र नवाचार-संचालित उच्च-तकनीकी उत्पादों की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके लिए भारत को प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिए अनुसंधान एवं विकास, कौशल और आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
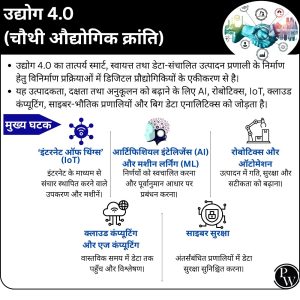

भारत का विनिर्माण क्षेत्र, जो GDP और रोजगार का एक महत्त्वपूर्ण कारक है, के वित्त वर्ष 2026 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के मूल्य तक पहुँचने की अपार संभावनाएँ हैं, जिसमें उन्नत अनुसंधान, कौशल विकास और मजबूत नीति समर्थन शामिल है। कम उत्पादकता, कौशल की कमी और बुनियादी ढाँचे के अंतराल जैसी चुनौतियों का समाधान करते हुए नवाचार और स्थिरता को अपनाकर, भारत अपने वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र तथा आर्थिक लचीलेपन को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है।
<div class="new-fform">
</div>

Latest Comments