![]() Lokesh Pal
Lokesh Pal
![]() October 07, 2025 02:54
October 07, 2025 02:54
![]() 401
401
![]() 0
0
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तटस्थ रुख के साथ रेपो दर को 5.50% पर अपरिवर्तित रखा है। मौद्रिक नीति समिति (MPC) के अनुसार, RBI ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लचीलेपन और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से चार प्रमुख उपाय किए हैं।
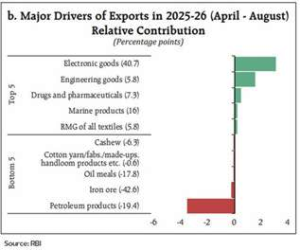
<div class="new-fform">
</div>

Latest Comments