- а§єа§Ѓа§Ња§∞а•З а§Ха•Ла§∞а•На§Єа•За§Ь
- а§ѓа•В৙а•Аа§Па§Єа§Єа•А а§С৮а§≤а§Ња§З৮
- а§ѓа•В৙а•Аа§Па§Єа§Єа•А а§Са§Ђа§≤а§Ња§З৮/а§єа§Ња§За§ђа•На§∞а§ња§°
- а§ѓа•В৙а•Аа§Па§Єа§Єа•А а§С৙а•Н৴৮а§≤
- а§Єа•На§Яа•За§Я ৙а•А.а§Па§Є.а§Єа•А. а§С৮а§≤а§Ња§З৮
- а§ѓа•В৙а•А. ৙а•А.а§Єа•А.а§Па§Є. а§С৮а§≤а§Ња§З৮
- а§ђа§ња§єа§Ња§∞ ৙а•А.а§Єа•А.а§Па§Є. а§С৮а§≤а§Ња§З৮
- а§Ѓа§єа§Ња§∞а§Ња§Ја•На§Яа•На§∞ ৙а•А.а§Па§Є.а§Єа•А. а§С৮а§≤а§Ња§З৮
- а§Ѓа§Іа•Нৃ৙а•На§∞৶а•З৴ ৙а•А.а§Па§Є.а§Єа•А. а§С৮а§≤а§Ња§З৮
- ৙৴а•На§Ъа§ња§Ѓ а§ђа§Ва§Ча§Ња§≤ ৙а•А.а§Па§Є.а§Єа•А. а§С৮а§≤а§Ња§З৮
- а§Єа•На§Яа•За§Я ৙а•А.а§Па§Є.а§Єа•А. а§Са§Ђа§≤а§Ња§З৮
- а§Яа•За§Єа•На§Я а§Єа•Аа§∞а•Аа§Ь
- а§Ха§∞а•За§Ва§Я а§Еа§Ђа•За§ѓа§∞а•На§Є
- а§°а•За§≤а•А ৙а•На§∞а•Иа§Ха•На§Яа§ња§Є
- а§Ђа•На§∞а•А а§∞а§ња§Єа•Ла§∞а•На§Єа•За§Ь
- а§Єа•За§Ва§Яа§∞


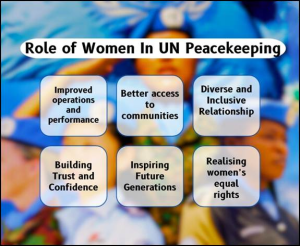
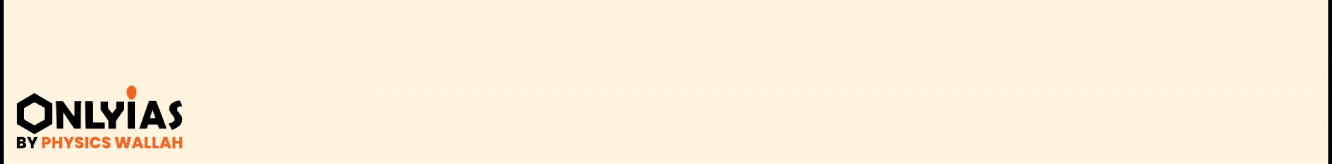
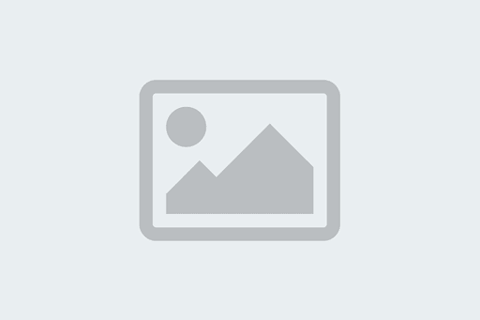
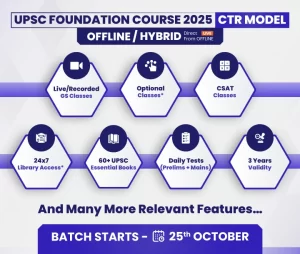




Latest Comments