प्रश्न की मुख्य माँग
- भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
- इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाएँ।
|
उत्तर:
भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने और कार्यबल को भविष्य के लिए कौशल विकास करने हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। चूंकि भारत, ‘नॉलेज इकॉनमी’ बनने का लक्ष्य रखता है, अतः सुलभ, न्यायसंगत और अभिनव शिक्षण अवसर प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 2047 तक स्थायी शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढाँचे की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल समावेशन जैसी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।
भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ
- बुनियादी ढाँचे और संसाधनों की कमी: कई स्कूल, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अपर्याप्त अवसंरचना हैं, जिसमें कक्षाओं, स्वच्छता सुविधाओं और डिजिटल उपकरण की कमी है, जो प्रभावी शिक्षण में बाधा डालते हैं।
- उदाहरण के लिए: वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2021 के अनुसार , केवल 67% ग्रामीण स्कूलों में कार्यात्मक शौचालय हैं, और 54% स्कूलों में डिजिटल शिक्षण उपकरणों तक पहुँच नहीं है जो गंभीर अवसंरचनात्मक कमी को दर्शाता है।
- शिक्षक की गुणवत्ता और प्रशिक्षण: शिक्षा की गुणवत्ता, सीधे तौर पर शिक्षकों की प्रभावशीलता से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुप्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में, जो छात्रों के शिक्षण परिणामों को प्रभावित करती है।
- उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, सरकारी स्कूलों में लगभग 20% शिक्षण पद खाली हैं, साथ ही STEM विषयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की भी काफी कमी है।
- उच्च ड्रॉपआउट दरें और असमानता: विशेष रूप से बालिकाओं और वंचित समुदायों की उच्च ड्रॉपआउट दरें, एक गंभीर चुनौती है। सामाजिक और आर्थिक कारक , जैसे बाल श्रम और कम उम्र में विवाह, इस समस्या के मुख्य कारण हैं।
- उदाहरण के लिए: यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+ 2020-21) के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर लगभग 17% है । बिहार और झारखंड जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में यह दर अधिक है।
- डिजिटल डिवाइड और प्रौद्योगिकी तक पहुँच: महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा की ओर बदलाव ने डिजिटल डिवाइड की समस्या को उजागर किया, जिसमें कई छात्रों के पास आवश्यक उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुँच नहीं होती।
- उदाहरण के लिए: शिक्षा मंत्रालय ने अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं हैं, जिससे ऑनलाइन शिक्षा में उनकी भागीदारी सीमित हो गई है।
- पुराना पाठ्यक्रम और रटकर पढ़ाई: कई भारतीय स्कूलों में पाठ्यक्रम पुराना है, और रटकर पढ़ाई करने पर अत्यधिक केंद्रित है, जो छात्रों में रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच का दमन कर देता है।
- उदाहरण के लिए: नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के अनुसार, कक्षा 8 में केवल 43% छात्र, गणित और विज्ञान में दक्ष थे, जो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।
इन चुनौतियों से निपटने के उपाय
- बुनियादी ढाँचे और संसाधनों में सुधार: स्कूली बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ाना चाहिए, विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में ताकि कक्षाएँ सुव्यवस्थित हो सकें तथा स्वच्छता एवं डिजिटल उपकरणों और संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- उदाहरण के लिए: समग्र शिक्षा अभियान का लक्ष्य 2022-23 में 37,500 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ स्कूली बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना है, जिसमें कक्षाओं के निर्माण और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती को बढ़ावा देना: विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों और वंचित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने चाहिए।
- उदाहरण के लिए: नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स (NISHTHA) ने नवीन शैक्षणिक प्रथाओं में 21 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है ।
- लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से ड्रॉपआउट दरों में कमी लाना: स्कूल में उपस्थिति को बढ़ावा देने और ड्रॉपआउट दरों को कम करने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों और मध्याह्न भोजन योजनाओं को लागू करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS), 2 लाख से अधिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करती है जिसका उद्देश्य ड्रॉपआउट दर को कम करना है।
- डिजिटल डिवाइड को कम करना: डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार करते हुए समावेशी डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को सस्ती इंटरनेट पहुँच और डिवाइस प्रदान करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: आत्मनिर्भर भारत के तहत 17 मई, 2020 को लॉन्च किया गया PM eVIDYA कार्यक्रम डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन-एयर शिक्षा प्रयासों को एकीकृत करता है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहु-आयामी पहुँच प्रदान करता है।
- पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधियों में सुधार: पाठ्यक्रम को जीवन कौशल, आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान को शामिल करने के लिए अद्यतन करना और रटने की शिक्षा से हटकर योग्यता-आधारित शिक्षण पाठ्यक्रम बनाना।
- उदाहरण के लिए: NEP 2020 मूल्यांकन के लिए एक नया ढाँचा प्रस्तुत करता है, जो समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए योगात्मक परीक्षाओं के बजाय निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देता है।
वर्ष 2047 तक भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढाँचे, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल समावेशन और पाठ्यक्रम सुधार को संबोधित करने वाले व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित होगी और नवाचार एवं आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा । इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करके, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन कर सकता है, आर्थिक विकास को गति दे सकता है और खुद को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित कर सकता है।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

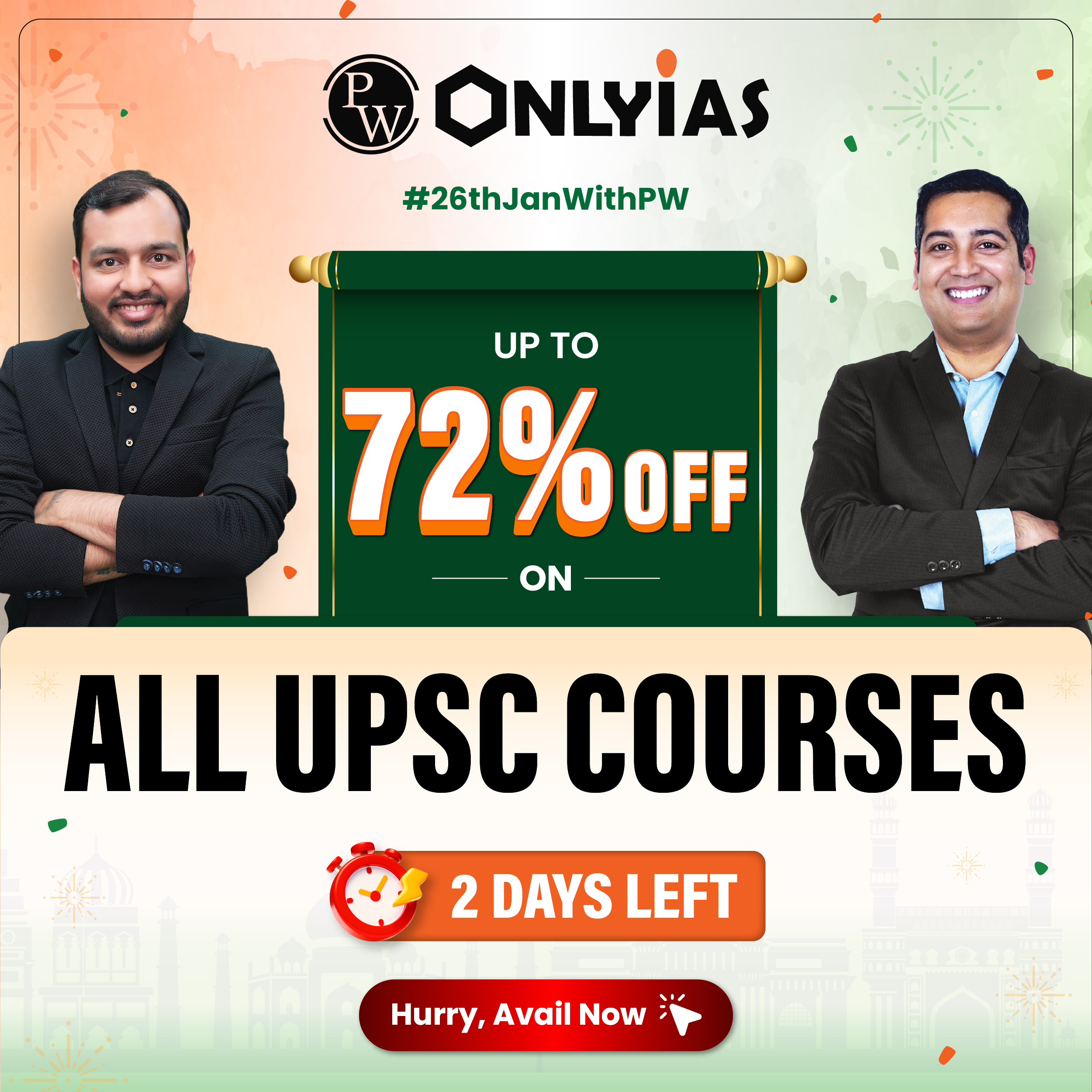
Latest Comments