प्रश्न की मुख्य माँग
- भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।
- PLI योजना के प्रभावी उपयोग में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- चर्चा कीजिए कि समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए इसका दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है।
|
उत्तर
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और वृद्धिशील उत्पादन से जुड़े वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके विदेशी निवेश को आकर्षित करना है । यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) का अनुमान है, कि GVA में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2030-31 तक 17% से बढ़कर 25% और 2047-48 तक 27% हो सकती है , जो भारत के आर्थिक परिवर्तन में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
Enroll now for UPSC Online Course
भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर PLI योजना का प्रभाव
- घरेलू उत्पादन को बढ़ावा: PLI योजना ने इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और फार्मास्यूटिकल्स जैसे 14 क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को काफी हद तक बढ़ाया है।
- उदाहरण के लिए: अगस्त 2024 तक, ₹1.46 लाख करोड़ का वास्तविक निवेश हुआ है, जिससे उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो ₹12.50 लाख करोड़ तक पहुँच गई है, जो विनिर्माण उत्पादन को बढ़ावा देने में योजना की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का आकर्षण: PLI योजना, FDI को आकर्षित करने में कारगर साबित हुई है, जिससे भारत में वैश्विक विनिर्माण केंद्र स्थापित हुए हैं।
- उदाहरण के लिए: फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जैसी कंपनियों ने भारतीय विनिर्माण संयंत्रों में अपना निवेश बढ़ाया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में देश की स्थिति मजबूत हुई है।
- रोजगार सृजन: PLI योजना ने कपड़ा और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करके रोजगार सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- उदाहरण के लिए: PLI योजना ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 9.5 लाख नौकरियां सृजित की हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- तकनीकी उन्नति: इस योजना ने विदेशी निवेश को आकर्षित किया है और भारतीय विनिर्माण में उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा दिया है।
- उदाहरण के लिए: ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, PLI योजना ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और नई पीढ़ी के ऑटोमोबाइल के उत्पादन को बढ़ावा दिया है, जिससे सतत विनिर्माण को बढ़ावा मिला है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि: PLI योजना का उद्देश्य उत्पादन लागत को कम करके और गुणवत्ता मानकों में सुधार करके भारत को वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- उदाहरण के लिए: इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों द्वारा संचालित निर्यात ₹4 लाख करोड़ को पार कर गया है।
PLI योजना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में आने वाली चुनौतियाँ
- क्षेत्रीय असमानताएँ : कुछ राज्य बेहतर बुनियादी ढाँचे और प्रशासनिक क्षमता के कारण PLI योजना को लागू करने में अधिक सक्षम हैं, जबकि अन्य पीछे हैं।
- उदाहरण के लिए: गुजरात और तमिलनाडु में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों जहाँ पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव है की तुलना में PLI के तहत निवेश आकर्षित करने में अधिक सफलता देखी गई है।
- बोझिल लाइसेंसिंग प्रक्रियाएँ: लाइसेंस प्राप्त करने की लंबी और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ परियोजनाओं में देरी करती हैं और निवेश को हतोत्साहित करती हैं, जिससे विनिर्माण पहलों का समय पर क्रियान्वयन प्रभावित होता है।
- उदाहरण के लिए: फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में जटिल विनियामक आवश्यकताओं के कारण उद्योगों को देरी का सामना करना पड़ता है।
- अप्रभावी अनुबंध कार्यान्वयन: अनुबंधों के कमज़ोर प्रवर्तन से निवेशकों का विश्वास कम होता है और विकास बाधित होता है, जिससे उद्योग अपना परिचालन बढ़ाने में हिचकिचाते हैं।
- उदाहरण के लिए: अनुबंध प्राप्त करने में होने वाली देरी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों के विश्वास में कमी लाई है।
- धीमी समग्र वृद्धि: अपनी क्षमता के बावजूद, संरचनात्मक और परिचालन अक्षमताओं के कारण विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार सुस्त बना हुआ है।
- उदाहरण के लिए: कुशल बुनियादी ढाँचे की कमी और उच्च रसद लागत, धीमी औद्योगिक वृद्धि में योगदान करती है, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में।
- आउटपुट और GVA वृद्धि के बीच अंतर: वर्ष 2022-23 में विनिर्माण आउटपुट वृद्धि (21.5%) और GVA वृद्धि (7.3%) के बीच असमानता स्पष्ट रुप से उजागर हुई है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती इनपुट लागत है।
- उदाहरण के लिए: इनपुट लागत में 24.4% की वृद्धि हुई , जिससे उत्पादन की मात्रा बढ़ने के बावजूद लाभप्रदता कम हो गई, विशेषकर बुनियादी धातुओं और पेट्रोलियम उत्पादों में।
समावेशी विकास हासिल करने के लिए PLI योजना का दायरा बढ़ाना
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना: PLI योजना के लाभों को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित करने से समावेशी विकास सुनिश्चित हो सकता है और महानगरीय केंद्रों के बाहर भी रोजगार सृजित हो सकते हैं।
- उदाहरण के लिए: यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़ा क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए, तो इससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय आय असमानताएँ कम हो सकती हैं।
- SME और स्टार्टअप के लिए सहायता: लघु और मध्यम उद्यमों (SME) और स्टार्टअप के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने से PLI योजना में उनकी भागीदारी बढ़ सकती है।
- उदाहरण के लिए: यदि माइक्रोमैक्स और लावा जैसी लघु, घरेलू कंपनियों को धन और प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच प्रदान करके सहायता प्रदान की जाये तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अधिक वृद्धि देखी जा सकती है।
- सतत विनिर्माण को बढ़ावा देना: इस योजना का विस्तार हरित और सतत विनिर्माण प्रथाओं की सहायता करने के लिए किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देकर वंचित समुदायों को लाभ होगा।
- कौशल विकास कार्यक्रम: क्षेत्र-विशिष्ट कौशल विकास कार्यक्रम स्थापित करने से यह सुनिश्चित होगा कि सभी क्षेत्रों में PLI योजना का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित कार्यबल तैयार हो।
- उदाहरण के लिए: यदि EV प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में श्रमिकों के कौशल को प्राथमिकता दी जाये तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है।
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकरण: छोटे उद्योगों का डिजिटलीकरण और अविकसित क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी से छोटी कंपनियों को PLI योजना का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
- उदाहरण के लिए: IoT और AI जैसी इंडस्ट्री 4.0 प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माताओं को, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वैश्विक बाज़ारों से जुड़ने में सक्षम बनाया जा सकता है।
Check Out UPSC CSE Books From PW Store
PLI योजना भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण पहल है, परंतु समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रभावी विस्तार और कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण है। निरंतर प्रयासों के साथ, वर्ष 2047 तक भारत की विकसित अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा में विनिर्माण क्षेत्र एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है ।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

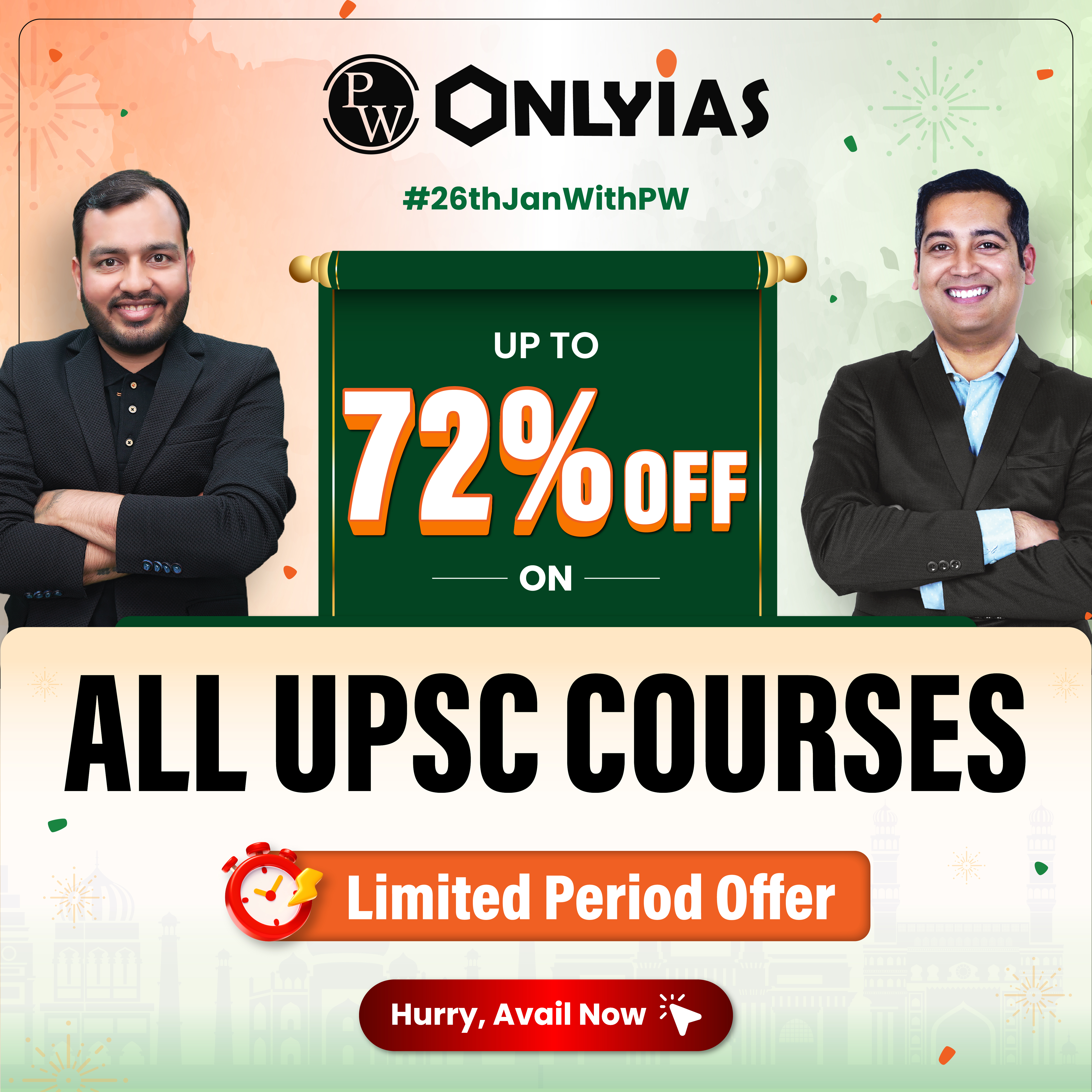
Latest Comments