प्रश्न की मुख्य माँग
- यह समझाइए कि वर्ष 2023 में सिक्किम हिमनद झील प्रस्फुटन से आई बाढ़ ने हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत अवसंरचना की सुभेद्यताओं को कैसे उजागर किया।
- हिमालयी क्षेत्र में विशाल बांध परियोजनाओं के औचित्य का परीक्षण कीजिए।
- जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों और पर्यावरणीय संधारणीयता के संदर्भ में हिमालयी क्षेत्र में विशाल बांध परियोजनाओं की व्यवहार्यता में चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
- आगे की राह लिखिये।
|
उत्तर
दक्षिण ल्होनक झील में हिमनद झील प्रस्फुटन बाढ़ आई जिसमें 55 लोगों की जान चली गई और 1,200 मेगावाट का तीस्ता-III जलविद्युत संयंत्र नष्ट हो गया। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हिमनद झील का बाँध कमजोर हो जाता है और जल तेज प्रवाह के साथ बहने लगता है जिससे जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अस्थिरता के बीच हिमालयी बुनियादी ढाँचे के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत सुभेद्यताओं का उजागर होना
- बांध के बुनियादी ढाँचे की कमजोरी: तीस्ता– III बांध के ढहने से भूगर्भीय रूप से अस्थिर, उच्च जोखिम वाले और जलवायु के प्रति संवेदनशील हिमनद क्षेत्रों में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं की संरचनात्मक सुभेद्यता उजागर हुई।
- उदाहरण के लिए: GLOF, बांध के मलबे को नीचे की ओर ले गया, जिससे अधिक गंभीर विनाश हुआ, हजारों लोग विस्थापित हुए और सिक्किम के कई जिलों के लोग प्रभावित हुए।
- अप्रत्याशित जलवायु-प्रेरित घटनाएँ: परंपरागत जल विज्ञान और मौसम विज्ञान मॉडल सिक्किम बाढ़ जैसी घटनाओं का अनुमान लगाने में विफल रहे, जिससे दीर्घकालिक आपदा तत्परता और प्रतिक्रिया तंत्र में गंभीर कमियाँ उजागर हुईं।
- उदाहरण के लिए: स्थानीय मौसम केंद्रों में मध्यम वर्षा दर्ज की गई फिर भी हिमनद बांध के ढहने के कारण बाढ़ का प्रभाव भयावह था जिससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई।
- प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का अभाव: इस आपदा ने चेतावनी तंत्रों की अपर्याप्तता, सीमित पूर्वानुमान क्षमताओं और खराब संचार नेटवर्क को उजागर किया, जिससे जनसमुदाय और बुनियादी ढाँचा अचानक उच्च तीव्रता वाली बाढ़ के प्रति असुरक्षित हो गया।
- उदाहरण के लिए: दक्षिण ल्होनक झील की इस घटना का पता सही समय पर नहीं चल पाया जिससे अधिकारियों को बड़े पैमाने के निकासी और शमन उपायों के लिए बहुत कम समय मिला।
- जलवायु परिवर्तन का गुणक प्रभाव: हिमनदो के पिघलने में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, झीलों का विस्तार और अनियमित मानसून, भविष्य में GLOF और बड़े पैमाने के पारिस्थितिक विनाश के जोखिम को बढ़ाते हैं, जिससे बड़े बांध और भी अधिक असुरक्षित हो जाते हैं।
- उदाहरण के लिए: हिमालय में हिमनद झीलों की संख्या में 10.8% की वृद्धि हुई है और वर्ष 2011 से वर्ष 2024 के बीच उनके सतही क्षेत्र में 33.7% का विस्तार हुआ है, जिससे जोखिम कारक बढ़ गए हैं।
- बुनियादी ढाँचे की विफलता से उत्पन्न द्वितीयक आपदाएँ: बांधों के विनाश, नदी तट के अपरदन, तलछट के संचय और भूस्खलन के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने की बाढ़ आई, जिससे सामाजिक-आर्थिक क्षति और पर्यावरणीय क्षति हुई।
हिमालय में विशाल बांध परियोजनाओं का औचित्य
- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन: जलविद्युत एक स्वच्छ, निम्न कार्बन वाला और संधारणीय ऊर्जा स्रोत है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है, जलवायु परिवर्तन को कम करता है और भारत की बढ़ती बिजली की माँग को पूरा करता है।
- उदाहरण के लिए: तीस्ता परियोजना की स्थापित क्षमता 1,200 मेगावाट थी, जिसने सिक्किम के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और बिजली ग्रिड स्थिरता में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- जल संसाधन प्रबंधन: बांध, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन और दीर्घकालिक जल भंडारण में मदद करते हैं, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में पीने, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- उदाहरण के लिए: भाखड़ा नांगल बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई कार्यों में मदद करता है, जिससे वर्षभर फसल उत्पादन और सूखे से निपटने की क्षमता सुनिश्चित होती है।
- आर्थिक और सामाजिक विकास: विशाल बांध परियोजनाएँ प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करती हैं, बुनियादी ढाँचे में सुधार करती हैं, पर्यटन को बढ़ावा देती हैं और राज्य के राजस्व को बढ़ाती हैं, जिससे स्थानीय समुदायों और समग्र क्षेत्रीय आर्थिक विकास को लाभ मिलता है।
- उदाहरण के लिए: टिहरी बाँध परियोजना ने सड़क नेटवर्क, जलविद्युत क्षमता और रोजगार के अवसरों को बढ़ाया, जिससे उत्तराखंड का आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी बढ़ी।
- ऊर्जा निर्यात क्षमता: हिमालयी राज्य, ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों में अधिशेष बिजली का निर्यात कर सकते हैं, जिससे अंतरराज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और आयातित ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी।
- उदाहरण के लिए: भारत को भूटान का जलविद्युत निर्यात उसके सकल घरेलू उत्पाद में 25% से अधिक का योगदान देता है जिससे भारत के साथ द्विपक्षीय आर्थिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत होते हैं।
- रणनीतिक राष्ट्रीय हित: सीमावर्ती क्षेत्रों के पास बांध, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, जल संप्रभुता और रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाते हैं, जिससे हिमालय की ऊपरी नदियों के प्रवाह पर चीन का नियंत्रण रुक जाता है।
- उदाहरण के लिए: अरुणाचल प्रदेश की जलविद्युत परियोजनाएँ ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की बांध-निर्माण पहल का मुकाबला करती हैं, जिससे भारत के जल अधिकार सुरक्षित होते हैं।
हिमालयी क्षेत्र में बड़े बांधों की व्यवहार्यता में चुनौतियाँ
- भूवैज्ञानिक और भूकंपीय अस्थिरता: हिमालय भूकंप, भूस्खलन, हिमनद संचलन और अपरदन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिससे बांधों के ढहने, संरचनात्मक विफलताओं और बड़े पैमाने की आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है।
- उदाहरण के लिए: 2015 के नेपाल भूकंप ने जलविद्युत संरचनाओं को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे हिमालयी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भूकंपीय सुभेद्यतायें उजागर हुईं।
- अप्रत्याशित जलवायु-प्रेरित आपदाएँ: हिमनद झील प्रस्फुटन बाढ़ (GLOF), बादल फटने की घटना में और अनियमित मानसून, मौजूदा बांध डिजाइनों को प्रभावित कर सकते हैं जिससे दीर्घकालिक व्यवहार्यता और जोखिम प्रबंधन बेहद मुश्किल हो सकता है।
- उदाहरण के लिए: केदारनाथ बाढ़ (2013) ने बुनियादी ढाँचे को तबाह कर दिया, जिससे साबित होता है कि चरम मौसम की घटनाएँ अनुमानित सुरक्षा सीमाओं को पार कर सकती हैं।
- पारिस्थितिकी और जैव विविधता ह्वास: बड़े बांधों से जंगल डूब जाते हैं, नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में बाधा आती है, मछलियों के प्रवास में बाधा आती है और वन्यजीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता ह्वास होता है और पर्यावरण को अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है।
- उदाहरण के लिए: अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी बांध परियोजना से नदी की प्रजातियाँ खतरे में हैं, जिनमें संकटग्रस्त गंगा डॉल्फ़िन और प्रवासी मछलियाँ शामिल हैं।
- विस्थापन और सामाजिक संघर्ष: बांध निर्माण के कारण जबरन बेदखली, भूमि से बेदखल होना, पैतृक आजीविका ह्वास और सांस्कृतिक क्षरण होता है, जिससे प्रतिरोध आंदोलन और दीर्घकालिक पुनर्वास चुनौतियां पैदा होती हैं।
- उच्च वित्तीय और रखरखाव लागत: बार-बार मरम्मत, अवसादन, पर्यावरण शमन और जलवायु अनुकूलन उपायों से परिचालन लागत बढ़ जाती है, जिससे जलविद्युत कम प्रतिस्पर्धी और आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाती है।
- उदाहरण के लिए: जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा जलविद्युत परियोजना को भूस्खलन, गाद और बिजली शुल्क वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ा।
आगे की राह
- ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना: विशाल बांधों पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और जलवायु अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देने के लिए विकेन्द्रीकृत सौर, पवन और लघु-स्तरीय पनबिजली परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: लद्दाख की हाइब्रिड सौर-पवन ऊर्जा परियोजनाएं, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव और सामुदायिक भागीदारी के साथ संधारणीय विद्युत की आपूर्ति करती हैं।
- जलवायु प्रतिरोध को बढ़ाना: जलवायु-प्रेरित चरम मौसमी घटनाओं का सामना करने के लिए बांध डिजाइन, बाढ़ जल निकासी क्षमता, आपदा न्यूनीकरण रणनीतियों और तलछट नियंत्रण प्रणालियों में सुधार करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: तीस्ता-3 के उन्नत स्पिलवे और मजबूत कंक्रीट संरचना का उद्देश्य उच्च बाढ़ को प्रबंधित करना और संरचनात्मक स्थिरता को बढ़ाना है।
- प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी प्रणाली: संभावित आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए AI-आधारित रियलटाइम हिमनद झील निगरानी, सैटेलाइट ट्रैकिंग, पूर्वानुमान विश्लेषण और स्थानीयकृत चेतावनी प्रणाली तैनात करनी चाहिए।
- उदाहरण के लिए: भूटान की GLOF प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली रिमोट सेंसिंग को एकीकृत करती है, जिससे गांवों को अचानक बाढ़ आने से पहले सुरक्षित रूप से गांव से निकासी करने की सुविधा मिलती है।
- समुदाय-केंद्रित विकास: विस्थापन-संबंधी संघर्षों को रोकने के लिए बांध प्रभावित आबादी हेतु स्थानीय भागीदारी, आजीविका बहाली, उचित मुआवजा और सतत आर्थिक विकल्प सुनिश्चित करना चाहिए।
- सख्त पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA): बांध परियोजनाओं की शुरुआत करने से पहले जलवायु जोखिम आकलन, हिमनद झील निगरानी और पारिस्थितिक प्रभाव अध्ययनों को शामिल करते हुए वैज्ञानिक, स्वतंत्र EIA लागू करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: नॉर्वे के जलविद्युत नियम सख्त पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययनों को अनिवार्य बनाते हैं, जिससे दीर्घकालिक संधारणीयता और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित होता है।
अंतर्निहित भूकंपीय गतिविधि, GLOF की बढ़ती आवृत्ति और हिमालय के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए, इस क्षेत्र में विशाल बांध परियोजनाओं की व्यवहार्यता अत्यधिक संदिग्ध है। पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर जैसे वैकल्पिक ऊर्जा समाधानों को प्राथमिकता देना और व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को लागू करना, संवेदनशील हिमालयी पर्यावरण को संरक्षित करते हुए सतत ऊर्जा विकास को प्राप्त करने की दिशा में प्रभावकारी कदम सिद्ध हो सकता है।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

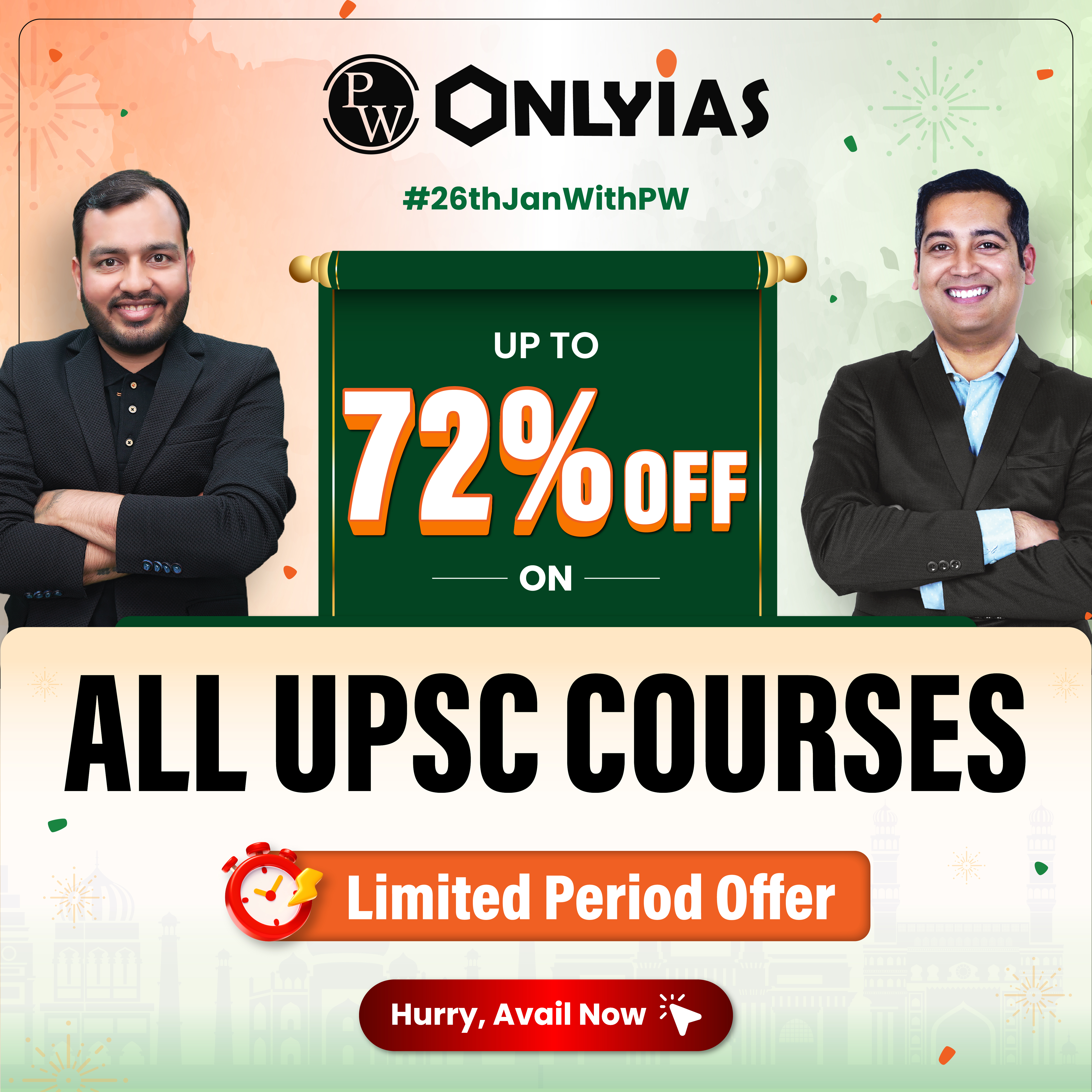
Latest Comments