प्रश्न की मुख्य माँग
- इस बात पर प्रकाश डालिये कि किस प्रकार भारत का वायु प्रदूषण संकट पर्यावरणीय निम्नीकरण से कहीं अधिक गहन संरचनात्मक मुद्दों को दर्शाता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का परीक्षण कीजिये।
- राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने में शासन-संबंधी चुनौतियों का परीक्षण कीजिये।
- आगे की राह लिखिये।
|
उत्तर
भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है। विश्व के 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 84 शहर, भारत में स्थित हैं। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (AQLI) की रिपोर्ट के अनुसार PM 2.5 प्रदूषण भारत में जीवन प्रत्याशा को 5.3 वर्ष से भी अधिक कम कर देता है। पर्यावरणीय क्षति से परे, यह संकट शहरी नियोजन विफलताओं, औद्योगिक कुप्रबंधन और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को रेखांकित करता है जिसके लिए प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है।
पर्यावरणीय क्षरण से परे गहन संरचनात्मक मुद्दे
- शासन क्षमता की कमी: वायु प्रदूषण को अक्सर बहु-क्षेत्रीय शासन चुनौती के बजाय एक तकनीकी मुद्दे के रूप में देखा जाता है, जो प्रभावी नीति निर्माण और प्रवर्तन को सीमित करता है।
- उदाहरण के लिए: कई नगर निकायों के पास प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए धन और स्वायत्तता का अभाव है जिसके कारण दिल्ली NCR में निर्माण धूल नियमों का खराब प्रवर्तन होता है ।
- आर्थिक विकास बनाम संधारणीयता: तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन वायु गुणवत्ता से जुड़े सख्त कानून आर्थिक विकास में बाधा डाल सकते हैं, जिससे नीति पर असर पड़ सकता है।
- प्रदूषण नियंत्रण में शहरी-ग्रामीण विभाजन: अधिकांश वायु गुणवत्ता निगरानी और शमन प्रयास शहरी केंद्रों पर केंद्रित होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र बायोमास जलने जैसे प्रदूषणों के बावजूद उपेक्षित रहते हैं।
- उदाहरण के लिए: पंजाब और हरियाणा में किसानों के लिए व्यवहार्य वैकल्पिक निपटान प्रोत्साहनों की कमी के कारण पराली जलाना जारी है जिससे सर्दियों में धुंध की स्थिति और खराब हो रही है।
- संस्थागत अव्यवस्था: विभिन्न एजेंसियां, नगर निकाय, राज्य प्रदूषण बोर्ड और केंद्रीय मंत्रालय एक दूसरे से अलग होकर काम करते हैं, जिससे नीति क्रियान्वयन में अक्षमता आती है।
- उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को धन के उपयोग में कठिनाई हो रही है और प्रशासनिक बाधाओं के कारण वर्ष 2019-2023 के बीच आवंटित धन का केवल 60% ही उपयोग किया जा सका है।
- तकनीकी अति-निर्भरता: भारत तेजी से AI डैशबोर्ड और स्मॉग टावरों पर निर्भर हो रहा है, लेकिन पुराने वाहनों और बायोमास जलाने जैसे बुनियादी प्रदूषण स्रोतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
- उदाहरण के लिए: दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर लगाए लेकिन अध्ययनों में पाया गया कि वाहनों पर प्रतिबंध और अपशिष्ट प्रबंधन की तुलना में इनका वायु गुणवत्ता पर नगण्य प्रभाव पड़ा।
वायु प्रदूषण से निपटने में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ
- प्रदूषण नियंत्रण की उच्च लागत: स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन को अपनाने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है, जो कई लघु व्यवसायों और उद्योगों के लिए वहनीय नहीं है।
- उदाहरण के लिए: भारत स्टेज VI (BS-VI) ईंधन में अपग्रेड करने से तेल कंपनियों को 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ, जिससे छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए अनुकूल वाहनों पर स्विच करना कठिन हो गया।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की भूमिका: भारत की अर्थव्यवस्था का एक विशाल हिस्सा, ईंट भट्टे, सड़क किनारे के विक्रेता और लघु-स्तरीय विनिर्माण, पर्यावरण नियमों का पालन किये बिना काम करते हैं जिससे प्रदूषण और भी गंभीर हो जाता है।
- उदाहरण के लिए: कानपुर में चमड़े के कारखाने, गंगा में प्रदूषक पदार्थ छोड़ते हैं और चमड़े के अवशेष जलाते हैं, लेकिन उनके आर्थिक महत्त्व के कारण उन पर सख्ती से अमल करना कठिन है।
- जन जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन का अभाव: जागरूकता या विकल्पों की कमी के कारण कई व्यक्ति अभी भी खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन और कचरे को खुले में जलाने पर निर्भर हैं।
- उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत 9.6 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन वितरित किए जाने के बावजूद कई परिवार दोबारा गैस भराने की लागत के कारण जलाऊ लकड़ी का उपयोग करना जारी रखे हुए हैं।
- स्वास्थ्य बोझ और आर्थिक उत्पादकता: प्रदूषण से संबंधित श्वसन संबंधी बीमारियां स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ाती हैं, कार्यबल की दक्षता कम करती हैं और सकल घरेलू उत्पाद को प्रभावित करती हैं।
- उदाहरण के लिए: प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य लागत के कारण भारत को प्रतिवर्ष अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.36% का नुकसान होता है जिससे उत्पादकता और आर्थिक उत्पादन प्रभावित होता है।
वायु प्रदूषण से निपटने में शासन-संबंधी चुनौतियाँ
- कमजोर नीति प्रवर्तन: मौजूदा प्रदूषण कानूनों को शायद ही कभी सख्ती से लागू किया जाता है, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्रों में उल्लंघन और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में बार-बार वृद्धि होती है।
- उदाहरण के लिए: दिल्ली की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) प्रायः निवारक के बजाय प्रतिक्रियात्मक होती है, जो गंभीर धुंध की घटनाओं को रोकने में विफल रहती है।
- खंडित संस्थागत जिम्मेदारियाँ: अनेक एजेंसियां, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शहरी स्थानीय निकाय, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र के साथ काम करते हैं जिसके कारण प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होता है।
- उदाहरण के लिए: दिल्ली -गुरुग्राम-फरीदाबाद प्रदूषण संकट के लिए राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता है, लेकिन राज्य अक्सर संयुक्त समाधान लागू करने के बजाय एक-दूसरे पर दोष मढ़ते हैं
- स्वच्छ वायु निधि का कम उपयोग: NCAP जैसे वायु गुणवत्ता कार्यक्रम, प्रशासनिक बाधाओं और कमजोर स्थानीय प्रशासन क्षमता के कारण कम निधि उपयोग की समस्या से ग्रस्त हैं।
- राजनीतिक और औद्योगिक प्रतिरोध: सख्त वायु प्रदूषण नीतियों को औद्योगिक लॉबी और राजनीतिक समूहों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो पर्यावरणीय चिंताओं पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते हैं।
- उदाहरण के लिए: खराब वायु गुणवत्ता के बावजूद, सिंगरौली में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र राजनीतिक और औद्योगिक दबाव के कारण काम करना जारी रखे हुए हैं।
आगे की राह
- स्थानीय शासन और वित्तपोषण को मजबूत करना: नगर निकायों को स्वच्छ वायु वित्तपोषण पर सीधा नियंत्रण और स्थानीय वायु गुणवत्ता उपायों के लिए निर्णय लेने की शक्ति मिलनी चाहिए।
- उदाहरण के लिए: अहमदाबाद जैसे शहरों ने वायु सूचना एवं प्रतिक्रिया (AIR) योजनाएं स्थापित की हैं जिससे स्थानीय प्रतिक्रिया और निधि आवंटन में सुधार हुआ है।
- लक्षित उत्सर्जन-कटौती मीट्रिक्स को अपनाना: वायु प्रदूषण के स्तर की निगरानी के बजाय उद्योगों, परिवहन और घरेलू क्षेत्रों से वास्तविक उत्सर्जन में कमी पर नज़र रखनी चाहिए।
- उदाहरण के लिए: कैलिफोर्निया की कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली ने उत्सर्जन सीमाओं को अनुपालन के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों से जोड़कर औद्योगिक प्रदूषण को कम किया।
- ग्रामीण और शहरी रणनीतियों को एकीकृत करना: वायु प्रदूषण शमन को महानगरों से आगे भी विस्तारित करना चाहिए, जिसमें ग्रामीण बायोमास विकल्प और कृषि अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल होना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: ब्राजील की सामुदायिक-नेतृत्व वाली अपशिष्ट प्रणालियों ने खुले में फसल जलाने को कम करने में मदद की, जिससे जमीनी स्तर पर भागीदारी का महत्त्व पता चला।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना: सरकारों को लागत प्रभावी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: FAME II नीति सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार में मदद करती है जिससे सार्वजनिक परिवहन संचालकों के बीच इनका प्रचलन बढ़ता है।
- व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना: व्यापक वायु प्रदूषण साक्षरता अभियान पर्यावरण अनुकूल आदतों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे कारपूलिंग और अपशिष्ट पृथक्करण।
- उदाहरण के लिए: स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रव्यापी सहभागिता प्रयासों के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जनता के दृष्टिकोण को बदलकर सफल हुआ।
भारत के वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए मजबूत नीति प्रवर्तन, तकनीकी नवाचार और समुदाय-संचालित समाधानों की आवश्यकता है। शासन ढाँचे को मज़बूत करना, संधारणीय शहरीकरण को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में तेजी लाना स्थायी बदलाव ला सकता है। स्वच्छ हवा और सभी के लिए स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार, उद्योगों और नागरिकों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक है।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

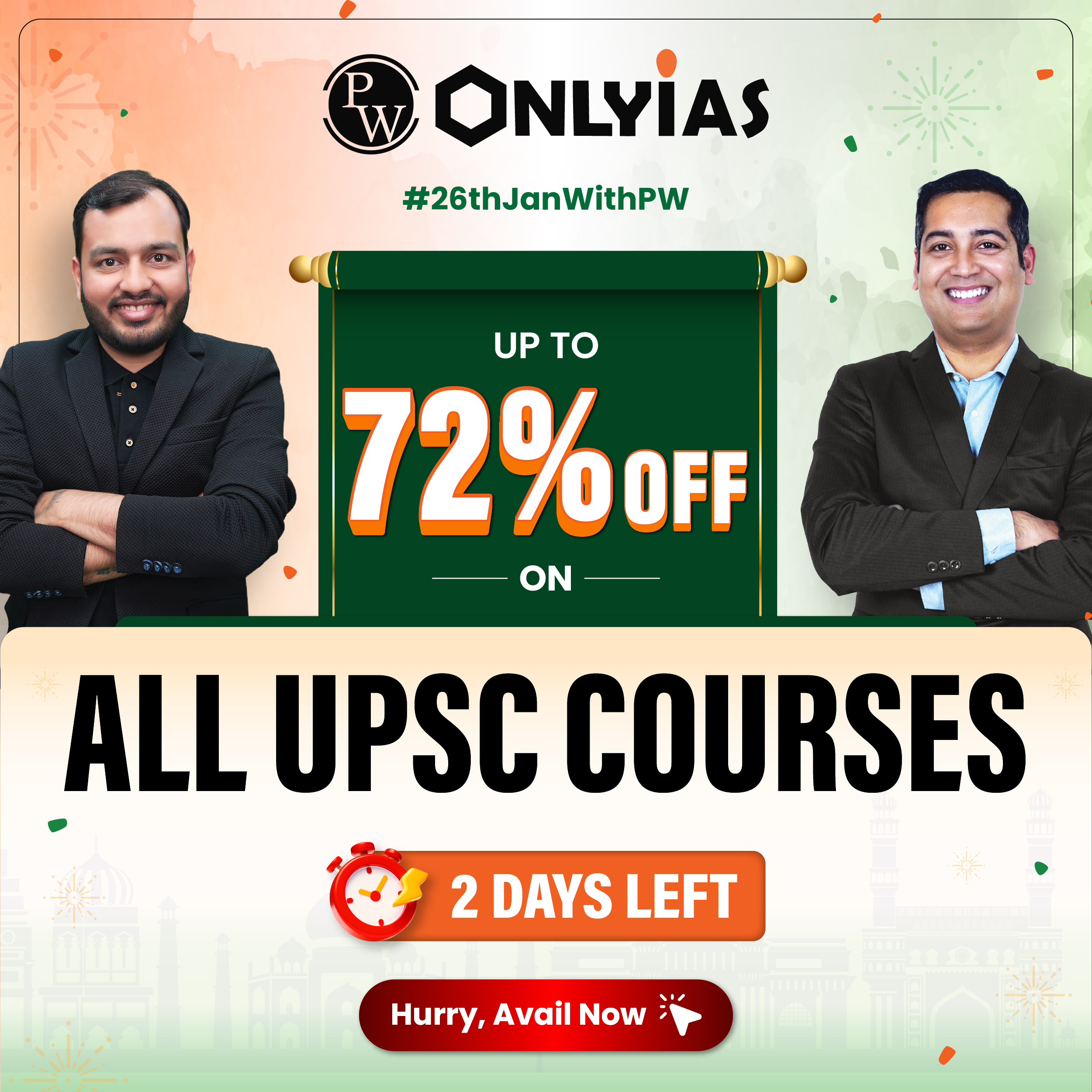
Latest Comments