निबंध का प्रारूपप्रस्तावना : दृश्यता-सशक्तिकरण विरोधाभास
मुख्य-विषयवस्तु
निष्कर्ष: देखे जाने से लेकर सुने जाने तक, वर्तमान से शक्तिशाली तक
|
आज के भारत में, महिलाएँ पहले से कहीं अधिक उपस्थित दिखती हैं, विमान उड़ा रही हैं, व्यवसायों का नेतृत्व कर रही हैं, संसद में बहस कर रही हैं और अकादमिक रैंकिंग में अपना दबदबा बना रही हैं। वित्त मंत्रालय की कमान संभाल रही श्रीमती निर्मला सीतारमण से लेकर स्वयं सहायता समूहों का नेतृत्व करने वाली आदिवासी महिलाओं तक, सभी क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी बढ़ी है। फिर भी, इस सतही प्रगति के पीछे एक परेशान करने वाला सवाल बना हुआ है: क्या यह मौजूदगी वास्तविक शक्ति में परिवर्तित होती है?
देखे जाने और सुने जाने के बीच का अंतर, जगह घेरने और नतीजों को आकार देने के बीच का अंतर, एक गहरी अस्वस्थता को दर्शाता है, जहाँ प्रतिनिधित्व पर नियंत्रण का अभाव है, उपस्थिति में स्वायत्तता का अभाव है, और उपलब्धियाँ पितृसत्तात्मक सीमाओं के भीतर ही सीमित रहती हैं। जैसा कि डॉ. अंबेडकर ने सटीक रूप से कहा था, “मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूँ।” केवल उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है। शक्ति ही प्रगति का सही माप है।
भारतीय सभ्यता की यात्रा महिलाओं की शक्ति की प्रकृति में एक गहन बदलाव को दर्शाती है। वैदिक युग में गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिलाएँ बौद्धिक चर्चाओं में शामिल थीं, यहाँ तक कि सभाओं में भी भाग लेती थीं। संपत्ति के अधिकार, शिक्षा और आध्यात्मिक अधिकार से उन्हें पूरी तरह वंचित नहीं किया गया था।
हालाँकि, बाद में मनुस्मृति जैसे धर्मग्रंथों और अन्य ग्रंथों की व्याख्या ने एक कठोर पितृसत्तात्मक व्यवस्था को संस्थागत बना दिया। मध्यकाल तक, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा ने महिलाओं को शारीरिक और वैचारिक रूप से हाशिये पर ला दिया था। औपनिवेशिक काल में सुधारवादी प्रयास, राजा राम मोहन राय का सती प्रथा के खिलाफ अभियान या ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास, हालांकि आवश्यक थे, लेकिन अक्सर महिलाओं को उत्थान के विषय के रूप में पेश किया गया, न कि परिवर्तन के कारक के रूप में।
इस प्रकार, भारतीय इतिहास केवल महिलाओं के दमन का ही अभिलेख नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म व्युत्क्रमण का भी अभिलेख है, जिसमें प्रारंभिक समाज में दृश्य शक्ति से लेकर संस्कृति, परिवार और नैतिकता के नाम पर अदृश्य अधीनता तक का वर्णन है।
भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक महिलाओं को उच्च राजनीतिक पदों पर देखा है, फिर भी उनका उत्थान अक्सर प्रणालीगत से ज़्यादा प्रतीकात्मक प्रतीत होता है। जमीनी स्तर पर, 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया, जो विकेंद्रीकृत सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। आज, ग्रामीण भारत में दस लाख से ज़्यादा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पद पर हैं।
लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह उपस्थिति सत्ता के बराबर है। “सरपंच पति राज” की घटना, जहाँ पुरुष रिश्तेदार निर्णयों को नियंत्रित करते हैं, यह उजागर करती है कि पितृसत्ता खुद को किस तरह नए रूपों में ढालती है। राष्ट्रीय स्तर पर, संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 15% है, और रक्षा या गृह जैसे महत्वपूर्ण विभाग अभी भी बड़े पैमाने पर पुरुषों के पास हैं। 33% महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने में देरी वास्तविक सशक्तिकरण के खिलाफ संस्थागत जड़ता को दर्शाती है।
जब तक महिलाएं न केवल मतदाताओं को बल्कि निर्वाचित लोगों को भी आकार नहीं देंगी, तब तक उनकी राजनीतिक उपस्थिति परिवर्तनकारी होने के बजाय प्रदर्शनकारी बनने का खतरा है।
महिलाएं अब अर्थव्यवस्था में हर जगह भाग ले रही हैं, गिग प्लेटफॉर्म से लेकर बोर्डरूम तक, लेकिन संसाधनों, पूंजी और निर्णयों पर उनका नियंत्रण अक्सर उनसे दूर रहता है। ग्रामीण महिलाएं कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जो 60% से अधिक श्रम का योगदान देती हैं, फिर भी उनके पास 15% से भी कम भूमि है। शहरी व्यावसायिक क्षेत्रों की स्थिति थोड़ी बेहतर है; कॉर्पोरेट बोर्ड अभी भी पुरुष-प्रधान हैं, और उच्च-कुशल क्षेत्रों में भी लिंग वेतन अंतर बना हुआ है।
जबकि फल्गुनी नायर या किरण मजूमदार शॉ जैसी सफल उद्यमियों की कहानियां भी मौजूद हैं, वे आदर्श के बजाय अपवाद ही बनी हुई हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की बढ़ती संख्या उत्साहजनक है, फिर भी उद्यम पूंजी और बाजार नेटवर्क तक पहुंच असमान बनी हुई है।
सफल स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में भी, वित्तीय स्वायत्तता अक्सर घरेलू स्तर पर बिखर सी जाती है, जहाँ पति या ससुराल वाले अंतिम खर्च के फैसले लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि घरेलू स्तर पर वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में उनकी भागीदारी होती है परंतु इस संदर्भ में निर्णय लेने की शक्ति उनके पास नहीं होती।
स्कूलों और उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में, विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करने में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों ने शिक्षा को राष्ट्रीय एजेंडे का मुख्य हिस्सा बना दिया है।
हालांकि, कम उम्र में शादी, घरेलू जिम्मेदारियों या सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण माध्यमिक विद्यालय के बाद लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने की दर बढ़ जाती है। यहां तक कि शिक्षित महिलाएं भी अक्सर कार्यबल से हट जाती हैं या उन्हें रूढ़िवादी भूमिकाओं में डाल दिया जाता है। शैक्षणिक प्रतिभा अक्सर प्रशासनिक या बौद्धिक नेतृत्व की ओर नहीं ले जाती।
इसके अलावा, स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में अक्सर महिलाओं के दृष्टिकोण या महिलाओं के हित को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। जैसा कि विद्वान उमा चक्रवर्ती ने कहा है, सच्ची शिक्षा केवल सक्षम बनाने के लिए नहीं बल्कि मुक्ति देने के लिए भी होनी चाहिए। अन्यथा, व्यवस्था शिक्षित महिलाओं को केवल अनुरूप बनने के लिए तैयार करता है, सवाल करने के लिए नहीं।
भारत में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मजबूत कानून हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम (2005), मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम (2017), और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम (2013)। हालाँकि, कागज़ पर लिखे अधिकार अक्सर ज़मीनी स्तर पर अप्रभावी साबित होते हैं। । कम सज़ा दर, सामाजिक कलंक और लंबी न्यायिक प्रक्रियाएँ उनकी प्रभावशीलता को कमज़ोर करती हैं।
उदाहरण के लिए, बलात्कार के मामलों में, पीड़ितों को अक्सर पुलिस और अदालतों से दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा के मामलों में, सामाजिक दबाव न्याय के बजाय समझौते की ओर ले जाता है। सुरक्षा तंत्र अक्सर धीमे, कम संसाधन वाले और पुरुष-प्रधान होते हैं।
जैसा कि न्यायमूर्ति लीला सेठ ने एक बार कहा था, “कानून दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन समाज को महिला को उसमें से गुजरने की अनुमति देनी चाहिए।” वास्तविक शक्ति केवल कानून बनाने में नहीं है, बल्कि उन सांस्कृतिक लोकाचारों को बदलने में निहित है जो उनका विरोध करते हैं।
समाज में अक्सर बहुत ही विरोधाभास देखने को मिलते हैं। जबकि महिलाओं को प्रतीकों और परंपराओं में सम्मानित किया जाता है, लेकिन उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रतिबंधों और असमान व्यवहार का सामना करना पड़ता है। आत्म-त्यागी, कर्तव्यनिष्ठ और चुप रहने वाली ‘भारतीय नारी’ की छवि परिवार, मीडिया और लोकप्रिय कल्पना पर हावी रहती है। मातृत्व और आज्ञाकारिता का महिमामंडन करने वाली फ़िल्में अक्सर निष्क्रिय भूमिकाओं को मजबूत करती हैं, तब भी जब वे महिलाओं को मुख्य भूमिकाओं में दिखाती हैं।
सामाजिक रीति-रिवाज़ अभी भी एक महिला के मूल्य को उसकी वैवाहिक स्थिति और संतान उत्पन्न करने की जैविक भूमिका से जोड़ते हैं। शिक्षित परिवारों में भी ‘आकांक्षा’ नहीं, बल्कि ‘समायोजन’ की अपेक्षा व्याप्त है। पितृसत्तात्मक मूल्यों को परंपरा के रूप में फिर से पेश किया जाता है जिससे असहमति जताने की स्थिति विचलन के रूप में दिखाई देती है।
जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने तर्क दिया था, “जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है।” लेकिन अधिकारों के बिना सम्मान, आवाज के बिना दृश्यता, एक खोखला आदर्श बना हुआ है।
डिजिटल युग ने अवसरों के समान होने का वादा किया है। महिला प्रभावशाली व्यक्ति, उद्यमी, कोडर और कार्यकर्ता शक्तिशाली ऑनलाइन हितों के रूप में उभरे हैं। डिजिटल इंडिया जैसी पहल का उद्देश्य पहुँच के अंतर को कम करना है। फिर भी, NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार, केवल ~33% भारतीय महिलाएँ ही इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि 55% पुरुष इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जो ग्रामीण भारत में और भी कम है।
इसके अलावा, ऑनलाइन दृश्यता महिलाओं को उत्पीड़न, ट्रोलिंग और धमकियों के प्रति सुभेद्य बनाती है, जिससे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जोखिम उत्पन्न होते हैं। लिसिप्रिया कंगुजम जैसी कार्यकर्ताओं को लैंगिक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, जो मुखर महिला उपस्थिति के प्रतिरोध को दर्शाता है। एल्गोरिदम पूर्वाग्रह, डिजिटल शिक्षा की कमी और सीमित तकनीकी भागीदारी महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाए गए माध्यम में अदृश्य बना देती है।
शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, यह मनोवैज्ञानिक भी होती है। कई महिलाएं, उपलब्धियों के बावजूद, इंपोस्टर सिंड्रोम, सबके सामने आ जाने के डर और चुप रहने की समस्या का शिकार हो जाती हैं। स्वीकृति पाने और संघर्ष से बचने की आदत के कारण, मुखरता को अक्सर महिलाओं में अहंकार समझ लिया जाता है।
भारतीय दर्शन आंतरिक मुक्ति को स्वीकार करता है। भगवद गीता सलाह देती है: “उद्धारेद् आत्मानात्मानम्”। व्यक्ति को स्वयं के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए। आंतरिक परिवर्तन, आत्म-मूल्य को पुनः प्राप्त करना, लिंग आधारित व्यवहार को भूलना, इस प्रकार वास्तविक शक्ति का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण है।
जब तक भीतर की जंजीरें नहीं टूट जातीं, तब तक बाहर की जंजीरें बनी रहेंगी।
हालाँकि, महिलाओं को एकरूपी तरीक़े से नज़रअंदाज़ नहीं किया जाता। दलित, आदिवासी, मुस्लिम, विकलांग और LGBTQ+ महिलाओं को कई स्तरों पर बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। हाथरस मामले (2020) ने उजागर किया कि कैसे जाति और लिंग बुनियादी सम्मान को नकारने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीति में, ज़्यादातर चुनी गई महिलाएँ प्रभावशाली जातियों से होती हैं। अर्थशास्त्र में, SHG या सरकारी लाभों तक पहुँच अक्सर सबसे कमज़ोर लोगों को बाहर कर देती है।
आदिवासी महिलाएँ, वन आंदोलनों में अपने नेतृत्व के बावजूद, शायद ही कभी राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा होती हैं। मुस्लिम महिलाएँ सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और पितृसत्ता के खिलाफ़ एक साथ संघर्ष करती हैं। इन बहुस्तरीय पहचानों को स्वीकार किए बिना, कोई भी सशक्तिकरण एजेंडा आंशिक ही रहता है।
वैश्विक स्तर पर, सत्ता संरचनाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। यहाँ तक कि लिंग कोटा वाले देश भी वास्तविक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करते हैं। आइसलैंड में, जिसे सबसे अधिक लिंग-समान राष्ट्र माना जाता है, महिलाओं को अभी भी उद्यमिता में असमान वित्तपोषण का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में केवल 10% का नेतृत्व महिलाएं करती हैं और 2023 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 127वें स्थान पर है।
SDG 5 (लैंगिक समानता) न केवल विकासशील देशों में बल्कि विकसित देशों में भी अधूरा है। इससे पता चलता है कि उपस्थिति एक आवश्यक कदम है, लेकिन अंतिम नहीं।
महिलाओं की दृश्यता और उनके वास्तविक सशक्तिकरण के बीच की खाई को पाटने के लिए एक व्यापक और सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानूनी और राजनीतिक सुधार आवश्यक हैं। इसमें विधायिकाओं में महिलाओं के लिए लंबे समय से लंबित 33% आरक्षण को लागू करना, कानूनों को अधिक लिंग-संवेदनशील बनाना और मजबूत फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से त्वरित न्याय सुनिश्चित करना शामिल है।
आर्थिक समावेशन को भागीदारी से आगे बढ़कर स्वामित्व और नियंत्रण तक पहुंचना चाहिए। इसका तात्पर्य है महिलाओं के बीच संपत्ति के स्वामित्व को प्रोत्साहित करना, समान वेतन सुनिश्चित करना, वित्तीय साक्षरता में सुधार करना और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों और उद्यमों के लिए मजबूत समर्थन प्रणाली बनाना।
शिक्षा और कौशल विकास बदलाव के लिए महत्वपूर्ण साधन बने हुए हैं। STEM शिक्षा को बढ़ावा देने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और युवा लड़कियों और महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए ताकि वे तेजी से बदलती दुनिया में कामयाब हो सकें। साथ ही, सांस्कृतिक आख्यान, विशेष रूप से मीडिया और शिक्षा के माध्यम से दर्शाए जाने वाले आख्यानों को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को सक्रिय रूप से चुनौती देने और महिला अनुभवों और रोल मॉडल के व्यापक स्पेक्ट्रम को उजागर करने के लिए बदलना चाहिए।
अंत में, सशक्तिकरण के लिए कोई भी दृष्टिकोण अंतःक्रियाशीलता में निहित होना चाहिए। नीतियों में हाशिये पर पड़े लोगों- दलित महिलाएँ, आदिवासी समुदाय, विकलांग महिलाएँ और अन्य कम प्रतिनिधित्व वाले समूह को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समावेशिता अभिकल्पना में अंतर्निहित हो, न कि बाद में जोड़ा जाए। तभी दृश्यता वास्तविक, व्यापक शक्ति में तब्दील हो सकती है।
कुछ लोगों का मानना है कि दृश्यता अपने आप में एक शक्तिशाली शक्ति है। यह मानदंडों को चुनौती देती है, रूढ़ियों को तोड़ती है, और परिवर्तन को संभव बनाकर अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है। टेसी थॉमस, इंद्रा नूयी और पी.वी. सिंधु जैसे व्यक्तित्वों द्वारा उदाहरण के तौर पर सिविल सेवा, विज्ञान और खेल जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति, प्रगति और आकांक्षा की किरण के रूप में कार्य करती है।
हालांकि, ये व्यक्तिगत सफलताएँ, महत्वपूर्ण होते हुए भी, प्रतीकात्मक बन सकती हैं यदि उनके साथ गहरे प्रणालीगत परिवर्तन न हों। सत्ता, संपत्ति और विशेषाधिकार के पुनर्वितरण के बिना, अकेले प्रतिनिधित्व को ही अधिक प्राथमिकता देने में जोखिम है। वास्तविक सशक्तिकरण दृश्यता से कहीं ज़्यादा की मांग करता है। इसके लिए वास्तविक, संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता होती है जो समाज के सभी स्तरों पर महिलाओं की एजेंसी और प्रभाव का विस्तार करते हैं।
आज दुनिया एक अद्वितीय चौराहे पर खड़ी है। महिलाओं की दृश्यता निर्विवाद है, फिर भी नाजुक है। सत्ता की संरचना काफी हद तक पुरुष-प्रधान है, जो गहन सांस्कृतिक परंपराओं, संस्थागत जड़ता और मौन प्रतिरोध द्वारा आकार लेती है। लेकिन दृश्यता अर्थहीन नहीं है। इसे परिवर्तन के प्रवेश द्वार में बदलने के लिए, दुनिया को न केवल सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के शरीर के लिए जगह बनानी चाहिए, बल्कि निर्णय लेने में उनके दिमाग और भविष्य को नया आकार देने में उनके हितों के लिए भी जगह बनानी चाहिए।
वास्तविक सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाएँ केवल सुर्खियों में ही नहीं दिखतीं, बल्कि नीतियों, अर्थव्यवस्थाओं, परिवारों और आख्यानों के पीछे अदृश्य शक्तियाँ हैं। केवल दिखाई नहीं देतीं, बल्कि उन पर ध्यान भी दिया जाता है। केवल मौजूद नहीं, बल्कि शक्तिशाली भी।
जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है:
“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:”
“जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं।”
अब समय आ गया है कि हम सम्मान को रस्म/प्रथा मानने से आगे बढ़कर सत्ता को अधिकार के रूप में स्वीकार करें।
| PWOnlyIAS विशेष:
प्रासंगिक उद्धरण:
|
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">
</div>
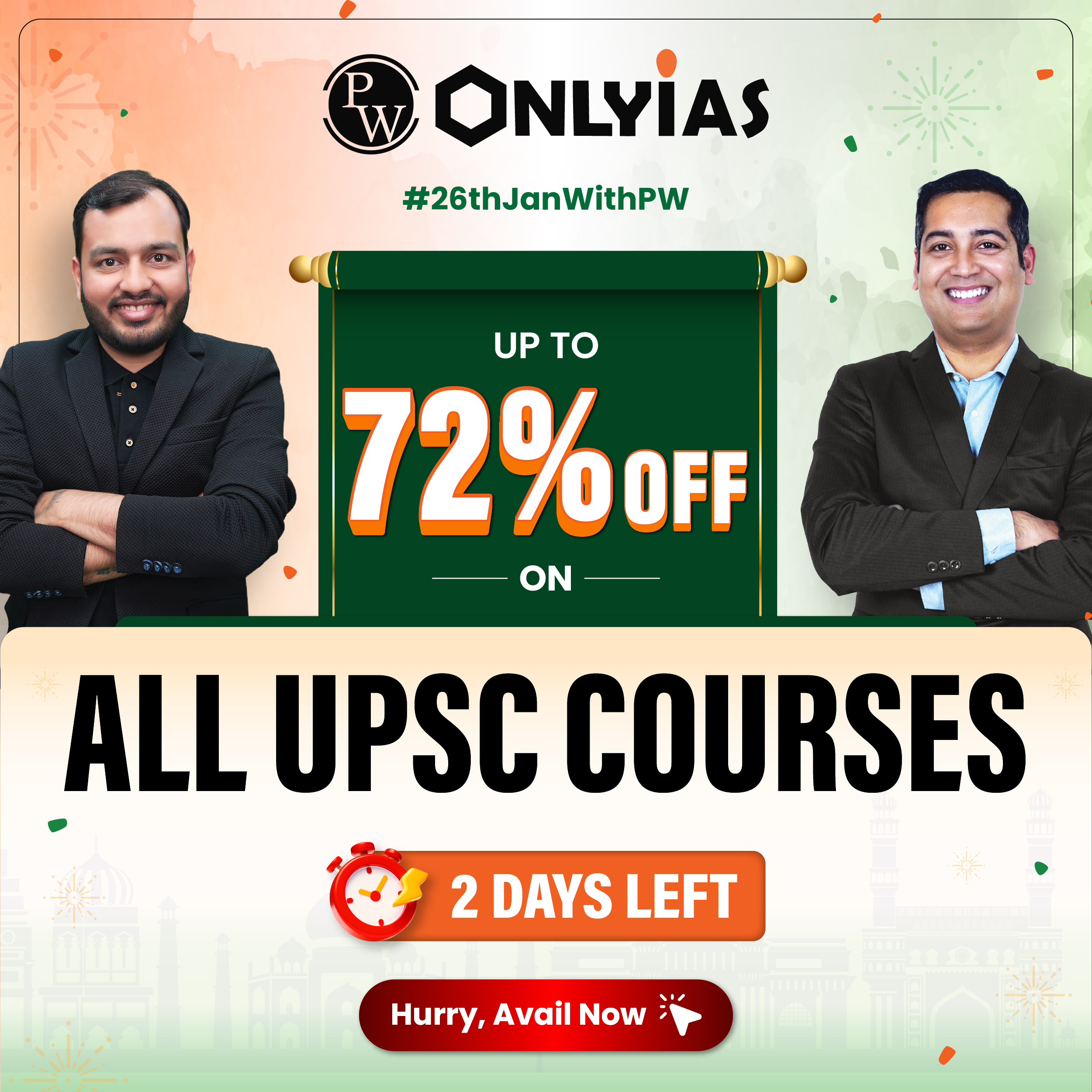
Latest Comments