प्रश्न की मुख्य माँग
- विकास प्रयासों के बावजूद मलिन बस्तियों के प्रसार के पीछे प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए।
- इस मुद्दे के समाधान के लिए दीर्घकालिक संधारणीय समाधान सुझाइए।
|
उत्तर
सरकारी अनुमानों के अनुसार, भारत में लगभग 34% शहरीकरण हो चुका है और 10-25% लोग अनधिकृत निर्माणों में रहते हैं, जो एक प्रकार से शहरी संकट का संकेत है। तीव्र विकास योजनाओं और शहरी नवीनीकरण के प्रयासों के बावजूद, मलिन बस्तियों का प्रसार निरंतर नीतिगत, आर्थिक और नियोजन विफलताओं को दर्शाता है।
शहरी भारत में झुग्गी बस्तियों के प्रसार के कारण
- शहरों में संपत्ति की ऊँची कीमतें: महानगरों में जमीन की बढ़ती कीमतें गरीबों को अवैध आवासों में रहने पर मजबूर करती हैं।
- उदाहरण के लिए: मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में, शहरी गरीबों के लिए बाजार में उपलब्ध आवास अफोर्डेबल नहीं हैं, जिससे झुग्गी-झोपड़ियों में एक समानांतर कम लागत वाले आवास का परिवेश बन रहा है।
- समानांतर अर्द्ध-कानूनी आवास बाजार: जहाँ औपचारिक आवास विफल हो जाता है, वहाँ अनौपचारिक अचल संपत्ति व्यवस्थाएँ उभरती हैं।
- उदाहरण के लिए: शैडो हाउसिंग अर्थव्यवस्था अनौपचारिक किरायेदारी और अतिक्रमण जैसी गतिविधियों पर आधारित होती है, जो कानूनी अस्पष्टताओं के चलते कम लागत वाले आवास विकल्प प्रदान करती है।
- नीतिगत अस्पष्टता और नौकरशाही दुविधा: अधिकारीगण विध्वंस और पुनर्वास के बीच दुविधा में हैं।
- शहरी नियोजन का अल्पकालिक फोकस: शहर अनौपचारिक आवास के मूल कारणों पर नहीं, बल्कि लक्षणों पर ध्यान देते हैं।
- उदाहरण के लिए: बड़े पैमाने पर किफायती आवास या बुनियादी ढाँचे के लिए व्यवस्थित योजना के बिना ही तोड़फोड़ और पुनर्वास अभियान चलाए जाते हैं।
- सीमित शहरी आवास आपूर्ति: भारत में भूमि का उपयोग उचित रूप से नहीं किया जाता है और शहरी आवास पहलों को बढ़ाने में भी विफलता ही देखी गई है।
- उदाहरण: शीर्ष 10 शहर भारत की कुल भूमि का केवल 0.2% हिस्से को आच्छादित करते हैं, फिर भी परिधीय क्षेत्रों में विस्तार न होने के कारण वे घनी आबादी वाले बने हुए हैं।
- रोजगार और आवास स्थानों के बीच बेमेल: शहरी केंद्रों में रोजगार के अवसर आवास विकल्पों के अनुरूप नहीं होते।
- उदाहरण के लिए: केंद्रीय शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, किफायती दूर-दराज के इलाकों से आने-जाने के बजाय, आस-पास की झुग्गियों में रहना पसंद करते हैं।
झुग्गी-झोपड़ियों की वृद्धि को रोकने के लिए दीर्घकालिक संधारणीय समाधान
- नए शहरों या उपग्रह कस्बों का निर्माण: नए नियोजित शहरों का विकास करके शहरीकरण का विकेंद्रीकरण करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: 100 नए स्मार्ट शहरों की स्थगित योजना को पुनर्जीवित करने से महानगरों में भीड़भाड़ कम हो सकती है और नियोजित विकास के जरिए झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास को रोका जा सकता है।
- कम आवंटित शहरी भूमि का अधिक कुशलता से उपयोग करना: किफायती आवास के लिए अप्रयुक्त भूमि का लाभ उठाना चाहिए।
- उदाहरण: शीर्ष 10 शहरों द्वारा केवल 0.2% भूमि क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, बेहतर योजना और जोनिंग के माध्यम से भूमि का उपयोग करके आवास स्टॉक का विस्तार किया जा सकता है।
- भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए नीतिगत सुधार: शहरी विकास आवश्यकताओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में संशोधन करना चाहिए।
- किफायती और किराये के आवास में व्यापक निवेश: कम लागत वाले आवास क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए।
- उदाहरण: PMAY-Urban जैसी योजनाओं की सफलता के लिए प्रवासी श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने हेतु किराये के अतिरिक्त घटकों के साथ इसे दोहराने की आवश्यकता है।
- नए शहरों में श्रम गतिशीलता और रोजगार-संबंधी आवास: नए शहरी केंद्रों में रोजगार-संबंधी प्रवासन को बढ़ावा किया जाना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: मौजूदा शहरों के झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग बेहतर आवास और पूर्णकालिक नौकरियों वाले नए शहरों में जा सकते हैं, जिससे महानगरों पर दबाव कम होगा।
- शहरी शासन क्षमता को मजबूत करना: स्थानीय सरकारों को समग्र रूप से योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए।
- उदाहरण: दीर्घकालिक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शहरों को समर्पित शहरी भूमि-उपयोग प्राधिकरणों और आवास बोर्डों की आवश्यकता है।
- समावेशी जोनिंग और मिश्रित उपयोग विकास को लागू करना: सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी विकास में किफायती आवास का हिस्सा शामिल हो।
निष्कर्ष
भारतीय शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों का लगातार बढ़ता प्रसार, भूमि के व्यवस्थित रूप से कम उपयोग, दीर्घकालिक योजना के अभाव और नीतिगत जड़ता को दर्शाता है। इन सब को देखते हुए विध्वंस और त्वरित समाधानों से संरचनात्मक शहरी विस्तार की ओर एक बदलाव की आवश्यकता है। चूँकि भारत में शहरीकरण अभी भी 34% है, इसलिए नए शहरों और उपनगरों का विकास करना व्यवहार्य तथा आवश्यक दोनों है, जो समावेशी, संधारणीय आवास और रोजगार प्रदान करेगा। यह केवल सम्मान और स्वास्थ्य से ही संबंधित नहीं है, अपितु यह भारत के भविष्य के शहरी ताने-बाने को आकार देने से संबंधित है।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

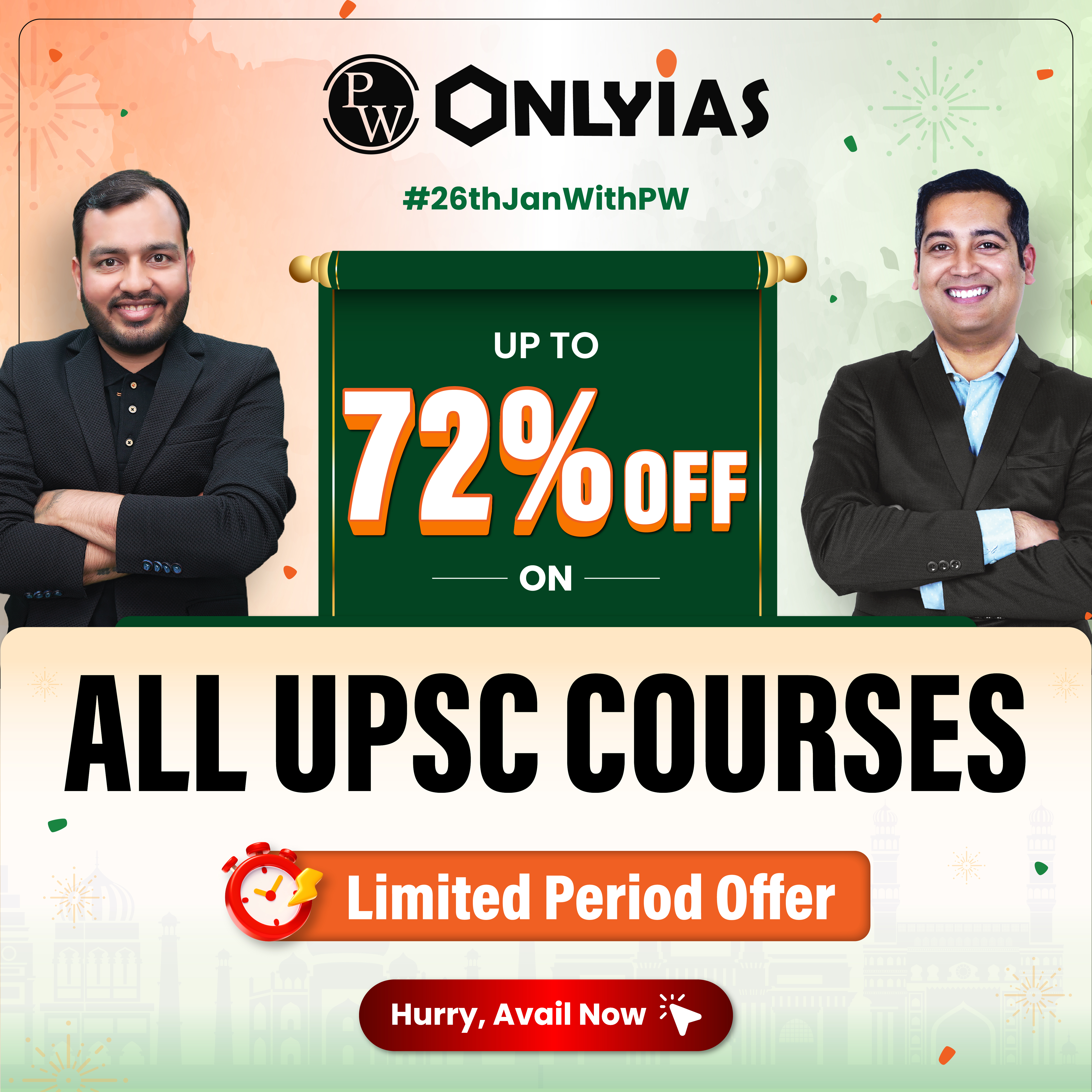
Latest Comments