प्रश्न की मुख्य माँग
- मौजूदा कानूनी और नीतिगत ढाँचों की प्रभावकारिता (शक्तियाँ और सीमाएँ)
- बेहतर रोकथाम और सहायता प्रणालियों के लिए सुधार या अतिरिक्त उपाय।
|
उत्तर
भारत में छात्रों की आत्महत्याएँ, विशेष रूप से युवाओं के बीच, एक गंभीर नैतिक और सामाजिक चिंता का विषय बन गई हैं। यद्यपि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (2017) और राष्ट्रीय आत्महत्या निवारण नीति (2021) कानूनी एवं नीतिगत ढाँचा प्रदान करते हैं, परंतु जागरूकता, संरचना और प्रवर्तन में व्याप्त कमियाँ इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सीमित करती हैं। अतः इनकी समीक्षा कर सुधार-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाना समय की आवश्यकता है।
A. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017
सकारात्मक पक्ष
- आत्महत्या के प्रयास का अपराधमुक्तीकरण: धारा 115 यह सुनिश्चित करती है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के बजाय देखभाल और परामर्श प्रदान किया जाए।
- उदाहरण: कर्नाटक और केरल में वर्ष 2017 के बाद छात्रों द्वारा आत्महत्या के प्रयासों की रिपोर्टिंग में वृद्धि दर्ज की गई।
- मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार: सभी छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।
- उदाहरण: दिल्ली और बंगलूरू के विश्वविद्यालयों में निःशुल्क परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
- अनिवार्य जागरूकता कार्यक्रम: विद्यालयों और कॉलेजों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अपेक्षा की गई है।
- उदाहरण: कुछ CBSE-मान्यता प्राप्त विद्यालयों ने पीयर-काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं।
सीमाएँ
- प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी: अधिकांश संस्थानों में योग्य मनोवैज्ञानिकों का अभाव है।
- उदाहरण: AIIMS (वर्ष 2023) के सर्वेक्षण के अनुसार, 70% भारतीय कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर नहीं हैं।
- प्रवर्तन की कमजोरी: ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में निगरानी और कार्यान्वयन कमजोर है।
- उदाहरण: बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में प्रशासनिक बाधाओं के कारण नीति के कार्यान्वयन में देरी हुई।
B. राष्ट्रीय आत्महत्या निवारण नीति, 2021
सकारात्मक पक्ष
- निवारक दृष्टिकोण: उच्च जोखिम वाले समूहों, विशेषकर छात्रों के लिए शीघ्र पहचान, जागरूकता और हस्तक्षेप पर बल।
- उदाहरण: महाराष्ट्र में शिक्षकों को आत्महत्या के चेतावनी संकेत पहचानने के लिए प्रशिक्षण दिया गया।
- बहु-क्षेत्रीय सहयोग: शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा।
- उदाहरण: केरल का स्टेट टास्क फोर्स शिक्षा और स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच समन्वित हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है।
- सामुदायिक भागीदारी: अभिभावकों, NGOs, और साथियों की भागीदारी को प्रोत्साहन।
- उदाहरण: iCall और वंडरेवाला फाउंडेशन जैसी NGOs हेल्पलाइन और पीयर-सपोर्ट कार्यक्रम संचालित करती हैं।
सीमाएँ
- कार्यान्वयन में विलंब: कई जिलों में आत्महत्या निवारण प्रकोष्ठ अभी तक कार्यशील नहीं हैं।
- उदाहरण: वर्ष 2024 तक उत्तर प्रदेश के 40% से अधिक जिलों में निगरानी प्रकोष्ठ सक्रिय नहीं थे।
- वित्त और डेटा की कमी: निरंतर वित्तीय सहयोग और केंद्रीकृत डेटा की अनुपलब्धता से नीति की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- उदाहरण: NCRB डेटा अक्सर छात्र आत्महत्याओं की रिपोर्टिंग में कमी दिखाता है, जिससे नीति मूल्यांकन कठिन हो जाता है।
सुधार और अतिरिक्त उपाय
- परामर्श संरचना को सशक्त बनाना: प्रत्येक विद्यालय और कॉलेज में प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की नियुक्ति अनिवार्य की जाए।
- उदाहरण: AIIMS और NIMHANS द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-काउंसलिंग नेटवर्क स्थापित किए जा रहे हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम की अनिवार्यता: मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
- उदाहरण: दिल्ली सरकार का लाइफ स्किल्स और इमोशनल रेजिलिएंस पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट।
- डिजिटल हेल्पलाइन और AI-आधारित निगरानी: तकनीक के माध्यम से 24×7 सहायता और जोखिमग्रस्त छात्रों की पहचान की जा सकती है।
- उदाहरण: विंडरेवाला फाउंडेशन और iCall AI चैटबॉट्स के माध्यम से तनाव की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर रही हैं।
- सामुदायिक एवं पारिवारिक भागीदारी: अभिभावकों के लिए जागरूकता शिविर और व्यवहारिक संकेत पहचानने का प्रशिक्षण।
- उदाहरण: महाराष्ट्र के जिलों में अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
- डेटा संग्रह और मूल्यांकन को सुदृढ़ करना: केंद्रीकृत रिपोर्टिंग प्रणाली और आवधिक नीति ऑडिट लागू किए जाएँ।
- उदाहरण: NCRB और राज्य शिक्षा विभागों के सहयोग से हस्तक्षेपों की निगरानी।
निष्कर्ष
यद्यपि मौजूदा नीतियाँ एक ठोस आधार प्रदान करती हैं, परंतु परामर्श संरचना का सुदृढ़ीकरण, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, तकनीकी समर्थन, सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शी निगरानी प्रणाली आवश्यक है। ऐसा सुधारात्मक दृष्टिकोण न केवल छात्रों के मानसिक कल्याण को सशक्त करेगा बल्कि नैतिक, समावेशी और विश्वासपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में भी एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

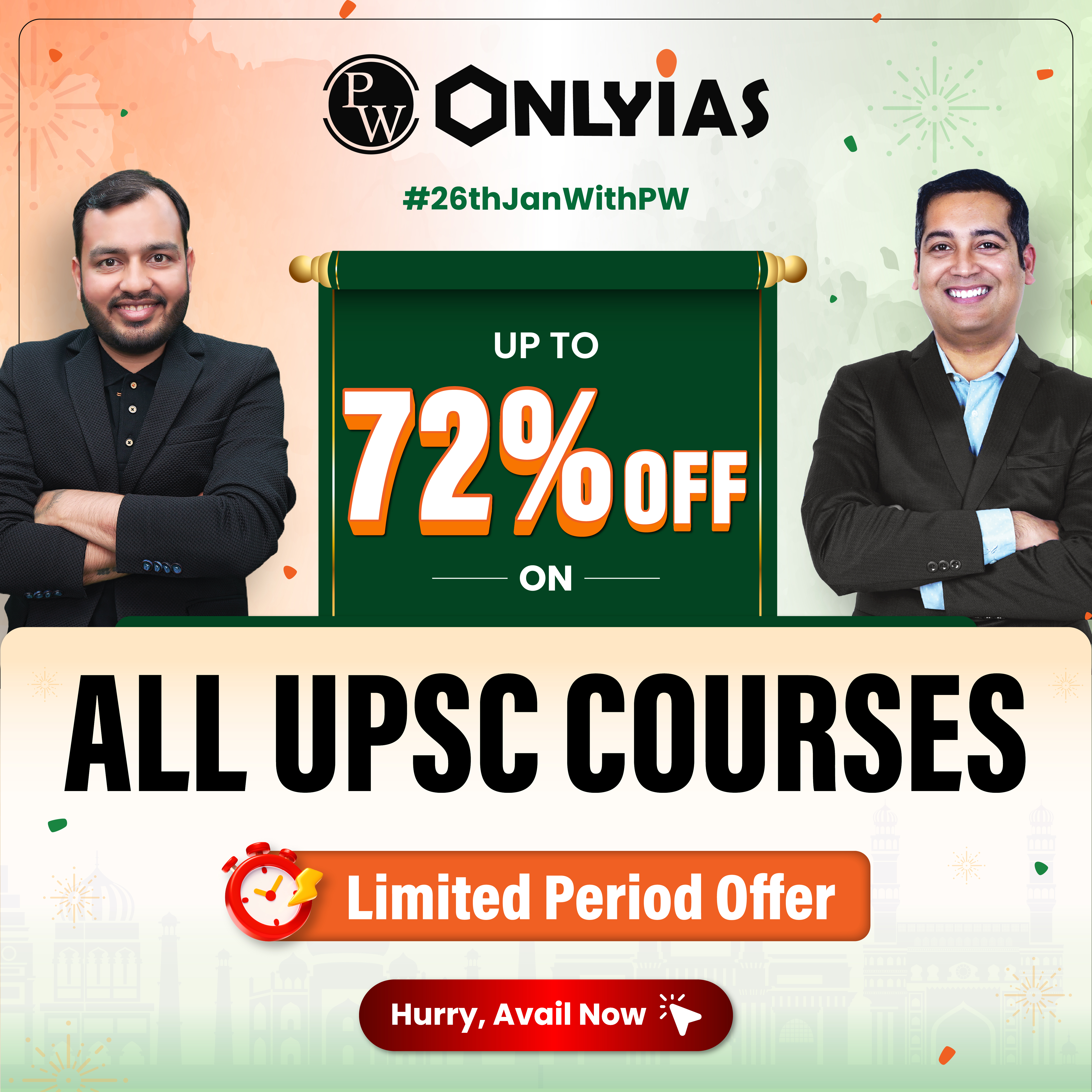
Latest Comments