प्रश्न की मुख्य माँग
- सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के बीच अंतर
- भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से संबंधित प्रमुख चिंताएँ
- इस ढाँचे को अधिक मानवीय और कुशल बनाने के उपाय
|
उत्तर
यूथेनेशिया (Euthanasia) का अर्थ है, कष्ट को दूर करने के लिए जानबूझकर जीवन का अंत करना। यह आत्मनिर्णय और गरिमा से मृत्यु से संबंधित नैतिक, सामाजिक और कानूनी प्रश्नों को जन्म देता है। भारत में, सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा शानबाग (2011) और कॉमन कॉज (2018) मामलों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सख्त शर्तों के साथ मान्यता दी, और अनुच्छेद-21 के अंतर्गत “गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार” को शामिल किया। तथापि, इसकी रूपरेखा अभी भी जटिल और अधिकांश लोगों के लिए अप्राप्य है।
सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में अंतर
| पहलू |
सक्रिय इच्छा मृत्यु |
निष्क्रिय इच्छा मृत्यु |
| अर्थ |
जानबूझकर किसी क्रिया द्वारा मृत्यु लाना (जैसे — विषाक्त इंजेक्शन देना)। |
जीवन को लंबा करने वाले उपचार यंत्रों को रोकना या हटाना (जैसे — वेंटिलेटर हटाना)। |
| कार्य की प्रकृति |
मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। |
प्राकृतिक मृत्यु को होने देना, बिना हस्तक्षेप के। |
| भारत में वैधता |
अवैध — भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत दंडनीय अपराध। |
कानूनी — सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (वर्ष 2011, वर्ष 2018) द्वारा मान्यता प्राप्त। |
| नैतिक दृष्टिकोण |
नैतिक रूप से हत्या के समान माना जाता है। |
प्रकृति को अपना कार्य करने देने के समान माना जाता है। |
| उदाहरण |
हृदय गति रोकने हेतु पोटैशियम क्लोराइड इंजेक्शन देना। |
बेहोश रोगी के जीवन समर्थन उपकरण को हटाना जब सुधार की कोई संभावना न हो। |
भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ
- प्रक्रियात्मक जटिलता: मेडिकल बोर्ड, अस्पताल समिति और कभी-कभी न्यायालय से कई अनुमतियाँ आवश्यक होती हैं, जिससे प्रक्रिया अत्यंत धीमी और कठिन हो जाती है। कई अस्पतालों में एथिक्स कमेटी (Ethics Committee) ही नहीं हैं।
- दुरुपयोग की आशंका: यह भय रहता है कि परिजन आर्थिक या उत्तराधिकार के कारण दबाव डाल सकते हैं या प्रावधान का दुरुपयोग कर सकते हैं।
- जागरूकता की कमी: डॉक्टरों और परिवारों को लिविंग विल (Living Will) या कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती, जिससे भ्रम और संकोच उत्पन्न होता है।
- क़ानूनी अस्पष्टता: वर्तमान ढाँचा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों पर आधारित है, कोई संपूर्ण वैधानिक कानून नहीं है।
- सांस्कृतिक एवं धार्मिक संवेदनशीलता: भारतीय समाज में जीवन को पवित्र (Sacred) माना जाता है, अतः यूथेनेशिया को नैतिक रूप से गलत समझा जाता है।
- अपर्याप्त उपशामक देखभाल: हॉस्पिस या परामर्श सेवाओं की कमी के कारण परिवार अक्सर भावनात्मक संकट में निर्णय लेने को विवश होते हैं।
ढाँचे को अधिक मानवीय और प्रभावी बनाने के उपाय
- व्यापक कानून बनाना: सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को संहिताबद्ध करते हुए एक “एंड-ऑफ-लाइफ केयर एक्ट (End-of-Life Care Act)” बनाया जाए, जिसमें स्पष्ट प्रक्रिया, अधिकार और सुरक्षा प्रावधान हों।
- डिजिटल रजिस्ट्री का निर्माण: नागरिकों के लिए आधार-लिंक्ड ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए, जहाँ वे लिविंग विल दर्ज, संशोधित या निरस्त कर सकें, जिसे अस्पतालों द्वारा एक्सेस किया जा सके।
- अस्पतालों की एथिक्स कमेटियों को सशक्त बनाना: तृतीयक अस्पतालों में अनिवार्य एथिक्स बोर्ड स्थापित किए जाएँ ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा हाईकोर्ट की अनुमति के बिना किया जा सके।
- विकेंद्रीकृत निगरानी प्रणाली: प्रत्येक जिले में निगरानी पैनल और डिजिटल डैशबोर्ड बनाए जाएँ, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और दुरुपयोग रोका जा सके।
- सुरक्षा प्रावधान: कूलिंग-ऑफ अवधि, थर्ड-पार्टी सत्यापन, और हितों के टकराव की जाँच जैसे सुरक्षा उपाय अनिवार्य किए जाएँ।
- डॉक्टरों के लिए कानूनी सुरक्षा: जो डॉक्टर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं, उन्हें कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे नैतिक रूप से निर्णय लेने में संकोच न करें।
- पैलिएटिव और हॉस्पिस केयर का विस्तार: दर्द प्रबंधन, परामर्श और सामुदायिक देखभाल को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में शामिल किया जाए।
- उदाहरण: केरल का सामुदायिक-आधारित पैलिएटिव केयर मॉडल देशभर में लागू किया जा सकता है।
निष्कर्ष
निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में गरिमा के संवैधानिक वादे को साकार करता है। परंतु जटिल प्रक्रिया, अस्पष्ट कानून और जागरूकता की कमी इसकी मानवीय भावना को सीमित करती है। यदि संपूर्ण कानून, डिजिटल संरचना, नैतिक प्रशिक्षण और उपशामक देखभाल को सुदृढ़ किया जाए, तो यह व्यवस्था करुणामय, प्रभावी और सभी के लिए सुलभ बन सकती है — जिससे भारत में गरिमा का अधिकार केवल जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि मृत्यु तक विस्तारित हो सके।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

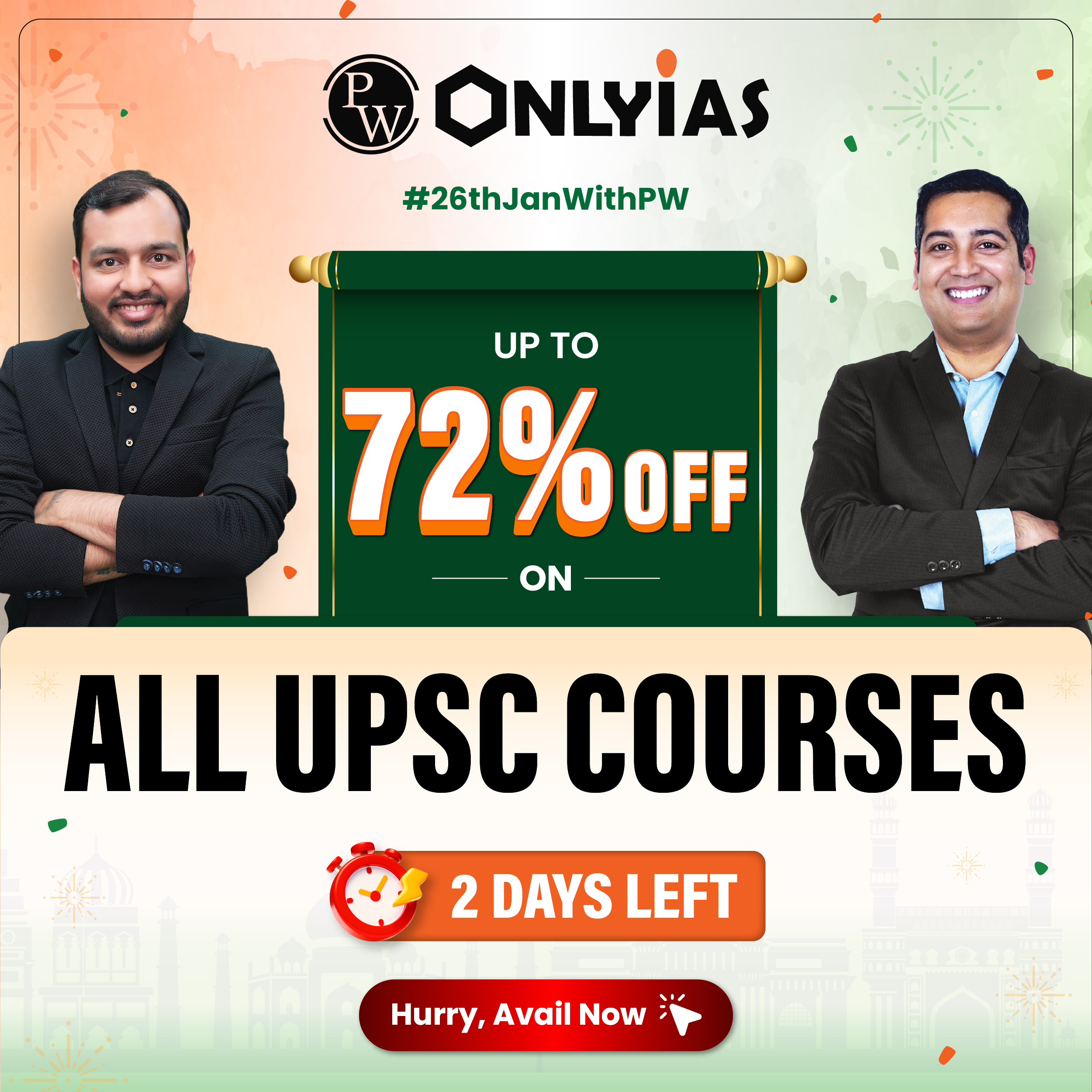
Latest Comments