प्रश्न की मुख्य माँग
- भारत के सोलर सिस्टम के विकास में योगदान देने वाले कारक।
- इसके विकास में नीतिगत, इन्फ्रास्ट्रक्चरल और वित्तीय बाधाओं पर चर्चा कीजिए।
- आगे की राह
|
उत्तर
भारत, जो अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन चुका है, वर्ष 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। सौर ऊर्जा इस परिवर्तन का प्रमुख चालक है, किंतु उच्च लागत, सीमित अपनाने, और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा इसके दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए चुनौती प्रस्तुत करती हैं।
भारत के सौर क्षेत्र की वृद्धि में योगदान देने वाले कारक
- स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धता: भारत की स्वच्छ ऊर्जा नीति ने सौर निवेश और साझेदारी को बढ़ावा दिया है, जिसमें पेरिस समझौते के तहत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य में से 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है।
- सौर ऊर्जा की लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता: वर्ष 2017 में सौर ऊर्जा की प्रति इकाई लागत कोयले से कम हो गई, जिससे यह व्यवसायों के लिए एक आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प बन गई।
- उदाहरण: भारत में सौर टैरिफ लगभग ₹2.5 प्रति यूनिट तक गिर गए हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम दरों में से एक हैं।
- घरेलू विनिर्माण क्षमता में विस्तार: सरकारी प्रोत्साहन और निजी निवेश के कारण सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता वर्ष 2014 में 2 गीगावाट से बढ़कर 2025 तक लगभग 100 गीगावाट तक पहुँच गई है।
- अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और बाजार विस्तार: भारत की अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में नेतृत्व भूमिका ने वैश्विक सौर सहयोग को बढ़ावा दिया है, विशेषकर अफ्रीकी देशों के साथ, जिससे ऊर्जा कूटनीति और निर्यात क्षमता मजबूत हुई है।
- उदाहरण: ISA के तहत भारत का अफ्रीकी देशों को सौर आपूर्तिकर्ता बनना बाजार विविधीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।
- प्रौद्योगिकी और ग्रामीण एकीकरण प्रयास: प्रधानमंत्री कुसुम योजना (ग्रामीण सौर सिंचाई हेतु) और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने हेतु) जैसी पहलें सौर ऊर्जा को विकेंद्रीकृत करने और घरेलू माँग बढ़ाने का कार्य कर रही हैं।
नीतिगत, अवसंरचनात्मक और वित्तीय चुनौतियाँ
नीतिगत चुनौतियाँ
- योजनाओं के असंगत क्रियान्वयन: प्रधानमंत्री कुसुम योजना जैसी नीतियों के क्रियान्वयन में देरी और असमानता ने ग्रामीण सौर अवसंरचना के विकास को सीमित किया है।
- व्यापार और शुल्क अस्थिरता: सौर घटकों पर उच्च आयात शुल्क, उत्पादन लागत बढ़ाते हैं, जबकि अस्पष्ट निर्यात नीतियाँ वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को सीमित करती हैं।
अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ
- ग्रिड एकीकरण और भंडारण सीमाएँ: कमजोर ग्रिड संरचना और ऊर्जा भंडारण की अपर्याप्तता बड़े पैमाने पर नवीकरणीय एकीकरण में बाधा बनती हैं।
- भूमि और प्रसारण संबंधी कठिनाइयाँ: सौर पार्कों के लिए भूमि अधिग्रहण और अंतिम कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना अभी भी एक मुख्य लॉजिस्टिक चुनौती है।
वित्तीय चुनौतियाँ
- कम लागत वाले वित्त तक सीमित पहुँच: उच्च ब्याज दरें और सीमित ऋण उपलब्धता लघु एवं मध्यम सौर उद्योगों के लिए बाधा हैं।
- आयात के मुकाबले मूल्य असंतुलन: घरेलू मॉड्यूल की लागत चीनी मॉड्यूल्स की तुलना में 1.5–2 गुना अधिक है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्द्धा और लाभांश प्रभावित होते हैं।
आगे की राह
- घरेलू प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना: आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करना, पॉलीसिलिकॉन और वेफर निर्माण का विस्तार करें, तथा R&D को प्रोत्साहन दें ताकि चीन के साथ लागत का अंतर घटाया जा सके।
- नीति और वित्तीय ढाँचे में सुधार: परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया सरल करना, ब्याज सब्सिडी प्रदान करना, और ग्रीन बॉण्ड्स व सॉवरेन गारंटी जैसे वित्तीय उपकरणों का विस्तार करना।
- वैश्विक बाजार एकीकरण को बढ़ावा देना: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के माध्यम से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय सौर उत्पादों के बाजार विकसित किए जाएँ।
- अवसंरचना और भंडारण सुधार: ग्रिड आधुनिकीकरण, हाइब्रिड नवीकरणीय प्रणाली, और स्वदेशी बैटरी तकनीक में निवेश बढ़ाया जाए, ताकि स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- समावेशी सौर अपनाने को प्रोत्साहन देना: रूफटॉप सौर और ग्रामीण सौर योजनाओं को गति दी जाए, ताकि घरेलू माँग बढ़े और नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार रोजगार और स्थिरता लक्ष्यों से जोड़ा जा सके।
निष्कर्ष
भारत का सौर क्षेत्र स्वच्छ विकास को आगे बढ़ा सकता है, यदि महत्त्वाकांक्षा और क्रियान्वयन के बीच की खाई को स्थिर नीति, वित्तीय नवाचार, और आधुनिक अवसंरचना के माध्यम से पाटा जाए। यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक नवीकरणीय नेतृत्व की दिशा में अग्रसर करेगा।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

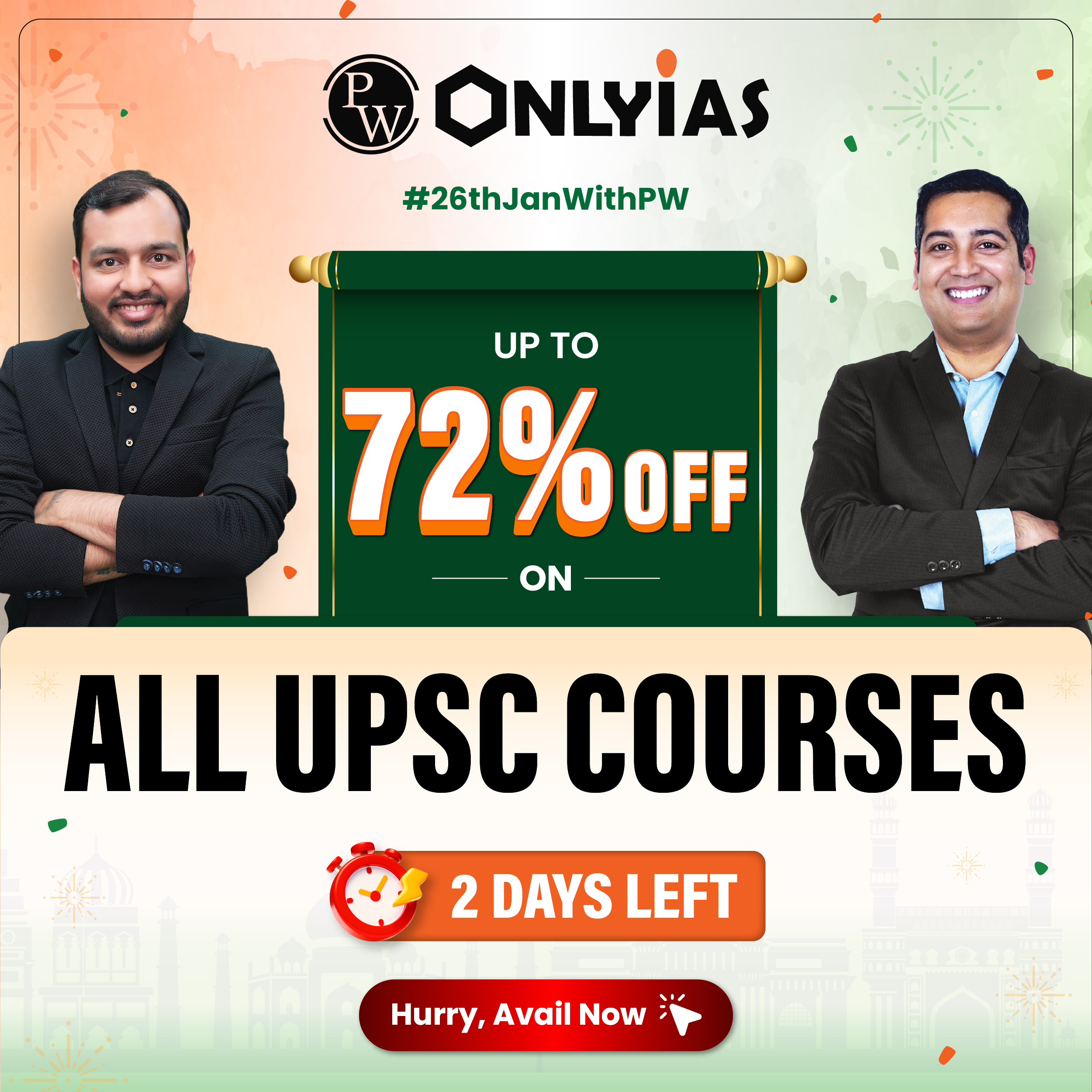
Latest Comments