प्रश्न की मुख्य माँग
- भारत ने लगभग एक शताब्दी में विज्ञान का कोई नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया है?
- नोबेल स्तर के अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रतिभा को बनाए रखने के लिए प्रणालीगत सुधार।
|
उत्तर
भारत ने वर्ष 1930 में सी. वी. रमन (भौतिकी) के बाद से कोई विज्ञान का नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है, जबकि उसके पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक कार्यबल है। फिर भी, अनुसंधान एवं विकास निवेश लगभग 0.7% GDP पर अटका हुआ है जो वैश्विक नवाचार की तुलना में बहुत कम है जिसके कारण वैज्ञानिक प्रतिभा ऐसी प्रणालियों में फँसी हुई है जो मौलिकता की बजाय आज्ञाकारिता को अधिक महत्त्व देती हैं।
क्यों भारत लगभग एक सदी से विज्ञान का नोबेल नहीं ला पाया है
- नवाचार को सक्षम करने के बजाय नियंत्रण करने वाला नेतृत्व: अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिक स्वतंत्रता की बजाय प्रशासनिक नियंत्रण को प्राथमिकता देते हैं, जिससे रचनात्मक जोखिम लेने की क्षमता दब जाती है।
- उदाहरण: संस्थान “ब्यूरोक्रेटिक फोर्ट्रेस” (Bureaucratic fortresses) बन गए हैं, जहाँ नेतृत्व खोजकर्ताओं को सक्षम करने के बजाय उनकी राह रोकता है।
- गैर-मेरिट आधारित नियुक्ति और संरक्षणवाद की संस्कृति: प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को फैकल्टी के पद नहीं मिलते, जबकि सामान्य/क्रमिक शोध करने वाले आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि नियुक्तियाँ नेटवर्क, क्षेत्रीय झुकाव और संरक्षणवाद पर आधारित होती हैं।
- अनुसंधान संस्कृति मौलिकता नहीं, संख्या को पुरस्कृत करती है: अकादमिक जगत शोधपत्रों, पुरस्कारों और उद्धरणों की संख्या को महत्व देता है, मौलिकता या सामाजिक प्रभाव को नहीं।
- उदाहरण: वैज्ञानिक मेडल, फैलोशिप और सिटेशन के पीछे भागते हैं, जिससे मूल्य की बजाय दृश्यता और नवाचार की बजाय अनुकूलन को बढ़ावा मिलता है।
- ब्यूरोक्रेटिक बाधाएँ वैज्ञानिक ऊर्जा को निचोड़ती हैं: युवा वैज्ञानिक वर्षों तक आंतरिक राजनीति और प्रशासनिक जाल से संघर्ष करते रहते हैं, जिससे बड़े सपने देखने की प्रेरणा समाप्त हो जाती हैं।
- जोखिम से बचने वाला वरिष्ठ नेतृत्व परिवर्तन का विरोध करता है: निर्णयकर्ता परिवर्तनकारी विचारों की अपेक्षा स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, जिससे युवा वैज्ञानिकों को वैश्विक संपर्क से वंचित होना पड़ता है।
नोबेल-स्तर के अनुसंधान को पोषित करने और प्रतिभा को बनाए रखने हेतु प्रणालीगत सुधार
- पारदर्शी, मेरिट-आधारित भर्ती: खुली और गुणवत्ता-आधारित नियुक्तियाँ ताकि भारत के श्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थानों में प्रवेश पा सकें।
- दूरदर्शी नेतृत्व: संस्थान प्रमुखों का चयन प्रशासनिक वरिष्ठता नहीं, बल्कि वैज्ञानिक उत्कृष्टता और वैश्विक शोध उपलब्धियों के आधार पर होना चाहिए।
- उदाहरण: होमी भाभा और विक्रम साराभाई जैसा नेतृत्व आवश्यक है। कम से कम 50% नेतृत्व भूमिकाएँ युवा वैज्ञानिकों (40–50 वर्ष) के लिए खोली जानी चाहिए।
- वित्तपोषण शोध की गुणवत्ता से जुड़ा है, प्रकाशनों की संख्या से नहीं: वित्तपोषण को साहसिक, उच्च जोखिम, उच्च पुरस्कार वाले विज्ञान की ओर पुनर्निर्देशित करना।
- प्रशासनिक नियंत्रण पर वैज्ञानिक स्वायत्तता: निर्णय लेने की शक्ति बिना लंबी अनुमोदन प्रक्रियाओं के उपलब्ध हो, जिससे प्रयोगों की गति बढ़े और उच्च-जोखिम अनुसंधान को प्रोत्साहन मिले।
- आर एंड डी निवेश को वैश्विक मानकों तक बढ़ाना: अनुसंधान निवेश को कम से कम GDP के 3% तक ले जाना आवश्यक है ताकि प्रतिभा बनी रहे।
निष्कर्ष
भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी उस प्रणाली की है जो साहसिक विचारों को पुरस्कृत करे।
नोबेल-स्तर का विज्ञान अधिक धन नहीं, बल्कि मेरिटोक्रेसी, स्वायत्तता, दूरदर्शी नेतृत्व और पारदर्शी संस्थागत संस्कृति की माँग करता है। जब तक अकादमिकसुधारों को प्रारंभ नहीं किया जाता, भारत “संभावनाओं का देश” बना रहेगा।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

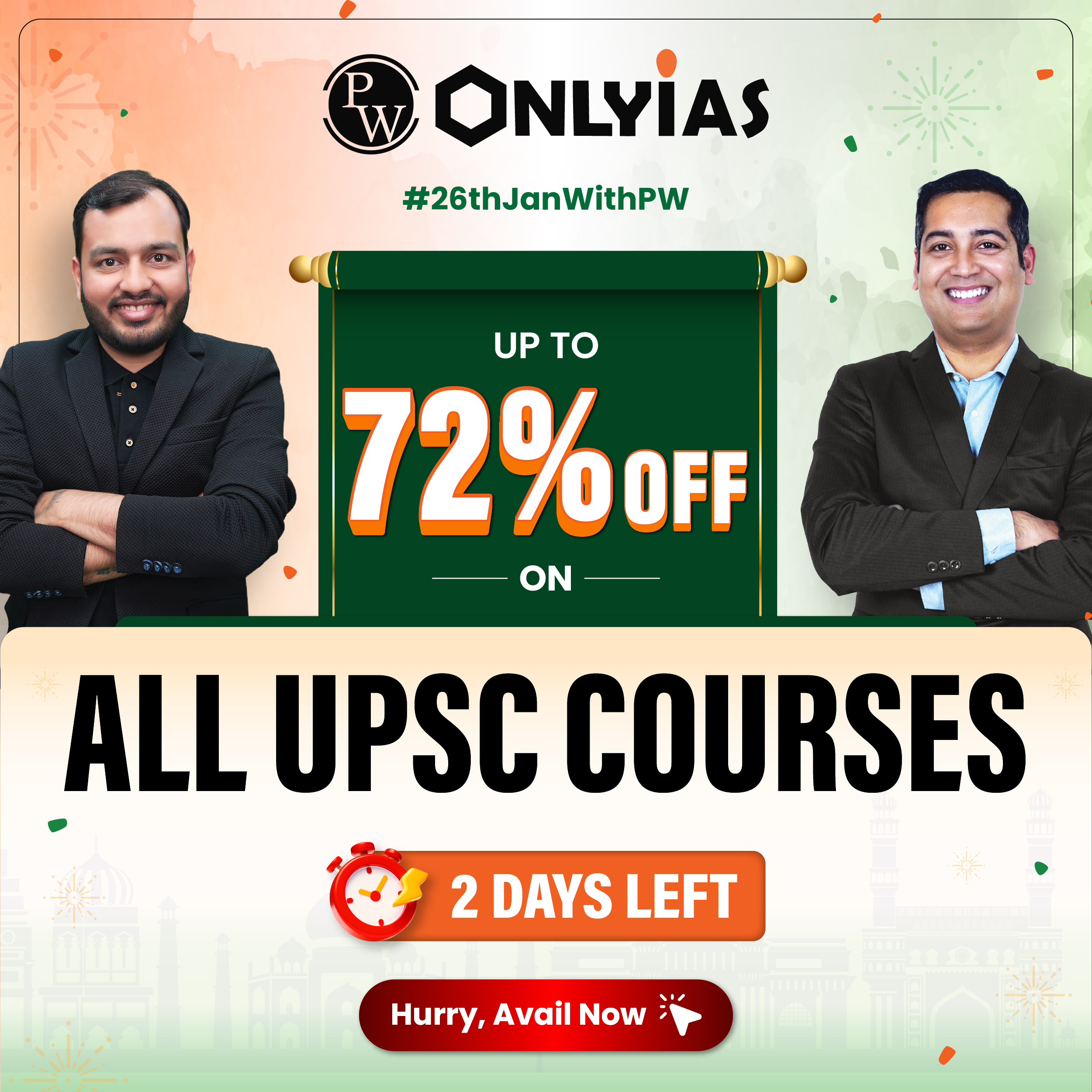
Latest Comments