प्रश्न की मुख्य माँग
- भारत में हिरासत में हिंसा के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार कारक।
- न्यायिक टिप्पणियों के निहितार्थ जो हिरासत में हिंसा को उचित या सामान्य ठहराते प्रतीत होते हैं।
- संवैधानिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और विधि के शासन को बनाए रखने के लिए मौलिक सुधार।
|
उत्तर
भारत में हिरासत में हिंसा, संवैधानिक अधिकारों के कमजोर प्रवर्तन, जातिगत पक्षपात और संस्थागत विफलताओं का परिचायक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (2021–22) के अनुसार, देश में लगभग 2,300 ऐसे मामले हुए हैं जहां हिरासत में मृत्यु हुई है। डी.के. बसु दिशानिर्देशों के बावजूद इस मामले को लेकर जवाबदेही का अभाव बना हुआ है, जिससे न्यायपालिका एवं पुलिस तंत्र पर जन विश्वास कमजोर पड़ता है।
भारत में हिरासत में होने वाली हिंसा के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार कारक
- संस्थागत दंडमुक्ति: स्वतंत्र जाँच न होने से प्रायः पुलिस ही स्वयं मामले की जाँच करती है, जिससे पक्षपातपूर्ण नतीजे सामने आते हैं।
- उदाहरण: NCRB की वार्षिक रिपोर्ट ‘क्राइम इन इंडिया’ के अनुसार, 2001 और 2020 के बीच हिरासत में 1,888 मौतें हुईं फिर भी केवल 26 पुलिसकर्मियों को ही दोषी ठहराया गया।
- न्यायिक देरी और कमज़ोर अभियोजन: विलम्बित सुनवाई अपराधियों को प्रोत्साहित करती है, जिससे उन पर अंकुश लगाने की क्षमता कम हो जाती है।
- उदाहरण: विंसेंट हिरासत में मृत्यु के वाद (तूतीकोरिन, 1999) में दोषसिद्धि तक पहुँचने में 25 साल लग गए।
- सामाजिक-जातीय पदानुक्रम: जाति और वर्गीय पूर्वाग्रहों के कारण हाशिए पर स्थित समुदायों को अक्सर असमान रूप से निशाना बनाया जाता है।
- उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि 1996 और 2018 के बीच हिरासत में हुई 71 प्रतिशत मौतें गरीब या सुभेद्य पृष्ठभूमि के बंदियों की थीं।
- निगरानी के उपकरण के रूप में यातना: अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के दबाव के कारण तीसरी डिग्री पद्धतियों (थर्ड-डिग्री मेथड्स) पर निर्भरता।
- उदाहरण के लिये: हाल ही में छत्तीसगढ़ की एक हिरासत में मृत्यु की घटना (2025) में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पीड़ित के शरीर पर 26 चोटों का खुलासा किया, जिसने कबूलनामा प्राप्त करने हेतु यातना के क्रूर उपयोग को उजागर किया।
- कमजोर निरीक्षण तंत्र: मानवाधिकार आयोग (Human Rights Commissions) के पास प्रवर्तन शक्तियों का अभाव है और इसकी सिफारिशों को प्रायः नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
हिरासत में हिंसा को सामान्य बनाने वाली न्यायिक टिप्पणियों के निहितार्थ
- राज्य की क्रूरता को सामान्य बनाना: जब न्यायालय हिंसा को “अनुशासन का साधन” (tool for discipline) के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वे विधि-प्रवर्तन और अतिरिक्त-वैधानिक दंड (extra-legal punishment) के बीच की सीमा को अस्पष्ट कर देते हैं।
- उदाहरण के लिए: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (2025) द्वारा हिरासत में हुई पिटाई को “सबक सिखाना” कहने से क्रूरता का सामान्यीकरण हुआ और इसने संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार किया।
- विधि के शासन का हनन: न्यायिक उदारता यह संकेत देती है कि राज्य की हिंसा सहनीय है, जिससे अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा के अधिकार) को दरकिनार किया जाता है।
- पीड़ितों के अधिकारों को कमजोर करना: क्रूरता के प्रति न्यायिक सहिष्णुता से हाशिए पर स्थित समुदायों को न्याय तक सार्थक पहुँच (meaningful access to justice) से वंचित किया जाता है और यह संस्थागत भेदभाव को स्थायी बना देती है।
- जन विश्वास को कमजोर करना: राज्य की हिंसा का समर्थन या उसकी अनदेखी, न्यायिक एवं विधिक संस्थाओं में जनसाधारण के विश्वास को क्षीण कर देती है।
- संवैधानिक नैतिकता का विकृतीकरण: गरिमा (dignity) और विधिक प्रक्रिया (due process) को अनिवार्य एवं अविच्छेद्य अधिकारों (inviolable rights) के रूप में न देखकर वैकल्पिक (optional) माना जाता है।
जनता के विश्वास और संवैधानिक मूल्यों को बहाल करने के लिए, न्यायिक और संस्थागत आत्मसंतुष्टि के स्थान पर शुद्ध सुधार लाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और विधि के शासन को बनाए रखने के लिए सुधार
- स्वतंत्र जाँच निकाय: पुलिस पदानुक्रम (hierarchy) से बाहर राज्य-स्तरीय कस्टोडियल डेथ इन्वेस्टिगेशन यूनिट (custodial death investigation units) की स्थापना की जानी चाहिए।
- सख्त न्यायिक जवाबदेही: उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय को हिरासत हिंसा (custodial violence) मामलों की नियमित निगरानी को अनिवार्य बनाना चाहिये।
- उदाहरण के लिए: डीके बसु वाद (वर्ष 1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिसकर्मियों पर स्पष्ट नामपट्टिकाएँ, गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार को देना और हर 48 घंटे में चिकित्सा जाँच जैसी सुरक्षा अनिवार्य कर दी थी।
- SC/ST अधिनियम के प्रवर्तन को सुदृढ़ करना: सभी जाति-प्रभावित हिरासत में हुई मृत्यु के मामले में अनुमानित जाति-पूर्वाग्रह प्रावधान लागू करना चाहिए।
- अनिवार्य प्रौद्योगिकी एकीकरण: सभी लॉकअप में CCTV कैमरे और बॉडीकैम लगाए जाएँ, जिनकी वास्तविक समय (real-time) पर मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानी की जाए।
- यातना-विरोधी कानून लागू करना: भारत ने वर्ष 1997 में यातना-विरोधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। हिरासत में यातना को अपराध घोषित करने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ घरेलू कानून आवश्यक है।
- पुलिस सुधारों को लागू करना: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (वर्ष 2006) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पूर्ण क्रियान्वयन किया जाए, जिनमें पुलिस विभाग की संवेदनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना शामिल है।
निष्कर्ष
हिरासत में होने वाली हिंसा एक प्रणालीगत चुनौती बनी हुई है, जो गरिमा, विधि के शासन (rule of law) और संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती है। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने इसे सही रूप में “सभ्य समाज का सबसे बड़ा अपराध” (worst crime in civilised society) कहा है, जो मज़बूत सुधारों, स्वतंत्र जवाबदेही तथा कठोर न्यायिक पर्यवेक्षण (strict judicial oversight) की माँग करता है ताकि सुभेद्य वर्गों की रक्षा की जा सके।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

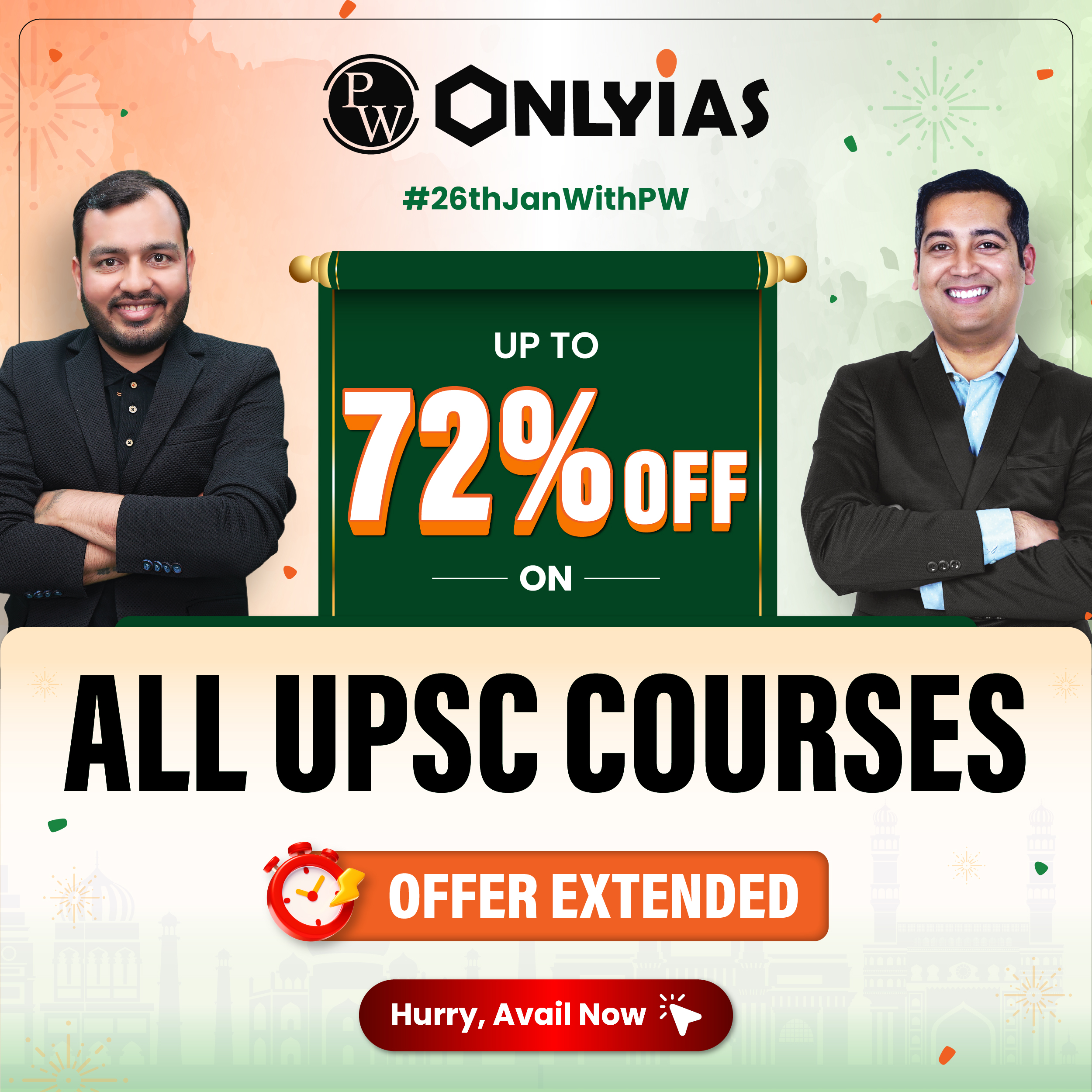
Latest Comments