प्रश्न की मुख्य माँग
- अनेक राष्ट्रीय नीतियों के बावजूद भारत में जल संकट के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए।
- उभरती जल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए आवश्यक सुधारों का सुझाव दीजिए।
|
उत्तर
भारत, जिसकी आबादी वैश्विक आबादी का 18% है, लेकिन मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4% है, दुनिया के सबसे गंभीर जल संकटों में से एक का सामना कर रहा है। कई राष्ट्रीय जल नीतियों और योजनाओं के बावजूद, भूजल की कमी, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे क्षेत्रों में जल तनाव को बढ़ा रहे हैं।
भारत में जल संकट
- उच्च भूजल निष्कर्षण: भारत विश्व के लगभग 25% भूजल का दोहन करता है जिसमें से 736 से अधिक इकाइयों (11%) को ‘अति-शोषित’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे जलभृत के ढहने और कुओं के सूखने का खतरा है।
- दूषित जल स्रोत: भारत का 70% जल प्रदूषित है; 230 मिलियन लोग फ्लोराइड और आर्सेनिक संदूषण के संपर्क में हैं।
- उदाहरण के लिए, जलजनित बीमारियों के कारण प्रत्येक वर्ष 200,000 से ज़्यादा मौतें होती हैं ( नीति आयोग, 2018)।
भारत में जल संकट के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक
- भूजल का अत्यधिक उपयोग: भारत में 85% से अधिक पेयजल और 60% से अधिक सिंचाई भूजल पर निर्भर करती है, जिससे भूजल का स्तर खतरनाक रूप से कम हो रहा है।
- उदाहरण के लिए, नीति आयोग के अनुसार, वर्ष 2030 तक दिल्ली और बेंगलुरु सहित 21 शहरों में भूजल स्तर खत्म हो सकता है।
- मानसून पर निर्भरता: भारत की कृषि मानसून पर निर्भर करती है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित हो गई है, जिससे जल उपलब्धता प्रभावित हो रही है।
- सूखा-प्रवण क्षेत्र: भारत की लगभग 33% भूमि सूखा-प्रवण है, जिसके कारण मिट्टी में आर्द्रता की कमी होती है और बार-बार कृषि हानि होती है। मराठवाड़ा क्षेत्र में लगातार सूखा पड़ता है, जिससे प्रतिवर्ष लाखों किसान प्रभावित होते हैं।
- ग्लेशियर पिघलना और जलवायु परिवर्तन: प्रारम्भ में नदी का प्रवाह बढ़ेगा, लेकिन ग्लेशियर के निर्वतन से अंततः मीठे पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी।
- असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ: चावल और गन्ना जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलें जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में हावी हैं, जिन्हें MSP प्रोत्साहनों से समर्थन मिलता है।
- उदाहरण: पंजाब और हरियाणा में भूजल संकट के बावजूद धान की कृषि जारी है।
- सूक्ष्म सिंचाई की उपेक्षा: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकें 50% तक पानी बचा सकती हैं, लेकिन वे केवल 9% कृषि भूमि को ही कवर करती हैं।
- शहरी अति प्रयोग और कुप्रबंधन: शहर बड़ी मात्रा में जल का उपभोग करते हैं और अपशिष्ट जल और वितरण का कुप्रबंधन करते हैं। वर्ष 2019 में चेन्नई में पानी सूख गया था और निवासियों को पानी की आपूर्ति के लिए जल रेलगाड़ियों पर निर्भर रहना पड़ा था।
उभरती जल चुनौतियों से निपटने के लिए सुधार
- सूक्ष्म सिंचाई कवरेज का विस्तार करना: कुशल सिंचाई विधियों के लिए सब्सिडी कवरेज और जागरूकता बढ़ानी चाहिए।
- अटल भूजल योजना को मजबूत करना: मौजूदा 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में समुदाय-नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, गुजरात में सहभागी जलभृत मानचित्रण से जल स्तर में सुधार हुआ।
- सौर ऊर्जा चालित सिंचाई को बढ़ावा देना: सब्सिडी वाली बिजली और भूजल निष्कर्षण पर निर्भरता कम करनी चाहिए।
- उदाहरण: KUSUM (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना ने सौर पंपों को प्रोत्साहित किया, संधारणीय सिंचाई को बढ़ावा दिया और भूजल के अत्यधिक दोहन को कम किया।
- जल मूल्य निर्धारण और मीटरिंग: तर्कसंगत मूल्य निर्धारण से अति उपयोग कम हो सकता है और दक्षता को बढ़ावा मिल सकता है।
- उदाहरण: चेन्नई के स्मार्ट मीटरिंग पायलट से घरेलू जल की बर्बादी में 18% की कमी आई।
- बांध आधुनिकीकरण और वर्षा जल संचयन: पुराने बुनियादी ढाँचे का जीर्णोद्धार करने के लिए बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) जैसी परियोजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, DRIP के तहत विश्व बैंक द्वारा 1 बिलियन डॉलर के निवेश से भारत भर में 300 बड़े बांधों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- एकीकृत नीति संरेखण: एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के माध्यम से ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों के साथ जल नीति को संरेखित करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य वर्ष 2025 तक जल-उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना है।
- निजी निवेश और नवाचार: सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाकर जल अवसंरचना में वित्त पोषण की कमी को पूरा करना।
- उदाहरण के लिए, दिल्ली में वाटर ATM को CSR और PPP मॉडल के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।
- जन भागीदारी: नियोजन और संरक्षण में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना चाहिये।
- उदाहरण: जल शक्ति अभियान ने बुंदेलखंड में स्थानीय भागीदारी के माध्यम से जल भंडारण संरचनाओं में सुधार किया।
भारत का जल संकट सिर्फ संसाधनों की चुनौती नहीं है, बल्कि यह शासन और व्यवहार की चुनौती भी है। इसे संबोधित करने के लिए विकेंद्रीकृत कार्रवाई, तकनीकी नवाचार, नीतिगत सुसंगतता और सबसे बढ़कर, भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण करने हेतु सक्रिय नागरिक भागीदारी की आवश्यकता है।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

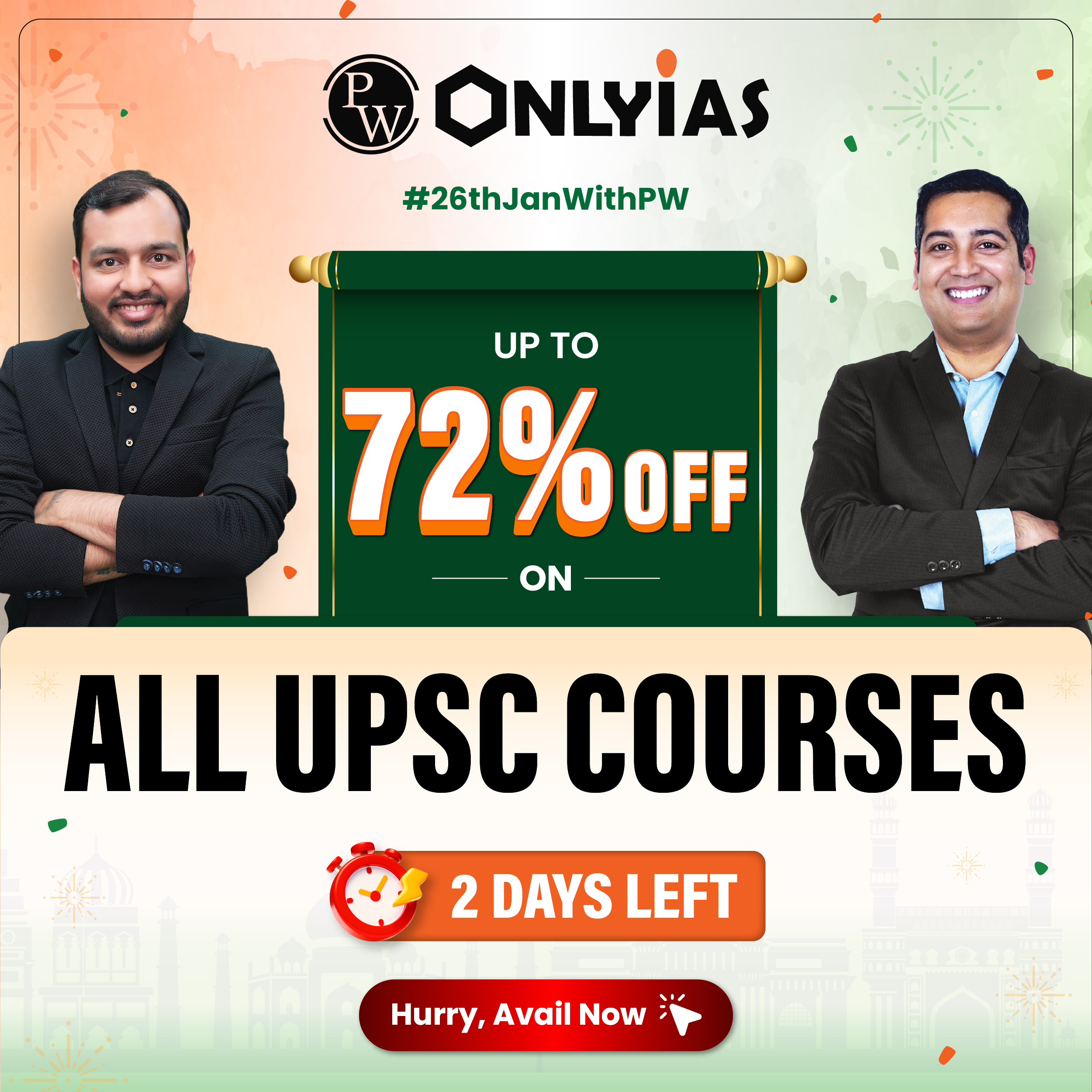
Latest Comments