प्रश्न की मुख्य माँग
- महाराष्ट्र और तेलंगाना में हालिया घटनाओं के आलोक में राज्य विधानसभाओं में दलबदल के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।
- दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए।
- दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) की चुनौतियों का समाधान करने और इसकी दक्षता बढ़ाने के तरीके सुझाइये।
|
उत्तर
दलबदल, जिसे अक्सर “राजनीतिक खरीद-फरोख्त” कहा जाता है, एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा उस पार्टी को छोड़ना है जिसके टिकट पर वे चुने गए थे। इस पर अंकुश लगाने के लिए, 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची डाली गई, जिसमें दलबदल विरोधी कानून (ADL) निर्धारित किया गया। इसके बावजूद, हाल के प्रकरणों, विशेष रूप से महाराष्ट्र (वर्ष 2022) और तेलंगाना (वर्ष 2023) में इसकी प्रभावशीलता के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।
राज्य विधानमंडलों में दलबदल के निहितार्थ
- लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करना: मतदाता राजनीतिक पार्टी की विचारधारा और घोषणापत्र के आधार पर नेताओं का चुनाव करते हैं। दलबदल इस लोकतांत्रिक विकल्प को विकृत करता है।
- उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र में, शिवसेना के विभाजन के कारण मूल चुनावी जनादेश के विपरीत सरकार बनी।
- राजनीतिक अस्थिरता: दलबदल के कारण सरकार में बदलाव और शासन में अस्थिरता हो सकती है। दलबदल के माध्यम से बनी सरकारें आमतौर पर कमजोर और अल्पकालिक होती हैं।
- उदाहरण के लिए: कर्नाटक (वर्ष 2019) और मध्य प्रदेश (वर्ष 2020) में दलबदल के कारण सरकार में परिवर्तन हुए।
- जन विश्वास में कमी: बार-बार दलबदल से राजनीतिक संस्थाओं में जनता का विश्वास खत्म हो सकता है। मतदाता अपने प्रतिनिधियों को स्वार्थी और अवसरवादी समझ सकते हैं, जिससे राजनीतिक प्रक्रिया के संबंध में संदेह उत्पन्न हो सकता है।
- धन और बाहुबल का उदय: विधायकों को पार्टी बदलने के लिए प्रलोभन दिए जाने के आरोप, राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वास को कम करते हैं। संसदीय लोकतंत्र के लिए यह एक गंभीर नैतिक चुनौती है।
- उदाहरण के लिए: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में 543 नवनिर्वाचित सदस्यों में से रिकॉर्ड 251 (46%) सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 27 को दोषी ठहराया जा चुका है।
- आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र का क्षरण: बारंबर विभाजन या बदलाव पार्टियों के भीतर खुली बहस को हतोत्साहित करते हैं और व्यक्ति-आधारित राजनीति को बढ़ावा देते हैं।
- न्यायिक अधिभार: अध्यक्षों द्वारा निर्णय में देरी के कारण प्रायः अदालती मामले लम्बे समय तक चलते हैं, जिससे न्यायपालिका पर बोझ बढ़ जाता है।
दलबदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता (दसवीं अनुसूची)
सकारात्मक योगदान
- अवसरवादी दलबदल को रोकता है: इसने व्यक्तिगत लाभ के लिए दलबदल करने वाले व्यक्तियों को अयोग्य ठहराकर “आया राम, गया राम” की राजनीति को काफी हद तक समाप्त कर दिया है।
- पार्टी अनुशासन को मजबूत करना: यह निर्वाचित प्रतिनिधियों को दलबदल के माध्यम से पार्टी की विचारधारा या नेतृत्व को कमजोर करने से हतोत्साहित करके पार्टी अनुशासन को लागू करता है।
- मतदाता के जनादेश को कायम रखता है: मतदाता अक्सर पार्टी की विचारधारा और घोषणापत्र के आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं, न कि केवल व्यक्ति के आधार पर। यह कानून,चुनावी जनादेश के साथ विश्वासघात को रोकता है।
- अयोग्यता के लिए कानूनी तंत्र प्रदान करता है: स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों को परिभाषित करता है जिनके तहत किसी चुने गये नेता को दलबदल के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है (जैसे, स्वैच्छिक त्यागपत्र, बिना अनुमति के पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करना/मतदान से परहेज करना)।
- प्रतिवारण मूल्य: नैतिक और कानूनी निवारक के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से व्यक्तिगत विधायकों के लिए।
सीमाएँ और खामियाँ
- असहमति को दबाना: विधायकों को व्यक्तिगत या नैतिक विश्वासों के विरुद्ध भी पार्टी व्हिप का पालन करना होगा, जिससे मतदाताओं के प्रति जवाबदेही सीमित हो जाएगी और आंतरिक असहमति का दमन किया जा सकेगा।
- अयोग्यता के फैसलों में देरी: कानून में स्पीकर के लिए कार्रवाई करने की कोई स्पष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र में, अयोग्यता याचिकाएँ एक साल से अधिक समय तक लंबित रहीं, जिससे विद्रोही गुट को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति मिल गई और यहाँ तक कि कुछ दलबदलुओं को मंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई।
- स्वतंत्र प्राधिकरण का अभाव: अध्यक्ष, जो अक्सर सत्तारूढ़ दल से होता है, निर्णायक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। दलबदल के मामले में अंतिम निर्णय लेते समय यह हित संघर्ष को जन्म देता है।
- उदाहरण के लिए: किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू (वर्ष 1992) वाद में सर्वोच्च न्यायलय ने अध्यक्ष के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी, जिससे तत्काल प्रवर्तन कमज़ोर हो गया।
- “विभाजन” और “विलय” प्रावधानों पर अस्पष्टता: दो-तिहाई नियम या इंजीनियर्ड इस्तीफे जैसी खामियाँ विधायकों/सांसदों के समूहों को दलबदल विरोधी प्रावधानों के अंतर्गत आए बिना दलबदल करने की सुविधा प्रदान करती हैं।
- उदाहरण के लिए: “विलय” खंड (2/3 सदस्यों का दूसरी पार्टी में शामिल होना) का अभी भी रणनीतिक रूप से उपयोग किया जा रहा है, जैसा कि तेलंगाना में हुआ।
- न्यायिक अतिक्रमण या विलंबित हस्तक्षेप: न्यायपालिका केवल अध्यक्ष के निर्णय के बाद ही हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे विलंब होता है और कानून की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
- उदाहरण के लिए: वर्ष 2020 में, न्यायालय ने संसद से संविधान में संशोधन करने के लिए कहा था ताकि विधान सभा अध्यक्षों से यह निर्णय लेने की उनकी विशेष शक्ति छीन ली जाए कि दसवीं अनुसूची के तहत विधायकों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं, जो दलबदल विरोधी कानून बनाती है।
- अंतर-पार्टी लोकतंत्र का अभाव: यह कानून पार्टियों को सदस्यों को नियंत्रित करने और अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तथा पार्टी के भीतर असहमति और बहस को हतोत्साहित करता है।
-
- उदाहरण के लिए: जैसा कि NCRWC (2002) द्वारा अनुशंसित किया गया है, पार्टियों के भीतर ऐसे तंत्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो स्वस्थ असहमति, पारदर्शी निर्णय लेने और जवाबदेही की अनुमति देते हैं।
हालिया मामले: महाराष्ट्र और तेलंगाना
- महाराष्ट्र (वर्ष 2022)
- वर्ष 2022 में शिवसेना विधायकों का एक बड़ा गुट अलग होकर भाजपा के साथ गठबंधन कर गया।
- अध्यक्ष ने अयोग्यता याचिकाओं में देरी की।
- सर्वोच्च न्यायालय (2023 निर्णय) ने अध्यक्ष की निष्क्रियता की आलोचना की और समय पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, लेकिन विश्वास मत के लिए राज्यपाल के निर्णय को बरकरार रखा।
- तेलंगाना (वर्ष 2023)
-
- चुनाव से ठीक पहले कई BRS विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए।
- तत्काल कोई अयोग्य नहीं करार दिया गया, जिससे समय पर प्रवर्तन में आने वाली खामियां उजागर होती हैं।
|
आगे की राह
- समयबद्ध अयोग्यता प्रक्रिया: 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने के लिए कानून या संशोधन लागू करना चाहिये।
- उदाहरण के लिए: केशम मेघचंद्र बनाम स्पीकर (वर्ष 2020) वाद में सर्वोच्च न्यायलय ने सिफारिश की कि हालांकि अदालतें अयोग्यता याचिका के नतीजे को तय नहीं कर सकती हैं, लेकिन वे स्पीकर को उचित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दे सकती हैं।
- स्वतंत्र न्यायाधिकरण: अयोग्यता के अधिकार को अध्यक्ष से हटाकर चुनाव आयोग या न्यायिक न्यायाधिकरण जैसे स्वतंत्र निकाय को सौंपना चाहिये।
- उदाहरण के लिए: मेघचंद्र वाद (वर्ष 2020) में, सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण नियुक्त किया जा सकता है जो दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामलों से निपटने के लिए अध्यक्ष का स्थान लेगा।
- दलबदलुओं के लिए कठोर दंड: दलबदलुओं को एक निश्चित अवधि के लिए मंत्री पद पर बने रहने या चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
- दसवीं अनुसूची में सुधार: विलयन खण्ड (Merger Clause) पर पुनः विचार होना चाहिए और सामूहिक दलबदल को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिए।
- राजनीतिक और चुनावी सुधार: पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए और उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता और मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: दलबदल के प्रभाव और राजनीतिक जवाबदेही के महत्त्व के बारे में मतदाताओं को शिक्षित करना चाहिए। अयोग्यता याचिकाओं और परिणामों पर नजर रखने के लिए सूचना के अधिकार (RTI) और नागरिक समाज निगरानीकर्ताओं का उपयोग करना चाहिए।
दलबदल विरोधी कानून राजनीतिक स्थिरता और विधायकों के नैतिक आचरण को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक सुधार था। हाल के दुरुपयोगों को संबोधित करने के लिए, प्रक्रियात्मक, कानूनी और राजनीतिक व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। भारत में लोकतंत्र की भावना और उसके मूल्य दोनों की रक्षा के लिए कानून को विकसित किया जाना चाहिए।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

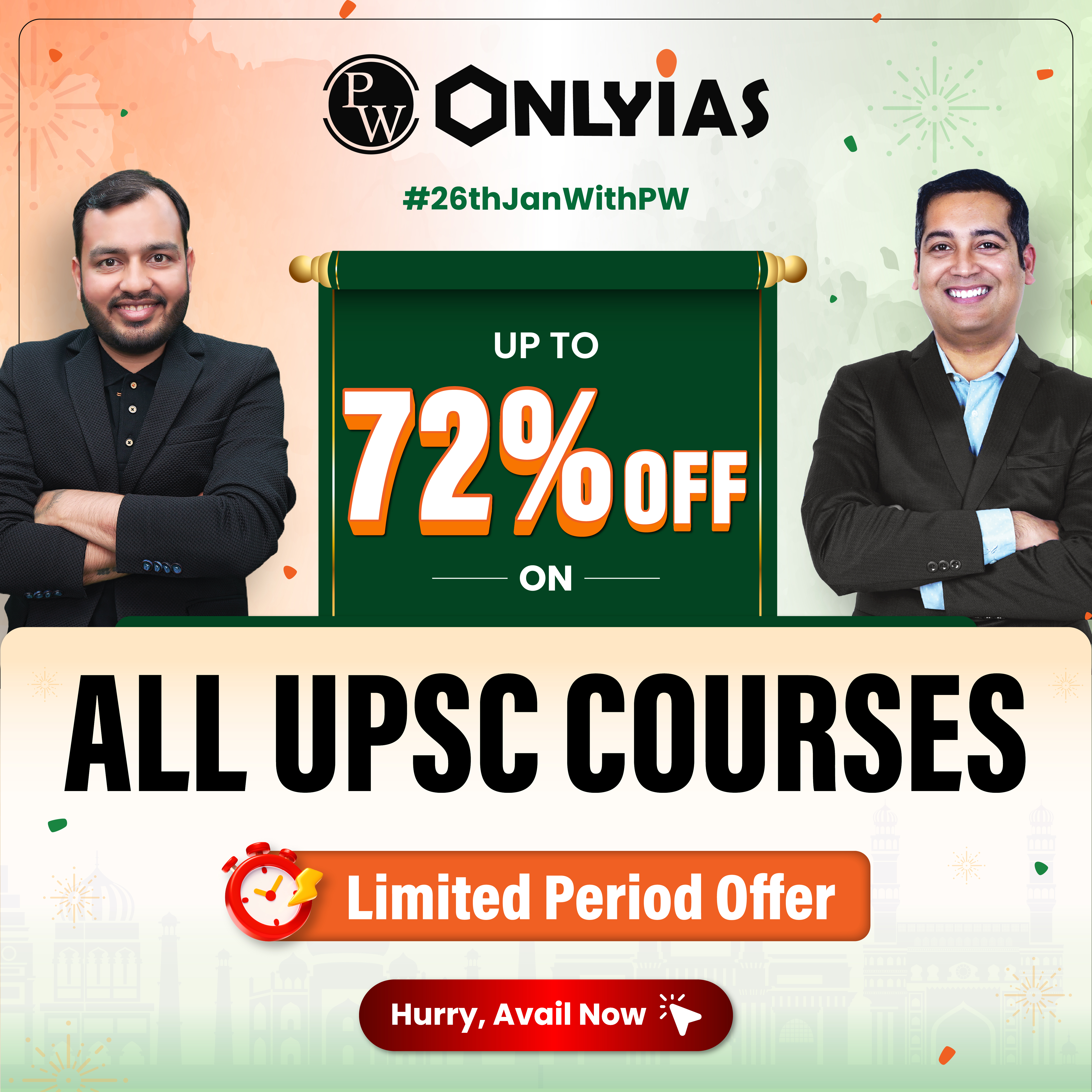
Latest Comments