प्रश्न की मुख्य माँग
- भारत में हिरासत में होने वाली हिंसा के संरचनात्मक कारण।
- विधि के शासन पर हिरासत में होने वाली हिंसा का प्रभाव।
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित व्यापक सुधार।
|
उत्तर
‘डर्टी हैरी’ मॉडल एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसमें पुलिस जबरदस्ती, भय और हिंसा के जरिए आरोपी से स्वीकारोक्ति प्राप्त करती है। जो लोकतांत्रिक पुलिसिंग को कमजोर कर देता है, क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रियाओं के स्थान पर बर्बरता को रखता है। भारत में निरंतर बनी रहने वाली हिरासत में प्रताड़ना संवैधानिक आदर्श और जमीनी हकीकत में विरोधाभास को दर्शाती है; 2018 से 2023 के मध्य 687 हिरासत में मौतें दर्ज हुईं, अर्थात् प्रति सप्ताह औसतन दो से तीन, जो गंभीर संस्थागत संकट और जवाबदेही की विफलता को दर्शाती हैं, भले ही कानूनी सुरक्षा प्रावधान मौजूद हैं।
भारत में हिरासत में होने वाली हिंसा के संरचनात्मक कारण
- वैज्ञानिक जाँच उपकरणों का अभाव: पुराने बुनियादी ढाँचे और सीमित फोरेंसिक संसाधनों के कारण पुलिस, स्वीकारोक्ति (Confessions) पर निर्भर रहती है।
- शीघ्र परिणाम के लिए दबाव: अधिकारी मामलों को शीघ्र हल करने के लिए राजनीतिक और उच्चाधिकारियों के दबाव में कार्य करते हैं।
- अपर्याप्त पुलिस प्रशिक्षण: 90% पुलिस कर्मी कांस्टेबल हैं, जिन्हें कानूनी या मानवाधिकार मानदंडों का न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त है।
- जवाबदेही तंत्र का अभाव: कोई भी स्वतंत्र प्राधिकारी हिरासत में व्यवहार की निगरानी नहीं करता है और वरिष्ठ अधिकारी अक्सर शिकायतों को नजरअंदाज कर देते हैं।
- संरचनात्मक सामाजिक पक्षपात: वंचित समुदायों को प्रणालीगत जाति और वर्ग पूर्वाग्रह के कारण अधिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।
- कमजोर कानूनी निवारक: भारत में कोई स्वतंत्र प्रताड़ना-विरोधी कानून नहीं है, जिससे पुलिस लगभग बेखौफ होकर काम करती है।
उदाहरण के लिए: भारत ने वर्ष 1997 में हस्ताक्षर करने के बावजूद अभी तक यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAT) का अनुमोदन नहीं किया है।
विधि के शासन पर हिरासत में हिंसा का प्रभाव
- संवैधानिक नैतिकता का क्षरण: प्रताड़ना अनुच्छेद-21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) का उल्लंघन करती है और नागरिक स्वतंत्रता को कमजोर करती है।
उदाहरण: के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय (2017) ने शारीरिक स्वायत्तता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।
- न्यायिक विश्वसनीयता को कमजोर करता है: जबरन कराई गई स्वीकारोक्ति मुकदमे की प्रक्रिया को भ्रष्ट करती है और दोषसिद्धि की विश्वसनीयता को भी कम करती है।
उदाहरण: डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए गिरफ्तारी ज्ञापन या अरेस्ट मेमो और परिवार को सूचना देना अनिवार्य कर दिया था।
- दंडमुक्ति की संस्कृति: पुलिस स्वयं को कानून से ऊपर मानने लगती है, जिससे संस्थाओं में जनता का विश्वास कम होता है।
उदाहरण: वर्ष 2001-2020 के बीच हिरासत में हुई 1,888 मौतों में से 893 मामले दर्ज किए गए, 358 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई, फिर भी केवल 26 पुलिसकर्मियों को ही दोषी ठहराया गया, जो दंडमुक्ति को दिखाता है।
- झूठी स्वीकारोक्ति और न्याय में विफलता: प्रताड़ना के परिणामस्वरूप झूठे सुराग बनाए जाते हैं, निर्दोषों को दंडित किया जाता है और वास्तविक अपराधियों को बच निकलने का मौका मिलता है।
- साक्ष्य-आधारित पुलिसिंग को हतोत्साहित करना: शारीरिक बल प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने से फोरेंसिक और विश्लेषणात्मक तरीकों का कम उपयोग किया जाता है।
- अंतरराष्ट्रीय आलोचना का बढ़ता जोखिम: UNCAT का अनुपालन न करने से भारत की वैश्विक मानवाधिकार छवि प्रभावित होती है।
उदाहरण: विश्व प्रताड़ना विरोधी संगठन द्वारा वैश्विक प्रताड़ना सूचकांक, 2025 में भारत को “उच्च जोखिम” वाले देश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
बलपूर्वक पुलिसिंग के स्थान पर भारत को सशक्त जवाबदेही के साथ मानवीय, साक्ष्य-आधारित मॉडल अपनाना होगा।
वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित व्यापक सुधार
- PEACE मॉडल (UK) अपनाना: बिना किसी दबाव के सम्मानजनक रूप से रिकॉर्ड किए गए और संरचित साक्षात्कारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें बल प्रयोग नहीं होता।
उदाहरण: यूरोपीय प्रताड़ना रोकथाम समिति (CPT) ने PEACE मॉडल को मान्यता दी है।
- पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग: यह पुलिस पूछताछ में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
उदाहरण: न्यूजीलैंड में सभी पुलिस पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है; भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है।
- स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण (IPCA): हिरासत में होने वाले उत्पीड़न की निष्पक्ष जाँच के लिए राज्य-स्तरीय IPCA की स्थापना की जानी चाहिए।
उदाहरण: 2006 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रकाश सिंह वाद के निर्णय में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (SPCA) की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
- अनिवार्य फोरेंसिक भागीदारी: दोषसिद्धि के लिए स्वीकारोक्ति के बजाय फोरेंसिक पर निर्भरता को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- मानवाधिकार-आधारित पुलिस प्रशिक्षण: पुलिस को अधिकारों, सामुदायिक सहभागिता और अहिंसक तरीकों में प्रशिक्षित करना चाहिए।
निष्कर्ष
संवैधानिक लोकतंत्र और प्रताड़ना एक साथ नहीं चल सकते। चूँकि भारत वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा रखता है, इसलिए उसकी पुलिस व्यवस्था में न्याय, गरिमा और प्रमाण के सिद्धांत प्रतिबिंबित होने चाहिए, न कि भय और क्रूरता। भविष्य की राह पेशेवरता, पारदर्शिता और वैधानिक पूछताछ में निहित है, न कि हिरासत में होने वाली प्रताड़ना में। जैसा कि संवैधानिक विचारधारा में निहित है, “एक निर्दोष के कष्ट सहने की अपेक्षा दस दोषियों का बच निकलना बेहतर है।”
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

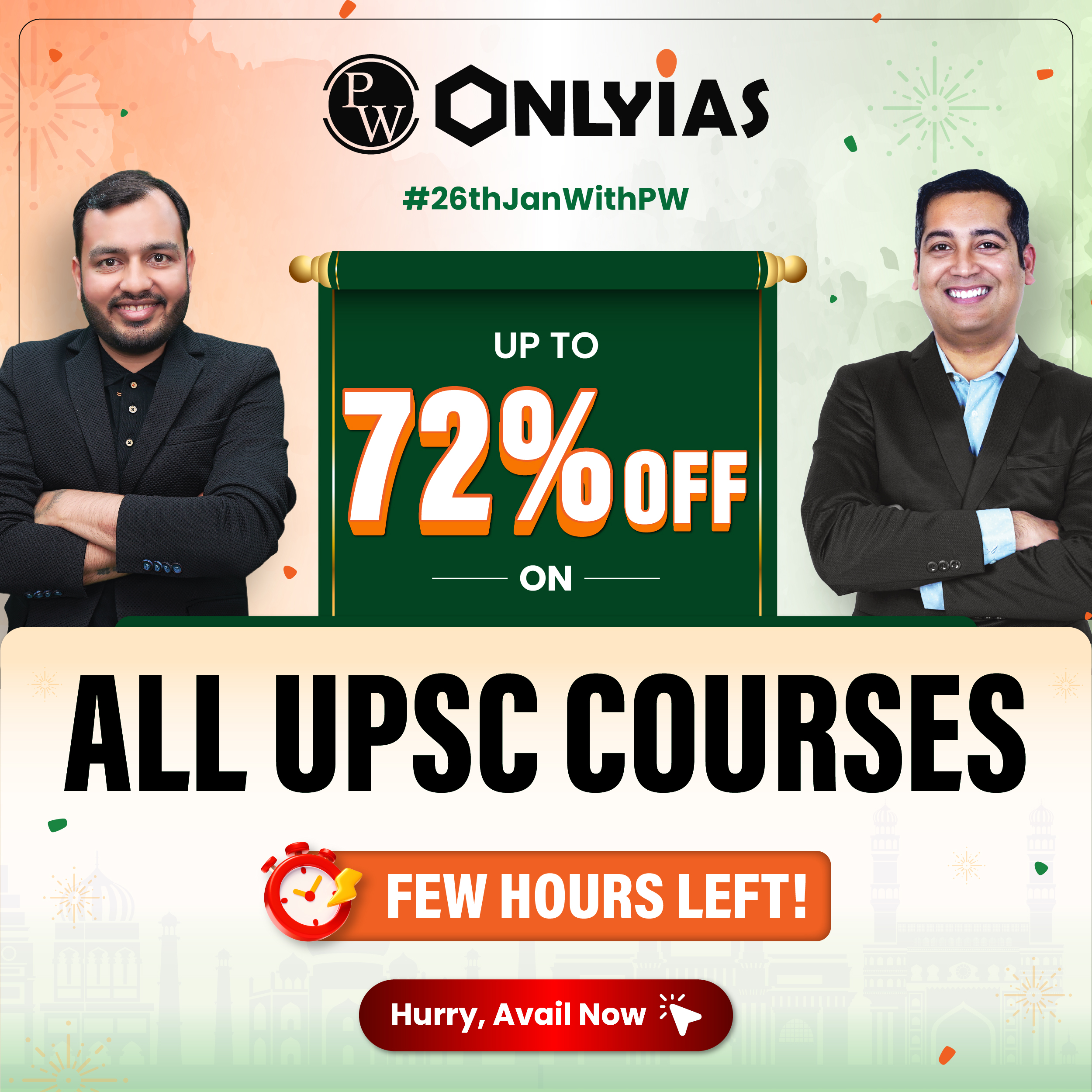
Latest Comments