निबंध लिखने का दृष्टिकोणभूमिका:
मुख्य भाग
निष्कर्ष
|
भारत और पाकिस्तान का मामला इस तथ्य को उद्घाटित करता है कि भूगोल देशों को पड़ोसी तो बना सकता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे मित्र भी हों। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही, दोनों देशों के बीच एक लंबी, विवादित सीमा रही है। हालाँकि, उनके संबंधों में शत्रुता की झलक मिलती है, जिसमें 1947, 1965 और 1971 में हुए तीन प्रत्यक्ष युद्ध, तथा कश्मीर पर चल रहा संघर्ष शामिल है। इसके अतिरिक्त, सीमापार आतंकवाद ने संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे विश्वास कायम करना कठिन हो गया है। भौगोलिक निकटता के बावजूद, इन युद्धों और संघर्षों जैसी ऐतिहासिक घटनाओं ने दोनों पड़ोसियों के बीच वास्तविक मित्रता के विकास को रोक दिया है।
इसके विपरीत, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध एक अलग कहानी बताते हैं। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद दोनों देश न केवल पड़ोसी बन गये बल्कि घनिष्ठ सहयोगी भी बन गये। भूगोल के कारण वे एक-दूसरे के निकट थे, लेकिन बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए उनके साझा ऐतिहासिक संघर्ष और सहयोग ने उनकी मित्रता को मजबूत किया। पिछले कुछ वर्षों में, 2015 के भूमि सीमा समझौते तथा व्यापार, जल बंटवारे और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग जैसे समझौतों ने इन संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है। दोनों देशों ने अपनी भौगोलिक निकटता का उपयोग स्थायी सहयोग और परस्पर सम्मान को प्रोत्साहन देने के लिए किया है।
ये दो उदाहरण दर्शाते हैं कि यद्यपि भूगोल देशों को एक-दूसरे के निकट लाता है, लेकिन वास्तव में इतिहास ही संबंधों को आकार देता है। भारत और पाकिस्तान के मामले में इतिहास ने विभाजन को जन्म दिया है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के मामले में इतिहास ने घनिष्ठ मित्रता का निर्माण किया है। यह निबंध के विषय को अच्छे ढंग से प्रतिबिंबित करता है: भूगोल ने हमें पड़ोसी बनाया है। इतिहास ने हमें मित्र बनाया है। यह निबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में भूगोल और इतिहास के महत्व को उद्घाटित करता है, तथा यह दर्शाता है कि भौगोलिक निकटता किस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करती है, जबकि साझा ऐतिहासिक अनुभव गहरी मित्रता का निर्माण करते हैं। यह एक समग्र दृष्टिकोण पर बल देता है, जो विद्यमान चुनौतियों के बावजूद स्थायी सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भूगोल और इतिहास दोनों का लाभ उठाता है। उद्धरण “भूगोल ने हमें पड़ोसी बनाया है। इतिहास ने हमें मित्र बनाया है।” इस बात पर बल दिया गया है कि जहां भूगोल राष्ट्रों को भौतिक रूप से निकट लाता है, वहीं यह इतिहास ही है जो साझा अनुभवों, संघर्षों और गठबंधनों के माध्यम से भावनात्मक संबंधों का निर्माण करता है।
भौगोलिक निकटता पड़ोसी देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीमा साझा करने वाले देश प्रायः व्यापार मार्गों, प्रवासन पैटर्न और सुरक्षा हितों के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत और नेपाल ने अपनी भौगोलिक निकटता के कारण खुली सीमा नीतियां विकसित की हैं, जो लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही की अनुमति देती हैं। इस निकटता के कारण दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध भी मजबूत हुए हैं, दोनों देश समान त्योहार, भाषाएं और परंपराएं साझा करते हैं, जिससे अलग-अलग संप्रभु इकाई होने के बावजूद सामुदायिक भावना को प्रोत्साहन मिलता है।
इसी प्रकार, यूरोपीय संघ (ईयू) यह दर्शाता है कि भूगोल किस प्रकार एक संयोजक के रूप में कार्य कर सकता है। यूरोपीय देशों की निकटता के कारण आर्थिक साझेदारियां विकसित हुईं और शेंगेन क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिससे सीमाओं के पार मुक्त आवागमन संभव हो पाया । इस भौगोलिक निकटता ने क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास को संभव बनाया है, तथा ऊर्जा, परिवहन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि हुई है है। इस प्रकार, भूगोल संबंधों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, जिससे सहयोग सुगम और आवश्यक हो जाता है।
जबकि भूगोल संबंधों के लिए अवसर प्रदान करता है, यह साझा ऐतिहासिक अनुभव ही हैं जो वास्तव में मित्रता को सुदृढ़ बनाते हैं। जिन राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर युद्ध लड़े हैं, औपनिवेशिक संघर्षों का सामना किया है, या रणनीतिक गठबंधन बनाए हैं, उनमें दीर्घकालिक विश्वास और सौहार्द विकसित होता है। उदाहरण के लिए, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए उनके साझा संघर्ष पर आधारित हैं, जहां भारत ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ाई में बांग्लादेश का समर्थन किया था। इस ऐतिहासिक अनुभव ने दोनों देशों के बीच परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त किया है।
एक अन्य उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच मैत्री है, जो विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साझा ऐतिहासिक अनुभवों से आकार लेती है। दोनों देशों ने सहयोगी के रूप में लड़ाई लड़ी, और तत्कालीन अवधि के दौरान उनके सहयोग ने आज के विद्यमान विशेष संबंधों की नींव रखी, जो मजबूत कूटनीतिक, रक्षा और आर्थिक संबंधों की विशेषता है। ये ऐतिहासिक बंधन अक्सर केवल राजनीतिक गठबंधनों से आगे निकल जाते हैं और स्थायी साझेदारी का आधार बनते हैं।
समय के साथ, साझा सीमाओं या ऐतिहासिक अनुभवों वाले राष्ट्र प्रायः कूटनीतिक समझौतों और व्यापार साझेदारी के माध्यम से अपने संबंधों को औपचारिक बनाने का प्रयास करते हैं। शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए कूटनीति आवश्यक है, जबकि व्यापार राष्ट्रों को उनकी निकटता से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। भूटान के साथ भारत के संबंध इस बात का प्रमाण हैं कि किस प्रकार कूटनीतिक प्रयास और व्यापार समझौते स्थायी संबंधों का निर्माण कर सकते हैं। 1949 की भारत-भूटान मैत्री संधि ने एक मजबूत कूटनीतिक संबंधों की नींव रखी और आज, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। दोनों देश जलविद्युत परियोजनाओं पर मिलकर कार्य कर रहे हैं, भूटान भारत को विद्युत निर्यात कर रहा है, जिससे दोनों देशों को लाभ हो रहा है।
वैश्विक संदर्भ में, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA), जिसे अब USMCA द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि किस प्रकार कूटनीति और व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच मित्रवत संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। इन व्यापार समझौतों ने सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह की अनुमति दी, जिसने परस्पर आर्थिक निर्भरता को जन्म दिया है, शांतिपूर्ण संबंधों और पारस्परिक विकास को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, ऐतिहासिक तनाव वाले देश भी कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग के माध्यम से मतभेदों को दूर कर सकते हैं, तथा अपनी निकटता को लाभकारी साझेदारी में बदल सकते हैं।
संपूर्ण इतिहास में, अनेक पड़ोसी देशों ने संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता का अनुभव किया है, लेकिन कुछ देशों ने इन्हें सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों में बदल दिया है। इसका एक प्रमुख उदाहरण फ्रांस और जर्मनी के बीच संबंध है। विनाशकारी विश्व युद्धों सहित सदियों के संघर्ष के बाद, दोनों देश कट्टर शत्रुओं से साझेदार बनने में सफल हुए। 1951 में यूरोपीय कोयला एवं इस्पात संगठन (ECSC) की स्थापना, जो यूरोपीय संघ का अग्रदूत था, ने सुलह को प्रोत्साहन दिया । अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करके, विशेष रूप से युद्ध के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों में, फ्रांस और जर्मनी ने शांति और सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार किया जो आधुनिक युग में भी जारी है।
भारतीय संदर्भ में, भारत और चीन ने अपने सीमा विवादों और 1962 के युद्ध के बावजूद सहयोग के क्षण दर्शाए हैं। यद्यपि सीमा विवादों को लेकर तनाव बना हुआ है, फिर भी दोनों देश आर्थिक साझेदारियों में शामिल हैं तथा ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय संगठनों में भाग ले रहे हैं। ये मंच संवाद और आर्थिक सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं, तथा यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार ऐतिहासिक रूप से प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र भी सहयोग हेतु समान आधार प्राप्त कर सकते हैं और पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं। यद्यपि चुनौतियां विद्यमान रहती हैं, किंतु ऐसे संबंध समय के साथ संघर्ष को सहयोग में बदलने की क्षमता का उदाहरण हैं।
साझा सांस्कृतिक विरासत प्रायः पड़ोसी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने और कायम रखने में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत और श्रीलंका के बीच संबंध है। दोनों राष्ट्र गहरे बौद्ध संबंध साझा करते हैं, श्रीलंका थेरवाद बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है और भारत बौद्ध धर्म का जन्मस्थान है। रामायण महाकाव्य के माध्यम से प्राचीन संबंध तथा भारत में बोधगया और श्रीलंका में श्री पद जैसे पवित्र स्थलों की निरंतर धार्मिक तीर्थयात्राएं सांस्कृतिक सेतु को मजबूत करने में मदद करती हैं। ये साझा धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास दोनों देशों के बीच सशक्त कूटनीतिक और सामाजिक संबंधों में योगदान देते हैं।
इसी प्रकार, मलेशिया और इंडोनेशिया एक सामान्य मलय सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं जो दोनों देशों के बीच एक सेतु का कार्य करती है। दोनों देशों ने भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास साझा किया है जो उन्हें कभी-कभी उत्पन्न होने वाली कूटनीतिक चुनौतियों के बावजूद एक साथ बांधे रखता है। दोनों देशों में मलय भाषा व्यापक रूप से बोली जाती है तथा इस्लाम प्रमुख धर्म है। ये साझा सांस्कृतिक तत्व परस्पर सम्मान और समझ को बढ़ावा देते हैं, जिससे तनावों को सुलझाना आसान हो जाता है तथा पर्यटन, शिक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है।
आधुनिक विश्व में, वैश्वीकरण और कूटनीति देशों को निकट लाने में महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिससे प्रायः भौगोलिक सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। वैश्विक व्यापार नेटवर्क, बहुराष्ट्रीय निगमों और डिजिटल संचार प्लेटफार्मों ने राष्ट्रों को अभूतपूर्व ढंग से जोड़ दिया है। उदाहरण के लिए, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश ऐतिहासिक संघर्षों के बावजूद वैश्वीकरण के माध्यम से आर्थिक रूप से निकट आ गए हैं। दोनों देश वैश्विक प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल उद्योगों में प्रमुख अभिकर्ता हैं, जो विश्व व्यापार संगठन (WTO) और APEC जैसे क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से सहयोग करते हैं। उनकी कूटनीतिक संलग्नता ने उन्हें शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने में मदद की है, साथ ही उनकी निकटता और वैश्विक एकीकरण से आर्थिक लाभ भी मिला है।
भारतीय संदर्भ में, वैश्वीकरण के युग में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंध उल्लेखनीय रूप से विकसित हुए हैं। भौगोलिक दृष्टि से दूर होने के बावजूद, आधुनिक कूटनीति और आर्थिक सहयोग ने दोनों देशों को निकट ला दिया है। भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते और रक्षा तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में साझेदारी जैसे समझौतों ने संबंधों को मजबूत किया है। अमेरिका में लाखों भारतीय प्रवासियों के साथ प्रवासी कूटनीति के उदय ने भी दोनों देशों के बीच मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहन दिया है। इस प्रकार, वैश्वीकरण ने देशों को अतीत के संघर्षों से उबरने में सक्षम बनाया है, तथा ऐसी मित्रताएं निर्मित की हैं जो पारंपरिक भौगोलिक सीमाओं से परे हैं।
साझा भूगोल और इतिहास के बावजूद, पड़ोसी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चुनौतियों से रहित नहीं है। सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक सीमा विवाद है। उदाहरण के लिए, लद्दाख क्षेत्र में भारत-चीन सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद प्रायः तनाव उत्पन्न होता रहा है। क्षेत्रीय दावों पर ऐतिहासिक असहमतियों के कारण झड़पें हुई हैं, जैसे कि 2020 में गलवान घाटी की घटना, जिसने इस तथ्य को उद्घाटित किया कि किस प्रकार अनसुलझे सीमा मुद्दे संघर्ष में बदल सकते हैं, यहां तक कि लंबे समय से आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान वाले देशों के बीच भी।
एक अन्य चुनौती राष्ट्रों के बीच वैचारिक मतभेद है। यहां तक कि जब देश एक ही भौगोलिक सीमा और ऐतिहासिक अनुभव साझा करते हैं, तब भी उनके आंतरिक राजनीतिक या वैचारिक परिदृश्य भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध उनकी भिन्न विचारधाराओं के कारण तनावपूर्ण रहे हैं, विशेषकर कश्मीर मुद्दे को लेकर। विभाजन-पूर्व युग से साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों के बावजूद, धर्म, शासन और राष्ट्रीय पहचान पर आधारित वैचारिक संघर्ष दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में बाधा बने हुए हैं।
आर्थिक असमानताएँ भी तनाव का एक स्रोत हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने के बावजूद, ग्रीस और जर्मनी जैसे देशों को यूरोजोन ऋण संकट के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ा। यद्यपि दोनों देशों को यूरोपीय संघ के भीतर आर्थिक सहयोग से लाभ मिला, लेकिन उनकी आर्थिक संरचनाओं और राजकोषीय नीतियों में भारी अंतर के कारण असंतोष और तनाव उत्पन्न हुआ, विशेषकर तब जब ग्रीस पर मितव्ययिता के उपाय लागू किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार आर्थिक असंतुलन, यहां तक कि घनिष्ठ क्षेत्रों के भीतर भी, मैत्रीपूर्ण संबंधों को बाधित कर सकता है।
अंततः, राष्ट्रवाद और घरेलू राजनीति प्रायः सीमापार मैत्री को जटिल बना देती है। नेता घरेलू समर्थन हासिल करने के लिए राष्ट्रवादी बयानबाजी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, भौगोलिक निकटता और मजबूत व्यापारिक संबंधों के बावजूद, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच तनाव कभी-कभी बढ़ जाता है, क्योंकि कोरिया पर जापान के औपनिवेशिक शासन और युद्धकालीन अत्याचार जैसे मुद्दों पर ऐतिहासिक शिकायतें बनी हुई हैं। ये आंतरिक दबाव कूटनीतिक बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे सकारात्मक संबंधों को कायम रखना कठिन हो सकता है।
इन चुनौतियों पर नियंत्रण प्राप्त करने और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, देशों को आर्थिक सहयोग में निवेश करना चाहिए जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो। भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जैसी साझा बुनियादी ढांचा परियोजनाएं दर्शाती हैं कि पड़ोसी किस प्रकार अपनी भौगोलिक निकटता को आर्थिक लाभ में बदल सकते हैं। यह परियोजना, जो दोनों देशों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है, द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देती है और परस्पर निर्भरता को मजबूत करती है, जिससे संघर्ष की संभावना कम होती है। इस तरह की पहल यह दर्शाती है कि भौगोलिक निकटता का उपयोग किस प्रकार पारस्परिक लाभ के लिए किया जा सकता है तथा देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जा सकता है।
संबंधों को मजबूत बनाने में सांस्कृतिक आदान-प्रदान एक और प्रभावी साधन है। उदाहरण के लिए, भारत-जापान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम ने परस्पर सम्मान और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, कला और खेल में आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देकर, राष्ट्र अपने राजनीतिक मतभेदों से आगे बढ़ सकते हैं और लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्माण कर सकते हैं। ये सांस्कृतिक पहल अधिक सतत संबंधों के लिए आधार तैयार करने में मदद करती हैं, क्योंकि सांस्कृतिक प्रशंसा नागरिकों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देती है, जो कूटनीतिक प्रयासों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
साझा भूगोल से उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए संघर्ष समाधान तंत्र आवश्यक है। आसियान और यूरोपीय संघ जैसे बहुपक्षीय मंच इस बात के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि पड़ोसी देश किस प्रकार बातचीत और वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से संघर्षों का समाधान कर सकते हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद से निपटने में आसियान के दृष्टिकोण ने टकराव की बजाय कूटनीति पर बल दिया है, तथा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दावों के बावजूद तनाव को बढ़ने से रोका है। इसी तरह, तीस्ता नदी से संबंधित जल-बंटवारे के मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही बातचीत से पता चलता है कि निरंतर संचार किस प्रकार सौहार्दपूर्ण संबंधों को बिगड़ने से उतरने से रोक सकता है।
अंततः, देशों को सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय संगठनों और बहुपक्षीय कूटनीति में निवेश करना चाहिए। अफ्रीकी संघ (AU) या यूरोपीय संघ (EU) जैसे व्यापार और सुरक्षा गठबंधनों का गठन, ऐतिहासिक और भौगोलिक चुनौतियों पर नियंत्रण प्राप्त करने में क्षेत्रीय एकता की शक्ति को प्रदर्शित करता है। दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) को यद्यपि बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी इसमें अपने सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की क्षमता है। सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और व्यापार जैसे मुद्दों पर सहयोग को प्रोत्साहित करने वाले ढांचे का निर्माण करके, देश दीर्घकालिक स्थिरता और शांति प्राप्त करने के लिए अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक नींव पर निर्माण कर सकते हैं।
भूगोल अनिवार्य रूप से राष्ट्रों को निकट लाता है, तथा साझा सीमाओं के माध्यम से परस्पर संपर्क के अवसरों को जन्म देता है। हालाँकि, यह इतिहास ही है जो गहन संबंध बनाता है, तथा संघर्ष, सहयोग और गठबंधन जैसे साझा अनुभवों के माध्यम से संबंधों को आकार देता है। भूगोल उन्हें पड़ोसी बना सकता है, लेकिन यह उनका साझा इतिहास ही है जो इन संबंधों को विश्वास और सहयोग पर आधारित स्थायी साझेदारी में बदलता है।
सीमा विवाद, वैचारिक मतभेद और आर्थिक असंतुलन से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, शांतिपूर्ण सहयोग की प्रबल संभावना बनी हुई है। आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से राष्ट्र संघर्षों को सुलझा सकते हैं और परस्पर निर्भरता प्रोत्साहित कर सकते हैं जो स्थिरता को बढ़ावा देती है। यूरोपीय संघ या आसियान जैसे बहुपक्षीय मंच यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार देश मतभेदों को दूर करने और संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं।
पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, “आप अपने मित्र बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी नहीं।” यह आशावादी दृष्टिकोण इस स्थायी सत्य को उद्घाटित करता है कि ऐतिहासिक तनावों के बावजूद, राष्ट्रों को अपनी भौगोलिक वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। एक साथ मिलकर कार्य करके और साझा इतिहास का लाभ उठाकर, पड़ोसी शांतिपूर्ण सहयोग के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, तथा निकटता को संघर्ष के स्रोत के बजाय शक्ति में बदल सकते हैं।
भूगोल हमें साथ-साथ लाता है,
लेकिन इतिहास हमारी प्रगति को आकार देता है।
हमने जो युद्ध लड़े हैं और जिस शांति की तलाश हमने की है,
साझा संघर्षों से मित्रता विकसित होती है।
सांस्कृतिक संबंधों और कूटनीतिक देखभाल के साथ,
पड़ोसी विकसित होना और साझा करना सीख सकते हैं।
जैसा कि वाजपेयीजी ने कहा था, “आप पड़ोसियों को नहीं बदल सकते,”
हम एक साथ बढ़ते हैं, जैसे-जैसे अतीत की शिकायतें मिटती जाती हैं।
संबंधित उद्धरण:
|
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

<div class="new-fform">
</div>
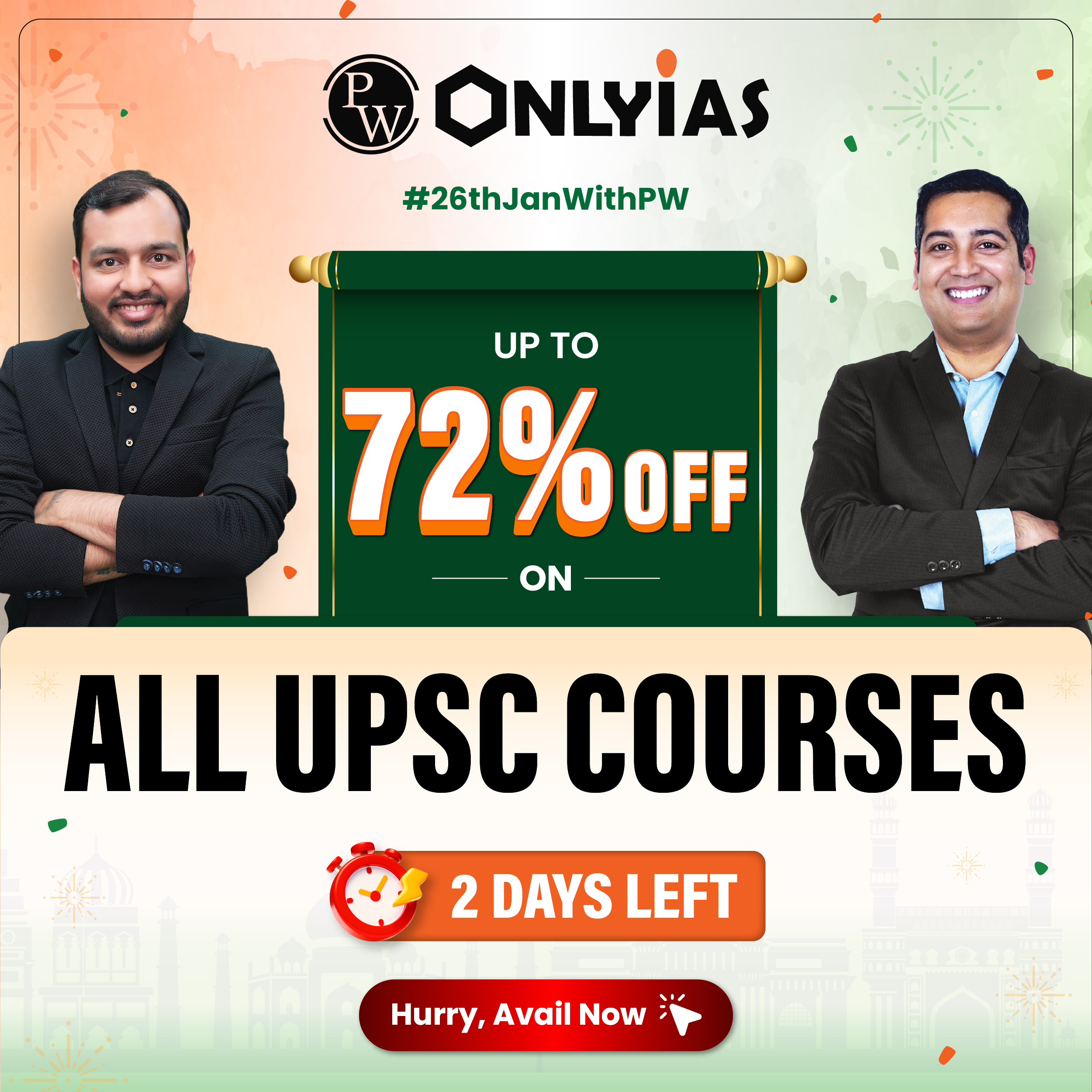
Latest Comments