प्रश्न की मुख्य माँग
- भारत में मानव पूँजी विकास के स्तंभों के रूप में शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकार का उल्लेख कीजिए।
- भारत में प्रजनन स्वास्थ्य पर सूचित विकल्पों और नियंत्रण में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
- एक बहुआयामी रणनीति का सुझाव दीजिए, जिसे भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए अपना सकता है।
|
उत्तर
37.1 करोड़ युवाओं (15-29 वर्ष) के साथ, भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। हालाँकि यह जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन युवाओं, विशेषकर महिलाओं में शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकारों का अभाव इस संभावना को कमजोर करता है। उनकी पूर्ण सामाजिक और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सटीक जानकारी, गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा विकल्प की स्वतंत्रता तक पहुँच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।
भारत में मानव पूँजी विकास के स्तंभ के रूप में शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकार
- सूचित परिवार नियोजन और आर्थिक स्थिरता को सक्षम बनाता है: जब व्यक्ति यह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें कब और कितने बच्चे पैदा करने हैं, तो वे अपने कॅरियर की बेहतर योजना बना पाते हैं, निर्भरता अनुपात कम कर पाते हैं और अर्थव्यवस्था में उत्पादक योगदान दे पाते हैं।
- उदाहरण के लिए: UNFPA 2025 में पाया गया कि 36% भारतीय वयस्क अनचाहे गर्भधारण का सामना करते हैं, जिससे शिक्षा और नौकरी की संभावनाओं पर असर पड़ता है।
- प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य जोखिमों को कम करता है: स्वायत्तता समय से पहले गर्भधारण और कम अंतराल पर जन्म से बचने में मदद करती है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है।
- उदाहरण के लिए: NFHS-5 के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर किशोरावस्था में प्रसव दर 7% है, जबकि कुछ राज्यों में यह दर अधिक होने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- लैंगिक समानता को मजबूत करता है: शारीरिक स्वायत्तता निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जिससे महिलाओं को समाज में समान रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है।
- उदाहरण: लक्ष्य-संचालित प्रजननवाद अक्सर पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को मजबूत करता है; स्वायत्तता नियंत्रण के बजाय सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है।
- शैक्षिक उपलब्धि और सामाजिक गतिशीलता में सुधार: जो लड़कियाँ समय से पूर्व गर्भधारण से बच सकती हैं, उनके उच्च शिक्षा पूरी करने और उच्च आय के अवसरों में आगे बढ़ने की संभावना अधिक होती है।
- उदाहरण के लिए: UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक वर्ष से बाल विवाह की संभावना 6% कम हो जाती है।
- समावेशी और समतामूलक विकास को बढ़ावा: स्वायत्तता यह सुनिश्चित करती है कि हाशिए पर स्थित लोगों सहित सभी समूह बिना किसी दबाव या भेदभाव के प्रजनन अधिकारों का प्रयोग कर सकें।
- उदाहरण के लिए: ICDP, 1994 के एजेंडे ने इस बात की पुष्टि की कि प्रजनन अधिकार गरिमा, विकल्प और सामाजिक समता बनाए रखने के लिए मौलिक हैं।
भारत में सूचित विकल्पों और प्रजनन स्वायत्तता में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ
- प्रजनन स्वायत्तता का अभाव और अधूरी आकांक्षाएँ: कई भारतीय बाँझपन, बच्चों की देखभाल को लेकर चुनौतियाँ और सामाजिक दबाव जैसी बाधाओं के कारण बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं।
- उदाहरण के लिए: UNFPA 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, 36% भारतीय महिलाओं को अनचाहे गर्भधारण का सामना करना पड़ा और 30% के प्रजनन लक्ष्य अधूरे रह गए।
- बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था का उच्च प्रचलन: कम आयु में विवाह लड़कियों की शिक्षा और प्रजनन क्षमता को सीमित करता है।
- उदाहरण: NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह का प्रचलन 23.3% और किशोर गर्भावस्था का प्रचलन 7% है, जबकि कुछ राज्यों में यह दर और भी अधिक है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सूचना तक सीमित पहुँच: युवाओं में व्यापक यौन शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में जागरूकता कम है।
- उदाहरण के लिए: विश्व जनसंख्या दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2025 के विषय में युवाओं की सटीक जानकारी और सेवाओं तक पहुँच पर जोर दिया गया है।
- लैंगिक मानदंड और सामाजिक कलंक: पितृसत्तात्मक मानदंड महिलाओं पर जल्दी माँ बनने का दबाव डालते हैं और उन्हें बच्चों के समय और संख्या पर स्वायत्तता से वंचित करते हैं।
- उदाहरण: जन्म-समर्थक उपाय अक्सर व्यक्तिगत पसंद को सशक्त बनाने के बजाय पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को और मजबूत करते हैं।
- आर्थिक और आवास संबंधी बाधाएँ: वित्तीय अस्थिरता, बेरोजगारी और अपर्याप्त आवास, दंपतियों को अपनी प्रजनन संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने से रोकते हैं।
- उदाहरण: 38% भारतीय उत्तरदाताओं ने वित्तीय सीमाओं और 22% ने आवास की कमी को प्रमुख बाधाएँ बताया (UNFPA 2025)।
- क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच विभिन्न क्षेत्रों में असमान है और ग्रामीण तथा हाशिए पर रहने वाले समूह असमान रूप से प्रभावित हैं।
- उदाहरण: जिन राज्यों में बाल विवाह की दर अधिक है, वहाँ प्रजनन संबंधी चुनौतियाँ अधिक हैं, जो भौगोलिक असमानताओं को दर्शाती हैं।
- श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी: रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव, महिलाओं के प्रजनन संबंधी विकल्पों पर सोच-विचार करने की क्षमता को सीमित करता है।
- उदाहरण के लिए, प्रोजेक्ट मंजिल ने 28,000 से अधिक महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर प्रजनन संबंधी निर्णय लेने में सक्षम बनाया।
भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी रणनीति
- बालिकाओं की शिक्षा और जीवन कौशल में निवेश करना: स्कूली शिक्षा का प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष बाल विवाह के जोखिम को कम करता है और प्रजनन परिणामों में सुधार करता है।
- उदाहरण के लिए, प्रोजेक्ट उड़ान ने माध्यमिक शिक्षा और सामाजिक स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से बालिकाओं की सहायता करके बाल विवाह को रोका।
- गर्भनिरोधकों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार: परिवार नियोजन, बाँझपन देखभाल, सुरक्षित गर्भपात और मातृ स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुँच का विस्तार करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: UNFPA की वर्ष 2025 की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रजनन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गर्भनिरोधकों तक पहुँच महत्त्वपूर्ण है।
- युवा-केंद्रित कार्यक्रमों का विस्तार करना: किशोरों को ज्ञान, नेतृत्व कौशल और निर्णय लेने के साधनों से सशक्त बनाना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, अद्विका (ओडिशा सरकार की एक पहल) ने किशोर सशक्तीकरण और शिक्षा के माध्यम से ओडिशा के 11,000 गाँवों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने में मदद की।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना: अनुकूलित कौशल और कार्यस्थल समावेशन के माध्यम से महिला कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, प्रोजेक्ट मंजिल ने 16,000 युवा महिलाओं को रोजगार हासिल करने, उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ाने और विवाह में देरी करने में मदद की।
- व्यवहार परिवर्तन संचार को मजबूत करना: सामुदायिक लामबंदी और जन जागरूकता के माध्यम से पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंडों को संबोधित करना चाहिए।
- संरचनात्मक सहायता प्रणालियाँ सुनिश्चित करना: बच्चों की देखभाल, आवास, लचीले कार्यस्थल और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल जैसे मूल मुद्दों का समाधान करना चाहिए।
- डेटा-आधारित लक्ष्यीकरण और जवाबदेही का उपयोग करना: हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करने के लिए अलग-अलग डेटा के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं और सुभेद्य समूहों पर नजर रखनी चाहिए।
- उदाहरण के लिए: NFHS-5 डेटा किशोर गर्भधारण और बाल विवाह के प्रमुख केंद्रों का मानचित्रण करने में सहायक रहा है।
निष्कर्ष
भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश अपने युवाओं—विशेषकर युवतियों—को सूचित प्रजनन विकल्पों, शिक्षा और अवसरों से सशक्त बनाने में निहित है। उड़ान, अद्विका और मंजिल जैसे एकीकृत कार्यक्रमों तथा स्वायत्तता पर केंद्रित अधिकार आधारित नीतियों के माध्यम से, भारत अपनी जनसांख्यिकीय क्षमता को सतत् विकास और समावेशी वृद्धि में परिवर्तित कर सकता है।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

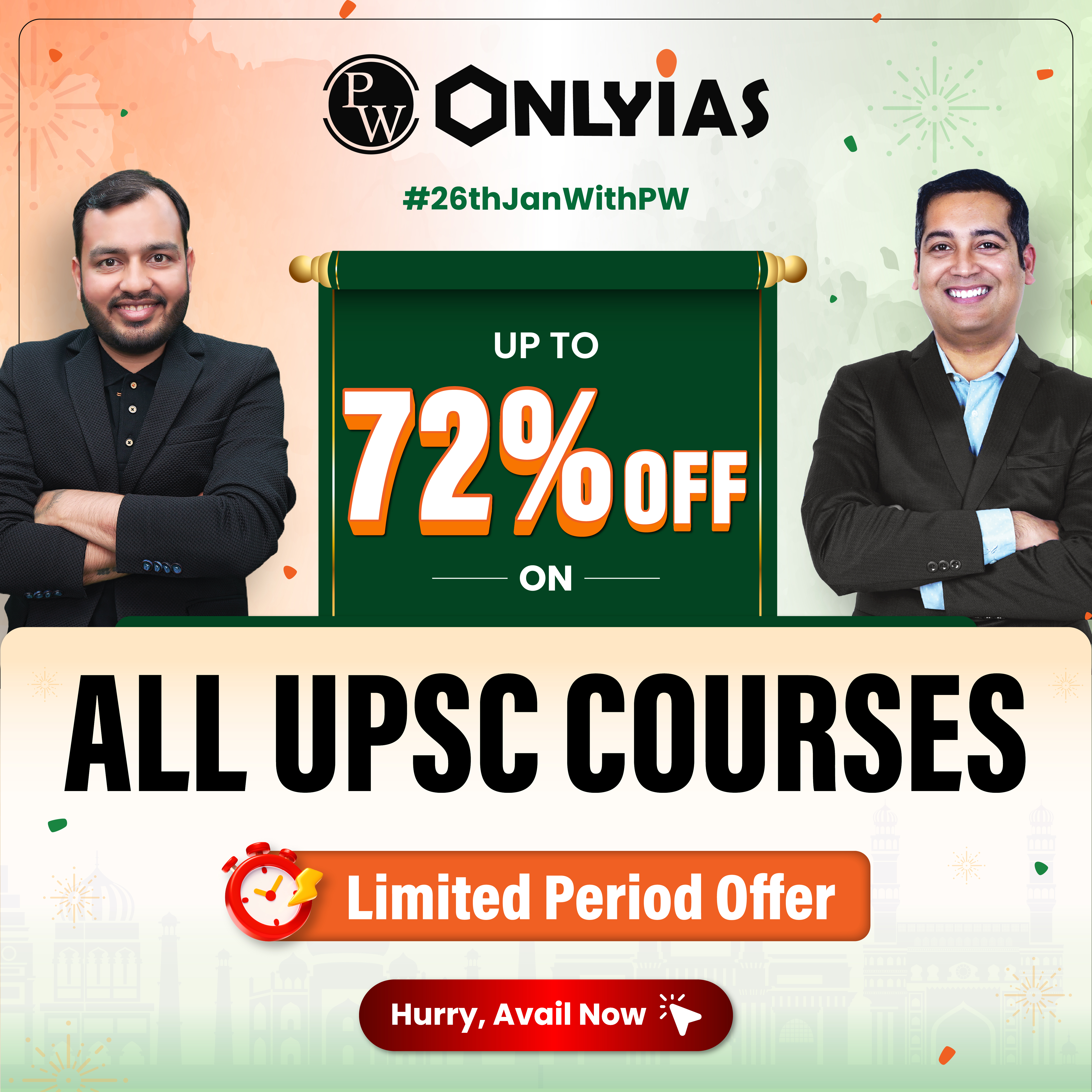
Latest Comments