प्रश्न की मुख्य माँग
- चर्चा कीजिए कि भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या किस प्रकार स्वास्थ्य सेवा वितरण में अंतराल को दर्शाती है।
- परीक्षण कीजिए कि भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या किस प्रकार गहन सामाजिक-आर्थिक और व्यवहारिक असमानताओं को दर्शाती है।
- भारत में टीकों की पहुँच बढ़ाने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह लिखिये।
|
उत्तर
जीरो-डोज वाले बच्चे, जिन्हें अपना पहला DTP (डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस) टीका नहीं मिला है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में एक महत्त्वपूर्ण अंतर को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में प्रगति होने के बावजूद, भारत में 2023 में ऐसे 1.44 मिलियन बच्चे थे जो विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक हैं। भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण लक्ष्यों के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
शून्य खुराक वाले बच्चों की निरंतरता और स्वास्थ्य सेवा वितरण अंतराल
- अपर्याप्त पहुँच: दूरदराज के इलाकों में खराब बुनियादी ढाँचे के कारण वैक्सीन वितरण में बाधा आती है, जिससे सुभेद्य आबादी को टीकाकरण से वंचित रहना पड़ता है।
- उदाहरण के लिए, NFHS-5 के अनुसार, नागालैंड जैसे राज्यों के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में तमिलनाडु ( 89.8% ) जैसे शहरी राज्यों की तुलना में पूर्ण टीकाकरण कवरेज ( 57.8%) काफी कम है।
- महामारी से प्रेरित व्यवधान: COVID -19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान और संसाधनों को दूसरी ओर मोड़ दिया, जिससे वर्षों की प्रगति उलट गई।
- उदाहरण के लिए, महामारी से संबंधित लॉकडाउन और सार्वजनिक भय के कारण भारत में शून्य खुराक की संख्या 2019 में 1.4 मिलियन से बढ़कर 2021 में 2.7 मिलियन हो गई।
गहन सामाजिक-आर्थिक और व्यवहारिक असमानताएँ
सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ
- गरीबी और जागरूकता: गरीबी एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करती है, कम आय वाले परिवारों को अवसर लागत का सामना करना पड़ता है और जागरूकता की कमी होती है।
- मातृ शिक्षा: मातृ शिक्षा का निम्न स्तर कम टीकाकरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माताओं की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक सीमित पहुँच हो सकती है।
उदाहरण के लिए, NFHS-5 के अनुसार, जिन माताओं की स्कूली शिक्षा नहीं हुई है, उनमें से 6.2% बच्चे जीरो डोज वाले हैं, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त माताओं के बच्चों के लिए यह आंकड़ा 2.7% है।
- सामाजिक हाशिये पर: दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों जैसे हाशिये पर रहने वाले समूहों को स्वास्थ्य सेवा से प्रणालीगत बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
व्यवहारगत असमानताएँ
- गलत सूचना और अफवाहें: व्यापक रूप से फैली गलत सूचना भय और अविश्वास को बढ़ाती है, जिससे लोग टीके लगाने से इन्कार करने लगते हैं।
- उदाहरण के लिए, वैक्सीन को बांझपन से जोड़ने वाले झूठे व्हाट्सएप वीडियो ने हरियाणा के नूह-मेवात क्षेत्र में टीकाकरण को बुरी तरह प्रभावित किया।
- विश्वास की कमी: ऐतिहासिक अनुभवों या सांस्कृतिक मान्यताओं में निहित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में विश्वास की कमी, टीकाकरण में हिचकिचाहट को बढ़ावा देती है।
- कम जोखिम: जैसे-जैसे बीमारियाँ दुर्लभ होती जाती हैं, माता-पिता की लापरवाही बढ़ती जाती है, जिससे टीकाकरण को प्राथमिकता नहीं मिलती।
- उदाहरण के लिए, वर्ष 2022-23 के दौरान मुंबई और मलप्पुरम (केरल) में खसरे के बड़े प्रकोप सीधे तौर पर पिछले वर्षों में कम टीकाकरण कवरेज से जुड़े थे।
वैक्सीन तक पहुँच बढ़ाने में चुनौतियाँ
- लास्ट माइल डिलीवरी: भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण इलाकों में लास्ट माइल तक पहुँचना एक सतत लाजिस्टिक संबंधी बाधा बनी हुई है।
- अनियोजित शहरीकरण: तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण सघन झुग्गियाँ बनती हैं, जहाँ पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अस्थायी आबादी को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है।
- उदाहरण के लिए, मुंबई के धारावी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी अत्यधिक गतिशील आबादी के लिए निरंतर रिकॉर्ड बनाए रखने हेतु संघर्ष करते हैं, जिसके कारण टीकाकरण छूट जाता है।
- स्वास्थ्य कर्मियों पर अत्यधिक बोझ: फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों पर बहुत अधिक दबाव है, जिससे काउंसलिंग और मोबिलाइजेशन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- उदाहरण के लिए, बिहार जैसे राज्यों में, एक आशा कार्यकर्ता अक्सर 2,000 से अधिक लोगों की सेवा करती है जो 1,000 लोगों के मानक से दोगुना है ।
- डेटा प्रबंधन अंतराल: यू-विन जैसी डिजिटल पहल के बावजूद प्रवासी बच्चों के टीकाकरण पर रियलटाइम डेटा बनाए रखना एक चुनौती बनी हुई है।
आगे की राह
- लक्षित सूक्ष्म-योजना: यू-विन और सर्वेक्षणों से प्राप्त डेटा का उपयोग करके जीरो-डोज हॉटस्पॉट की पहचान करनी चाहिए और उन्हें लक्षित करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, कम प्रदर्शन करने वाले जिलों में छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करके सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 5.0 जैसे केंद्रित टीकाकरण अभियान शुरू करने चाहिए।
- व्यवहारिक संचार: गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और विश्वास बनाने के लिए स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों और सामुदायिक नेताओं का उपयोग करके लक्षित संचार को लागू करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के मेलघाट में आदिवासी माताओं के बीच वैक्सीन के प्रति संदेह का मुकाबला करने के लिए विश्वसनीय डॉक्टरों के साथ स्थानीय कोरकू भाषा के वीडियो का उपयोग करना चाहिए।
- अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण: समग्र दृष्टिकोण के लिए स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा पंचायती राज विभागों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना: निरंतर वैक्सीन आपूर्ति, कोल्ड चेन अखंडता और पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मियों को सुनिश्चित करके बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, सुदूर उत्तर-पूर्व और आदिवासी क्षेत्रों में अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना करना ताकि सुलभ टीकाकरण केंद्र के रूप में काम किया जा सके।
टीकाकरण एजेंडा 2030 के शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या को आधा करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, भारत को अपने प्रयासों को और तेज़ करना होगा। एक सतत, न्यायसंगत दृष्टिकोण जो प्रणालीगत वितरण अंतराल और बहिष्कार को बढ़ावा देने वाले गहन सामाजिक निर्धारकों दोनों को संबोधित करता हो, हर बच्चे की सुरक्षा और स्थायी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

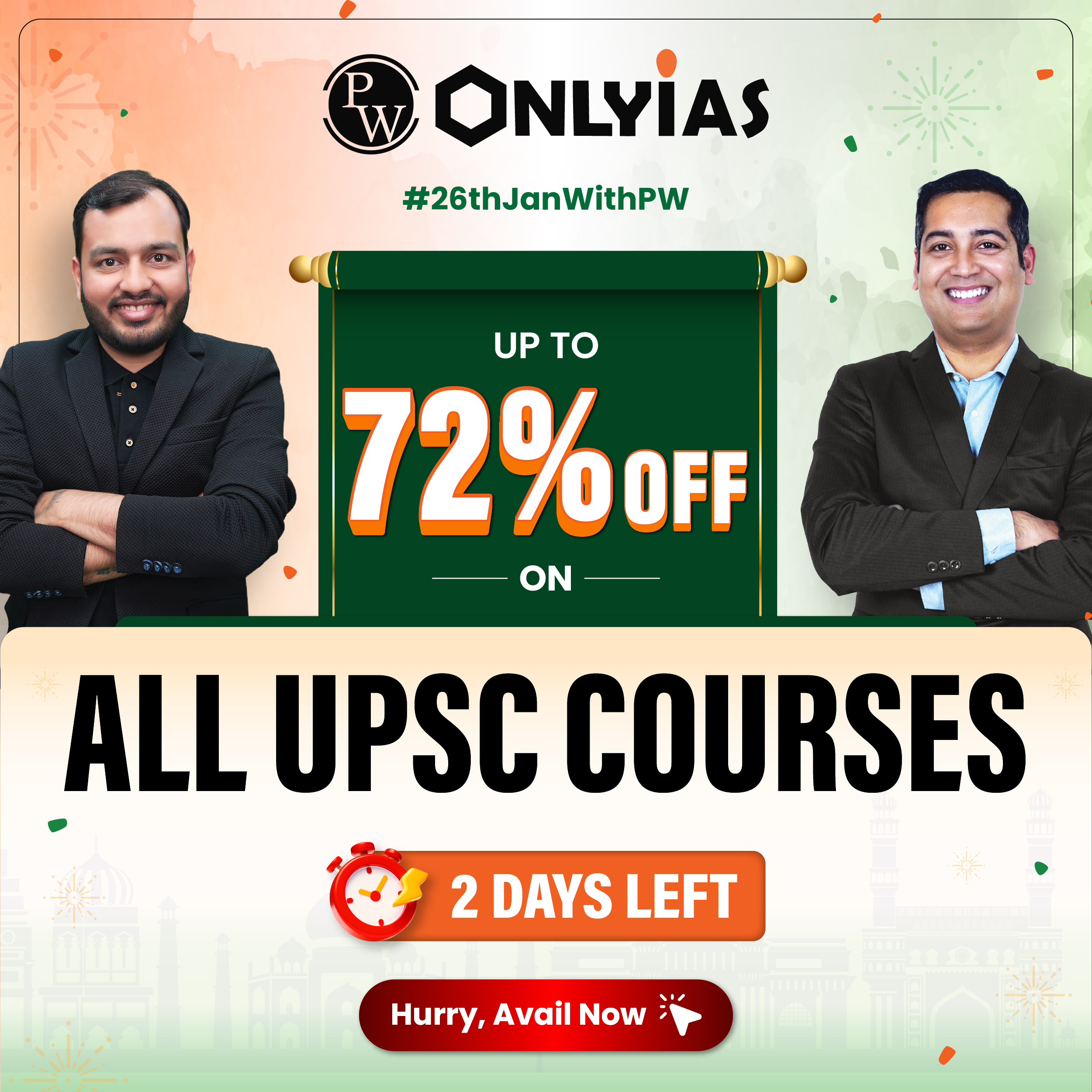
Latest Comments