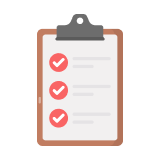भारत के भूआकृति विज्ञान की बुनियाद # |
विषयों का अध्ययन करेंगे:
|
| भारतीय भूवैज्ञानिक इतिहास |
इसे जटिल और विविध भूगार्भिक इतिहास के आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक स
र्वेक्षण ने देश की शैल क्रम को 4 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया है
| भारतीय वर्गीकरण | पृथ्वी की भूगर्भीय समय सीमा पर पत्राचार | |
| 1. | तीरंदाजी | प्रारंभिक प्रीकाम्ब्रियन ईऑन |
| 2. | पुराण | स्वर्गीय प्रीम्ब्रम्बियन |
| 3. | द्रविड़ियन | 600-400 मीटर (मोटे तौर पर पुरापाषाण युग के साथ मेल खाना) |
| 4. | आर्यन | 400mya – वर्तमान |
| पूर्व-कैंब्रियन चट्टानें |
आर्कियन क्रम की चट्टानें
- ये सबसे प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं क्योंकि इनका निर्माण तप्त व पिघली हुई पृथ्वी के ठंडे होने के क्रम में हुआ था।
- इसमें जीवाश्म अनुपस्थित होते हैं।
- अत्यधिक कायांतरण के कारण उनका मूल स्वरूप नष्ट हो गया है।
- आग्नेय चट्टानें > कायांतरण > नाइस (Gneiss)
- बुंदेलखंड नाइस सबसे पुराना है।
- प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 66% हिस्से में आर्कियन क्रम की चट्टानें पायी जाती हैं। ये वृहत हिमालय के साथ-साथ पर्वत चोटियों के नीचे भी पाई जाती हैं।
- इस क्रम की चट्टानें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के छोटानागपुर पठार और राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भाग में पाई जाती हैं।
धारवाड़ क्रम की चट्टानें
- आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणामस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ।
- इनमें जीवाश्म नहीं मिलता (इनके गठन के दौरान प्रजातियों की उत्पत्ति नहीं हुई थी ) है।
- ये पुरातन अवसादी चट्टानें होती हैं।
- विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला अरावली इन्ही चट्टानों से बनी है।
- आर्कियन क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रमुख धात्विक खनिज (सोना, लोहा, मैंगनीज आदि) इन्हीं चट्टानों में पाई जाती है।
- धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक के कावेरी घाटी, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, जबलपुर और नागपुर में सासार पर्वत तथा गुजरात में चंपानेर पर्वत श्रृंखला से दक्षिणी दक्कन क्षेत्र में पाई जाती हैं।
- उत्तर भारत में इस क्रम की चट्टानें लद्दाख, ज़ास्कर, गढ़वाल और कुमाऊँ की हिमालय पर्वत श्रृंखला तथा असम के पठार की लंबी श्रृंखला में मौजूद हैं।
कुडप्पा क्रम की चट्टानें
- आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणामस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ।
- ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर अभ्रक आदि के लिए प्रसिद्ध हैं।
- इन चट्टानों का नाम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से लिया गया है।
- ये चट्टानें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय और राजस्थान में पाई जाती हैं।
- कुडप्पा चट्टानों के अयस्कों में धातु की मात्रा कम होती है। और कहीं-कहीं पर इनका निष्कर्षण आर्थिक दृष्टिकोण से अलाभकारी होता है।
विंध्यन क्रम की चट्टानें
- ये चट्टानें कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बनने के बाद नदी घाटियों और उथले महासागरों के गाद जमाव द्वारा बनी थी। इसलिए ये चट्टानें अवसादी चट्टानें होती हैं।
- इन चट्टानों में सूक्ष्म जीवों के जीवाश्मों के साक्ष्य पाए गए हैं।
- यह चट्टानें गृह-निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। लाल किला, सांची स्तूप, जामा मस्जिद आदि की संरचना इसी क्रम की लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। इसके अतिरिक्त चीनी मिट्टी, डोलोमाइट(dolomite), चूना पत्थर आदि भी इस क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं।
- मध्य प्रदेश ( पन्ना) और कर्नाटक के गोलकोंडा की हीरे की खदानें इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं।
- ये चट्टानें मालवा पठार, सोन घाटी में सेमरी श्रेणी, बुंदेलखंड आदि में पाई जाती हैं।
| द्रविड़ समूह की चट्टाने |
द्रविड़ समूह की चट्टान (कैम्ब्रियन से मध्य कार्बोनिफेरस तक )
- इसका निर्माण प्रायद्वीपीय पठार में नहीं हुआ हैं क्योंकि यह उस समय समुद्र तल से ऊपर था।
- ये चट्टानें हिमालय में एक निरंतर क्रम में पाई जाती हैं।
- ये चट्टानें जीवाश्म से युक्त हैं।
- कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण शुरू हुआ।
- भूविज्ञान में कार्बोनिफेरस का अर्थ है- जिसमें कोयला पाया जाए।
- भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला कार्बोनिफेरस कल्प का नहीं हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन में ग्रेट लेक्स क्षेत्र का उच्च गुणवत्ता वाला कोयला और जर्मनी के रुर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला कार्बोनिफेरस कल्प का है।
- इनका निर्माण प्रायद्वीपीय पठार में नहीं हुआ हैं क्योंकि यह उस समय समुद्र तल से ऊपर था।
| आर्यन समूह की चट्टाने |
गोंडवाना क्रम की चट्टानें
- गोंडवाना शब्द मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र से लिया गया है।
- भारत में 98% कोयला इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है।
- गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस कोयले की तुलना में बहुत बाद का बना हुआ है इसलिए इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है।
- इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस और जुरासिक काल के बीच हुआ था।
- कार्बोनिफेरस कल्प के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में विवर्तनिक हलचल द्वारा कई दरारों/संकरी घाटियों का निर्माण हुआ। तथा इन संकरी दरारों में नदियों द्वारा लाए गए पदार्थों के जमाव से इस अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ।
- उस काल की वनस्पतियों के जमीन के अन्दर दबने के परिणामस्वरूप कोयले का निर्माण हुआ।
- यह कोयला अब मुख्य रूप से दामोदर नदी, सोन, महानदी, गोदावरी और वर्धा नदी घाटियों में पाया जाता है।
जुरासिक क्रम :
- जुरासिक के उत्तरार्ध में समुद्री जल के क्रमिक फैलाव ने राजस्थान और कच्छ में उथले पानी के जमाव की वृहत् श्रृंखला को जन्म दिया।
- मूंगा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पिण्ड और शेल्स, कच्छ से प्राप्त होते हैं।
- प्रायद्वीप के पूर्वी तट गुंटूर और राजमुंदरी के बीच ठीक ऐसे ही सागरी जल का फैलाव पाया गया।
दक्कन ट्रैप
- मेसोज़ोइक महाकल्प की अंतिम काल (क्रेटेशियस कल्प ) में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी प्रक्रिया शुरू हुई जिसके परिणामस्वरूप दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ।
- यह संरचना बेसाल्ट और डोलोराइट चट्टानों से बनी है।
- ज्वालामुखी की इन चट्टानों में लावा के बीच कुछ पतली जीवाश्म अवसादी परतें पायी जाती हैं। यह लावा के असतत प्रवाह को इंगित करता है। ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण दो बड़ी घटनाएं हुईं थीं:
- गोंडवानालैंड का विभाजन।
- टेथिस सागर से हिमालय का उत्थान।
- ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं और इन चट्टानों के लंबे समय तक हुए अपक्षय के परिणामस्वरूप काली कपासी मिट्टी का निर्माण हुआ जिसे ‘रेगुर’ के नाम से भी जाना जाता है।
- यह संरचना महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है।
तृतीयक कल्प की चट्टानें
- तृतीयक कल्प को कालानुक्रमिक रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है
- इयोसीन
- ओलिगोसीन
- मायोसीन
- प्लायोसीन
- भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास के लिए यह कल्प, हिमालय के विकास के कारण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है।
- हिमालय पर्वत श्रृंखला का विकास निम्न क्रम में हुआ है:
-
- बृहत हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन काल के दौरान हुआ था।
- मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन काल के दौरान हुआ था।
- शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन और ऊपरी प्लायोसीन काल के दौरान हुआ था।
- असम, राजस्थान और गुजरात में खनिज तेल इयोसीन और ओलिगोसीन काल के चट्टानों में पाया जाता है।
चतुर्थ (Quarternary) कल्प की चट्टानें
- ये चट्टानें गंगा और सिंधु नदी के मैदानों में पाई जाती हैं।
- चतुर्थ कल्प को कालानुक्रमिक रूप से दो भागों में बांटा गया है
प्लेइस्टोसिन काल
- पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे ‘बांगर’ के नाम से जाना जाता है, का निर्माण ऊपरी और मध्य प्लीस्टोसीन काल के दौरान हुई थी।
- कश्मीर घाटी शुरुआत में एक झील थी लेकिन मिट्टी के निरंतर निक्षेपण ने वर्तमान स्वरूप (घाटी) को जन्म दिया, जिसे ‘करेवा‘ के नाम से जाना जाता है।
- प्लीस्टोसीन काल का निक्षेपण थार रेगिस्तान में भी पाया जाता है।
होलोसीन युग
- खादर’ के रूप में जानी जाने वाली जलोढ़ मिट्टी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल के अंत में शुरू होकर होलोसीन काल तक चला।
- ‘कच्छ का रण’ पहले समुद्र का एक हिस्सा था जो प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल के दौरान अवसादी निक्षेपण से भर गया।
| भारत का भूगोल |
भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7 वाँ सबसे बड़ा देश है। जिसे हिमालय शेष एशिया से अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है।
| मानचित्र कुंजी (map key): |
- भारत के द्वीप समूह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं।
- मानचित्र में दिखाये गए देश भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं ।
- गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
- सबसे उत्तरी अक्षांश जम्मू और कश्मीर में इंदिरा कोल है।
- भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी अक्षांश तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। ध्यान दें कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। इंदिरा पॉइंट को पहले पैग्मलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के रूप में जाना जाता था।
- मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी देशांतरीय विस्तार को दिखाया गया है।
- समुद्र से तीन तरफ से घिरा क्षेत्र
- श्रीलंका और भारत को अलग करने वाला जलडमरूमध्य, पाक जलडमरूमध्य है।
- भारत के संघ शासित प्रदेश को दिखाया गया है।
भारत के बारे में भौगोलिक तथ्य
- भारत का क्षेत्रफल28 लाख वर्ग किमी. है।
- भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग4 प्रतिशत है।
- भारत का तट पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तक फैली है।
- गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच दो घंटे का समय अंतर होता है। (1 ° = 4 मिनट)।
- उत्तर से दक्षिण तक मुख्य भूमि की अधिकतम लंबाई लगभग 3214 किमी है।
- पूर्व से पश्चिम तक की मुख्य भूमि की अधिकतम लंबाई लगभग 2933 किमी है।
- भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 6,100 किमी है तथा अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूह सहित लगभग 7,516 किलोमीटर है।
- भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र से 12 समुद्री मील (यानी लगभग9 किमी) तक फैली हुई है।
भारतीय मानक याम्योत्तर
- 82° 30‘ पूर्वी मध्यान्ह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर को पार करते हुए गुजरती हैं। इसको भारत के मानक याम्योत्तर के रूप में जाना जाता है।
- भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से (जिसे जीएमटी या 0 ° या प्रधान याम्योत्तर के रूप में भी जाना जाता है) 5 घंटे 30 मिनट आगे है।
- कर्क रेखा (23 ° 30’N) गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है।
देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार
- कर्क रेखा देश के मध्य से होकर गुजरती है जो इसे दो बराबर अक्षांशीय हिस्सों में विभाजित करती है
- कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र इसके दक्षिण में स्थित क्षेत्र का लगभग दोगुना है।
- 22 ° उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में देश प्रायद्वीप के रूप में हिंद महासागर से 800 किमी अधिक दूर है।
- यह अवस्थिति देश में जलवायु, मिट्टी के प्रकार और प्राकृतिक वनस्पतियों में बड़े बदलाव के लिए जिम्मेदार है।
भारत उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय देश?
कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित देश का आधा भाग उष्णकटिबंधीय या गर्म क्षेत्र में स्थित है और दूसरा कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है।
- हिमालय द्वारा देश को शेष एशिया से अलग किया जाता है
- इसकी जलवायु पर उष्णकटिबंधीय मानसून का अधिक प्रभाव होता है।
- हिमालय ठंडी शीतोष्ण वायु धाराओं को रोकता है।
अतः भारत मुख्य रूप से हिमालय के कारण उष्णकटिबंधीय देश है।
| संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि |
- समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) को समुद्री विधि संधि के रूप में भी जाना जाता है।
- इसे “महासागरों का संविधान” माना जाता है।
- नवीनतम समुद्री विधि का संस्करण UNCLOS III है। इसमें समुद्री सीमाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है।
यह समुद्र में खनन, पर्यावरण संरक्षण, समुद्री सीमा और विवाद निपटान का कार्य करता है।
UNCLOS महासागरों को निम्न प्रकार से विभाजित करता है
प्रादेशिक जल
- बेसलाइन से 12 नॉटिकल मील।
- देश इसके संसाधनों का उपयोग करने और कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
- “निर्दोष गमन के मार्ग” (innocent passage) को छोड़कर विदेशी जहाजों को गुजरने के सभी अधिकार नहीं दिए गए हैं।
- ऐसे जलमार्गो से गुजरता है जो शांति और सुरक्षा की दृष्टि के पूर्वाग्रह से मुक्त है।
- राष्ट्रों को निर्दोष गमन मार्ग को बन्द करने का अधिकार है।
- किसी देश के क्षेत्रीय जल से गुजरते समय पनडुब्बी को सतह पर चलना होता हैं और अपने झंडे दिखाने होते हैं।
समीपवर्ती क्षेत्र
- क्षेत्र 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक जल से आगे (यानी आधारभूत सीमा से 24 समुद्री मील)।
- देश केवल 4 क्षेत्रों में कानून लागू कर सकता है – प्रदूषण, कराधान, सीमा शुल्क और अप्रवास पर ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ)
- बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्र के किनारे का क्षेत्र।
- सभी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर संबंधित देश का एकाधिकार होता है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण मछली पकड़ने के अधिकार और तेल अधिकारों पर होने वाली झड़पों को रोकना था।
- विदेशी जहाजों को तटीय राज्यों के विनियमन के अधीन रहकर , नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता है।
- विदेशी राज्यों को पनडुब्बी पाइप और केबल बिछाने की अनुमति है।
भारत और उसके पड़ोसी
- भारत की 7 किलोमीटर की स्थलीय सीमा 7 देशों की स्थलीय सीमा से घिरी हुई है।
- भारत उत्तर और पूर्वोत्तर में नवीन वलित पर्वतों (बृहत् हिमालय) से घिरा हुआ है ।
- प्राचीन समय में भारत के व्यापारिक संबंध यहां के जलमार्ग और पर्वत-पठार के कारण अत्यधिक प्रभावित हुए थे।
- भारत उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ; उत्तर में चीन, तिब्बत (चीन), नेपाल के साथ; उत्तर-पूर्व में भूटान; और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है।
- भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है।
- श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित भारत के दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं।
- मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य( pak strait) श्रीलंका को भारत से अलग करता है।
| पड़ोसी | सीमा की लंबाई (किमी में) | सीमावर्ती राज्य |
| बांग्लादेश | 4096 | पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम |
| चीन | 3488 | जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश |
| पाकिस्तान | 3322 | जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात |
| नेपाल | 1751 | उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम |
| म्यांमार | 1643 | अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम |
| भूटान | 699 | सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश |
| अफ़ग़ानिस्तान | 106 | जम्मू और कश्मीर (पीओके में वाखान कॉरिडोर) |
| उत्तरी और पूर्वोत्तर पर्वत |
हिमालय ( भूगर्भीय रूप से युवा और वलित पर्वत) भारत के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। ये पर्वत श्रृंखलाएं सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। हिमालय दुनिया के सबसे ऊबड़-खाबड़ पर्वतीय बाधाओं में से एक है। वे एक चापाकार (arc shaped) आकृति बनाते हैं, जो लगभग 2,400 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। इनकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। पश्चिमी हिस्से की तुलना में पूर्वी भाग में ऊंचाई की भिन्नताएं अधिक हैं। हिमालय अपने अनुदैर्ध्य विस्तार में तीन समानांतर पर्वत श्रेणियों को शामिल करता हैं। इन श्रेणियों के बीच कई घाटियाँ हैं। सबसे उत्तरी सीमा को महान या भीतरी हिमालय या ‘हिमाद्रि‘ के रूप में जाना जाता है। यह 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची चोटियों से युक्त है। इसमें हिमालय की सभी प्रमुख चोटियाँ पायी जाती हैं।
| हिमालय का गठन |
- 225 मिलियन वर्ष पूर्व (MA) भारत एक बड़ा द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर था और टेथिस महासागर द्वारा एशिया से अलग था।
- सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया 200 मिलियन वर्ष पहले (Ma) विघटित होना आरम्भ हुआ और भारत का एशिया की ओर एक उत्तरमुखी बहाव शुरू हुआ।
- 80 मिलियन वर्ष पहले (Ma) भारत एशियाई महाद्वीप से 6,400 किमी दक्षिण में था लेकिन प्रति वर्ष 9 से 16 सेमी की दर से यह इसकी ओर बढ़ रहा था।
- एशिया के नीचे टेथिस महासागरीय नितल उत्तर की ओर बढा होगा और प्लेट सीमान्त महासागरीय-महाद्वीपीय हो गई होगी जैसा की वर्तमान एंडीज श्रेणी ।
- लगभग 50-40 मिलियन वर्ष पहले , भारतीय महाद्वीपीय प्लेट के उत्तरोत्तर अपवाह की दर लगभग 4-6 सेमी प्रति वर्ष हो गई।
- इस दर मे कमी को, यूरेशियन और भारतीय महाद्वीपीय प्लेटों के बीच टकराव की शुरुआत, पूर्व टेथिस महासागर के समापन और हिमालय के उत्थान की शुरुआत के रूप में चिह्नित किया गया है।
- यूरेशियन प्लेट आंशिक रूप से टूटने लगी और भारतीय महाद्वीप प्लेट के ऊपर आ गई, लेकिन उनके कम घनत्व के कारण दोनों मे से किसी भी महाद्वीपीय प्लेट का क्षेपण नही हो सका।
- हिमालय और तिब्बती पठार को ऊपर की ओर धकेलने वाले संपीडित बलों द्वारा वलन और भ्रंशन ( folding and faulting) के कारण यह महाद्वीपीय परत मोटी हो गई।
- भारत एशिया के पूर्वोत्तर में लगातार संचलित हो रहा है इसलिए हिमालय अभी भी प्रति वर्ष 1 सेमी अधिक ऊँचा हो रहा है, जो आज इस क्षेत्र में उथले फोकस वाले भूकंपों की घटनाओं का स्पष्ट कारण है।
| विशेषताएं |
- हिमालय का दक्षिणी भाग धनुषाकार या चापाकार है।
- हिमालय का यह घुमावदार आकार इसके उत्तर की ओर संचलन के दौरान भारतीय प्रायद्वीप के दोनो किनारों पर लगने वाले बल के कारण हुआ है।
- उत्तर-पश्चिम में यह बल अरावली द्वारा और पूर्वोत्तर में असम पर्वतश्रेणी द्वारा लगाया गया था।
- पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है तथा पूर्व की ओर हिमालय संकरा होता चला गया है जिसके कारण पूर्वी हिमालय की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय के अपेक्षाकृत अधिक है।
हिमालय के अक्षसंघीय मोड़
पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज, पश्चिम में सिन्धु गार्ज में हिमालय पूर्व – पश्चिम तक फैला है और इन घाटियों पर तेज दक्षिणमुखी मोड़ लेता है। इन मोड़ों को हिमालय के अक्षसंघीय मोड़ के नाम से जाना जाता है।
- पश्चिमी अक्षसंघीय मोड़ नंगा पर्वत के पास पाया जाता है।
- पूर्वी अक्षसंघीय मोड़ नमचा बरवा के पास है।
| हिमालय का विभाजन |
| उत्तर हिमालय प्रभाग
1. पार्श्व विभाजन अनुदैर्ध्य प्रभाग
|
- हिमालय पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिमालय में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- कभी-कभी तिब्बत हिमालय को शामिल करके एक और वर्गीकरण जोड़ा जाता है जिसमें तिब्बत के पठार के दक्षिणी किनारे शामिल होते हैं।
- पश्चिमी हिमालय में जम्मू और कश्मीर, पीरपांजाल, लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र शामिल हैं।
- मध्य हिमालय जम्मू और कश्मीर से सिक्किम तक फैला है और इसमें हिमाचल, गढ़वाल, पंजाब और नेपाल का क्षेत्र शामिल है।
- पूर्वी हिमालय सिक्किम से असम तक फैला हुआ है और इसमें भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम श्रृंखलाएं शामिल है।
हिमालय पर्वत श्रृंखला को तुंगता(ऊंचाई) के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है:
1.बृहत हिमालय जिसमें निम्न शामिल हैं:
- महान हिमालय (हिमाद्री)
- पार-हिमालय श्रृंखला
- मध्य हिमालय (हिमांचल श्रृंखला)
- बाह्य या उप-हिमालय (शिवालिक श्रृंखला )
हिमालय
|
| पार्श्व मंडल |
- पूर्व की तुलना में पश्चिम में हिमालय अधिक चौड़ा है।
- चौड़ाई कश्मीर में 400 किमी से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 160 किमी तक है।
- इस अंतर के पीछे मुख्य कारण यह है कि संपीडनात्मक बल पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक है।
- इसीलिए पूर्वी हिमालय में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियाँ मौजूद हैं।
- विभिन्न श्रेणीयों को गहरी घाटियों द्वारा अलग किया जाता है जो एक अत्यधिक विच्छेदित स्थलाकृति बनाती है।
- भारत की ओर हिमालय का दक्षिणी ढाल तीक्ष्ण है जबकि तिब्बत की और इसकी ढाल सामान्य हैं।
- इसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े हिमनद शामिल हैं और गंगोत्री एवं यमुनोत्री हिमनद सहित इनकी संख्या 15000 तक पहुँच जाती है।
- हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती हैं और इनमें साल के लगभग हर महीने में पानी होता है।
- दुनिया की आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा हिमालय प्रणाली के जल पर निर्भर करता है।
- हिमालय का बेसिन लगभग 19 नदियों द्वारा बना है। जिन्हें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की तीन प्रमुख नदी प्रणालियों में बांटा जा सकता है।
- नदियों के अलावा हिमालय श्रृंखला में कई मीठे पानी एवं खारे पानी की झीले मौजूद है।
- मत्वपूर्ण झीलों में तिलिचो, पैगोंग सो और यमद्रोक सो झील शामिल हैं।
| बृहत् हिमालयन पर्वत श्रृंखला |
पार–हिमालयन श्रृंखला (तिब्बती हिमालय)
हिमालय के इस भाग की अधिकांश सीमा तिब्बत में स्थित है और इसलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। यह सीमा हिमाद्रि के उत्तर में मुख्य श्रेणियों के साथ स्थित है।
जास्कर
- यह 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास महान हिमालय से अलग हो जाती है और इसके समानांतर चलती है।
- नंगा पर्वत (8126 मीटर) उत्तर-पश्चिम में ज़ास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इसके अंतर्गत निकटवर्ती देवसई पर्वत को भी शामिल किया जा सकता है।
- लद्दाख श्रेणी ज़ास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है, जो इसके समानांतर चलता है।
काराकोरम (उत्तरतम सीमा)
- इसे कृष्णगिरि के नाम से भी जाना जाता है, जो ट्रांस-हिमालय पर्वतमाला के उत्तरी भाग में स्थित है।
- दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर इसमें स्थित है।
- यह चीन और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है।
- K2 (गॉडविन ऑस्टिन) दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है।
लद्दाख
- यह लेह के उत्तर में स्थित है।
- यह तिब्बत में कैलाश श्रृंखला के साथ मिल जाता है।
कैलाश
पामीर ग्रंथि (Pamir knot)
- पामीर पर्वत की एक अद्वितीय भौगोलिक विशेषता है।
- यह दुनिया की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के अभिसरण को संदर्भित करता है। जिसमें तियान- शान, काराकोरम, कुनलुन शान, हिन्दकुश और पामीर श्रेणी शामिल हैं।
- कई देश पामीर गाँठ पर अपना दावा करते हैं जबकि यह वास्तव में पूर्वी ताजिकिस्तान के गोर्नो-
बदाख-शान स्वायत्त क्षेत्र में है।
महान हिमालय (हिमाद्रि)
- हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी सीमा।
- 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची चोटियों से मिलकर बनी श्रेणी है ।
- इसमें हिमालय की सभी प्रमुख चोटियाँ शामिल हैं।
- यह अक्षसंघीय मोड़ पर आकर समाप्त हो जाती हैं ।
- महान हिमालय की तहें प्रकृति में विषम हैं। हिमालय के इस भाग का मुख्य भाग ग्रेनाइट से बना है।
- चोटियाँ ऊंचाई के कारण बर्फ से ढकी रहती हैं। इसलिए इसका नाम हिमाद्रि भी है
- हिमालय की लगभग सभी प्रमुख चोटियाँ इस श्रेणी में स्थित हैं जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि।
- गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे प्रसिद्ध ग्लेशियर यहाँ स्थित हैं।
- वनों के प्रकार → शंकुधारी वृक्ष
मध्य हिमालय (हिमांचल श्रेणी)
- यह सीमा दक्षिण में शिवालिक और उत्तर में महान हिमालय के बीच स्थित है।
- अधिकांश बीहड़ पर्वतीय तंत्र अत्यधिक संकुचित और परिवर्तित चट्टानों से बनी हैं।
- ऊँचाई 3,700 से 4,500 मीटर के बीच और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है।
- इसमें मुख्य रूप से रूपांतरित चट्टानें हैं।
- इस श्रेणी के पूर्वी भाग के ढलान घने जंगलों से आच्छादित हैं।
- इस श्रेणी के दक्षिण की ओर तीब्र ढाल है और यह आम तौर पर किसी भी वनस्पति से रहित हैं।
- जबकि इस श्रेणी की उत्तरी ढाल घनी वनस्पतियों से आच्छादित है।
- स्थानीय नाम -जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल; हिमाचल प्रदेश में धौलाधार।
- शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि जैसे पहाड़ी शहर हिमाचल में स्थित हैं।
- सभी बड़ी घाटियाँ जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी यहाँ मौजूद हैं।
- वनों के प्रकार → चौड़े पत्तों वाले ,सदाबहार वन
बाह्य या उप हिमालय (शिवालिक श्रेणी )
- हिमालय की सबसे दक्षिणी और बाहरी सीमा जो विशाल मैदानों और निम्न हिमालय के बीच स्थित है।
- इसे प्राचीन काल में मानक पर्वत के रूप में भी जाना जाता था।
- इनका विस्तार 10-50 किलोमीटर की चौड़ाई और 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई तक है।
- ये पर्वतमाला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय पर्वतमाला से नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बनी हैं।
- ये घाटियाँ मोटी बजरी और जलोढ़ से आच्छादित हैं।
- 80-90 किमी के अंतराल को छोड़कर ये कम ऊँची पहाड़ियां लगभग अखंड श्रृंखला हैं जो तीस्ता नदी और रैडक नदी की घाटी द्वारा आच्छादित है।
- अधिकांश दून और दुआर इस श्रेणी में स्थित हैं।
- वनों के प्रकार → पर्णपाती प्रकार के वन
दून:
दून अनुदैर्ध्य घाटियां हैं जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने के कारण हुए वलन के परिणामस्वरूप बनी हैं । ये निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच बने हैं। इन घाटियों में हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए मोटे जलोढ़ का निक्षेपण पाया जाता है। इन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में दुआर के नाम से जाना जाता है । देहरा दून ,कोटली दून और पटली दून कुछ प्रसिद्ध दून हैं।
Chhos / चोस
नेपाल तक शिवालिक श्रेणी का पूर्वी भाग घने जंगलों से ढका हुआ है। जबकि पश्चिम में वनावरण कम घना है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढाल लगभग वन आवरण से रहित हैं और मौसमी धाराओं द्वारा निर्देशित हैं। ऐसे क्षेत्रों को स्थानीय रूप से चोस (chhos) के रूप में जाना जाता है। इसे आमतौर पर पंजाब के होशियारपुर जिले में देखा जाता है।
| शिवालिक का नाम | क्षेत्र |
| जम्मू क्षेत्र | जम्मू की पहाड़ियाँ |
| दफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ी | अरुणाचल प्रदेश |
| धंग श्रेणी , डंडवा श्रेणी | उत्तराखंड |
| चुरिया घाट हिल्स | नेपाल |
| अनुदैर्ध्य विभाजन |
नदी घाटी के आधार पर हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक विभाजन निम्न तरीके से किया गया है।
पंजाब हिमालय
- सिंधु और सतलुज नदियों के बीच का हिमालय क्षेत्र (560 किमी लंबा)।
- सिंधु नदी प्रणाली की सभी प्रमुख नदियाँ पंजाब हिमालय से होकर बहती हैं।
- पंजाब हिमालय का एक बड़ा हिस्सा जम्मू- कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। इसलिए उन्हें कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है।
- प्रमुख श्रेणियां: काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, ज़ास्कर और धौलाधार।
- कश्मीर हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है जो केसर की स्थानीय किस्म ज़ाफ़रान की खेती के लिए उपयोगी हैं।
- दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण ग्लेशियर जैसे बोल्तारो और सियाचिन भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
- लद्दाख पठार और कश्मीर घाटी, कश्मीर हिमालय क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
कुमाऊं हिमालय
- कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है और सतलुज से काली नदी तक फैला हुआ है।
- कुमाऊं हिमालय में लघु हिमालय का प्रतिनिधित्व, मसूरी और नाग टिबा पर्वतमाला द्वारा किया जाता है।
- भूआकृति विज्ञान के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र की दो विशेषताएं ‘शिवालिक’ और ‘दून ‘ निर्माण हैं।
- इस क्षेत्र में शिवालिक, गंगा और यमुना नदियों के बीच मसूरी श्रेणी के दक्षिण में स्थित है।
- इस क्षेत्र में पाँच प्रसिद्ध प्रयाग (नदी संगम) हैं।
नेपाल हिमालय
- बृहत् हिमालय श्रृंखला इस हिस्से में अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करती है।
- यह पश्चिम में काली नदी और पूर्व में तीस्ता नदी के बीच मे स्थित है।
- प्रसिद्ध चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाईथान और धौलागिरी यहाँ स्थित हैं।
- इस क्षेत्र में लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है।
- इसकी श्रेणी को घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियों द्वारा पार किया जाता है।
- महान और लघु हिमालय के बीच में काठमांडू और पोखरा सरोवर घाटियाँ हैं।
असम हिमालय
- हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में तीस्ता नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है और लगभग 720 किमी की दूरी तक फैला है।
- यह कंचनजंगा जैसी उच्च पर्वत चोटियों का एक क्षेत्र है।
- इसका दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है लेकिन उत्तरी ढाल मंद हैं।
- ब्रिटिशों ने इस क्षेत्र में चाय के बागानों की शुरूआत की थी।
- ‘दुआर संरचनाओं’ के लिए प्रसिद्ध, जैसे- बंगाल दुआर ‘
- इस क्षेत्र में हिमालय संकरा है और यहाँ लघु हिमालय बृहत् हिमालय के करीब है।
- असम हिमालय भारी वर्षा के कारण नदी-संबंधी कटाव का एक प्रमुख प्रभाव दर्शाता है।
- जेलेप ला पास- भारत – चीन-भूटान का त्रि-जंक्शन- इस क्षेत्र में स्थित है।
| पूर्वी हिमालय |
उत्तर–पूर्वी पहाड़ी और पर्वत
- दिहांग घाटी के बाद हिमालय अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। उत्तर-दक्षिण दिशा म्यांमार और भारत की सीमा के साथ में चलने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से पूर्वांचल पहाड़ी के रूप में जाना जाता है।
- पूर्वांचल की पहाड़ियों को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है जैसे पटकाई बुम, नागा पहाड़ी, कोहिमा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिज़ो पहाड़ी (पहले लुशाई पहाड़ी के रूप में जाना जाता था), त्रिपुरा पहाड़ी और बरैल श्रेणी।
- ये पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती हैं।
- ये पहाड़ियाँ पैमाने और उच्चावच में भिन्न हैं लेकिन इनकी उत्पत्ति हिमालय से ही हुई है।
- वे ज्यादातर सैंडस्टोन (यानी तलछटी चट्टानों) से बने होते हैं।
- ये पहाड़ियाँ घने जंगलों से आच्छादित हैं।
- उत्तर से दक्षिण की ओर इनकी ऊँचाई कम होती जाती है। हालांकि तुलनात्मक रूप से कम ऊँची होती हैं क्योंकि ये पहाड़ी ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों, घने जंगलों और तेज़ धाराओं के कारण परिवर्तन का विरोध करती हैं।
इन पहाड़ियों से बनी है:
- पटकाई बूम – अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच की सीमा
- नागा पहाड़ियाँ
- मणिपुरी पहाड़ियाँ – मणिपुर और म्यांमार के बीच की सीमा
- मिजो पहाड़ियाँ
- पटकाई बूम और नागा पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती हैं।
पूर्वांचल पहाड़ियों का अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक विस्तार
- पूर्वांचल हिमालय का विस्तार म्यांमार श्रृंखला (अराकान योमा) और यहां से आगे इंडोनेशिया द्वीप समूह से होते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक विस्तृत है।
पश्चिमी और पूर्वी हिमालय के बीच मुख्य अंतर
| पश्चिमी हिमालय | पूर्वी हिमालय |
| 1. नदी काली (लगभग 80 ° E देशांतर) के पश्चिम तक फैली हुई है।
2. इस भाग के मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ऊंचाई कई चरणों में बढ़ जाती है। मैदानी इलाकों से ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं लंबी दूरी पर हैं
3. यहाँ वर्षा की मात्रा कम है और पूर्वी हिमालय की 1/4 वीं है।
4. पश्चिमी हिमालय में प्रमुख वनस्पति शंकुधारी वन और अल्पाइन वनस्पतियाँ हैं। प्राकृतिक वनस्पति कम वर्षा के प्रभाव को दर्शाती है।
5. पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई पूर्वी हिमालय से अधिक है
6. स्नोलाइन पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है
7. पश्चिमी हिमालय में अधिक वर्षा होती है सर्दियों में उत्तर पश्चिम से
8. पूर्वी हिमालय की तुलना में कम जैव विविधता |
1. यह सिक्किम में सिंगालीला पर्वतमाला के पूर्व (88 ° E देशांतर) से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमाओं तक माना जाता है।
2 यह हिस्सा मैदानी इलाकों से अचानक उगता है। इस प्रकार चोटियाँ मैदानों से दूर नहीं जाती हैं (उदाहरण: कंचनजंगा)
3. यह क्षेत्र पश्चिमी हिमालय की तुलना में 4 गुना अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अधिक वर्षा के कारण, यह घने जंगलों से आच्छादित है। 4. स्नोलाइन पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक है
5. पूर्वी हिमालय ग्रीष्मकाल में दक्षिण-पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है।
6. जैव विविधता के मामले में पश्चिमी हिमालय से बहुत आगे और एक है जैव विविधता के आकर्षण के केंद्र |
| भारत के महत्वपूर्ण दर्रे |
पर्वतों के आर-पार विस्तृत सँकरे और प्राकृतिक मार्ग, जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है, दर्रे कहलाते हैं| परिवहन, व्यापार, युद्ध अभियानों और मानवीय प्रवास में इन दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है| भारत के अधिकतर दर्रे हिमालय क्षेत्र में पाये जाते हैं|
J & K के दर्रे
| चांग-ला | तिब्बत के साथ लद्दाख |
|
| खारदुंग ला | लद्दाख में लेह सीमा के पास |
|
| लनक ला | भारत और चीन (अकसाई)
जम्मू और कश्मीर का चिन क्षेत्र) |
|
| पीर-पंजाल पास | पीर पंजाल रेंज के पार |
|
जम्मू और कश्मीर
| नाम | महत्व (कनेक्ट) | टिप्पणियाँ |
| मिंटका पास | कश्मीर और चीन |
|
| पारपिक दर्रा | कश्मीर और चीन |
|
| खुंजेरब पास | कश्मीर और चीन | भारत-चीन सीमा |
| अघिल पास | झिंजियांग प्रांत (चीन) के साथ लद्दाख |
|
| बनिहाल दर्रा | जम्मू और श्रीनगर |
|
|
हिमाचल प्रदेश के दर्रे
| बारा लचा ला | हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर |
|
| देबसा पास | कुल्लू और स्पीति जिले के बीच की कड़ी |
|
| रोहतांग दर्रा | कुल्लू के बीच सड़क संपर्क, लाहुल और स्पीति घाटियाँ |
|
| शिपकी ला | हिमाचल प्रदेश और ती |
|
उत्तराखंड के दर्रे
उत्तराखंड
| लिपु लेख | उत्तराखंड का निर्माण (भारत), तिब्बत (चीन) और नेपाल की सीमाएँ | कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्री इस दर्रे का उपयोग करते हैं। |
| मन पास | उत्तराखंड तिब्बत के साथ | 5610 की ऊंचाई
बद्रीनाथ के थोड़ा उत्तर में स्थित है
सर्दियों के मौसम में बंद रहता है (Nov – Apr) |
| मंगशा धुरा | उत्तराखंड तिब्बत के साथ | इसका उपयोग कैलाश-मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाता है |
| नीती पास | उत्तराखंड तिब्बत के साथ | यह सर्दियों के मौसम में बंद रहता है (Nov – Apr) |
| मुलिंग ला | उत्तराखंड तिब्बत के साथ | 5669 की ऊँचाई पर गंगोत्री के उत्तर में स्थित है |
सिक्किम के दर्रे
सिक्किम
| नाथु ला | तिब्बत के साथ सिक्किम |
|
| जलेप ला | सिक्किम-भूटान की सीमा |
|
अरुणाचल प्रदेश के दर्रे
अरुणाचल प्रदेश
| बम दि ला | अरुणाचल प्रदेश और भूटान |
|
| दिहांग पास | अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार |
|
| योंग्यप पास | तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश | |
| डिफर पास (दिफू पास) | भारत चीन और म्यांमार की तिकड़ी |
|
हिमालय में ग्लेशियर और हिम रेखा # |
किसी पर्वत या उच्च भूमि पर वह कल्पित रेखा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है। यह स्थायी हिमावरण की निम्नतम सीमा होती है। इस रेखा के नीचे संचित हिम ग्रीष्म ऋतु में पिघल जाती है किन्तु इसके ऊपर का भाग सदैव हिमाच्छादित रहता है।
पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा पूर्वी हिमालय की तुलना में कम ऊंचाई पर होती है। #
- उदाहरण के लिए सिक्किम में कंचनजंगा के हिमनद मुश्किल से 4000 मीटर से नीचे हैं, जबकि कुमाऊं और लाहुल में 3600 मीटर और कश्मीर हिमालय के ग्लेशियर समुद्र तल से 2500 मीटर तक हैं।
- इसका कारण अक्षांश में वृद्धि है जो कंचनजंगा में 28 ° N से काराकोरम में 36 ° N तक देखी जा सकती हैं (निम्न अक्षांश > गर्म तापमान > उच्च हिम रेखा )।
- इसके अलावा पूर्वी हिमालय, उच्च श्रेणियों के हस्तक्षेप के बिना पश्चिमी हिमालय से औसतन ऊँचा उठा हुआ है।
- पश्चिमी हिमालय में कुल वर्षा बहुत कम होती है लेकिन पूरे वर्षभर बर्फ के रूप में वर्षा होती है।
- बृहत् हिमालयन पर्वतमाला के उत्तरी ढलान की तुलना में दक्षिणी ढलानों पर कम ऊंचाई की हिम रेखा हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तरी ढलानों की तुलना में दक्षिणी ढलान अधिक खड़ी हैं तथा ये अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं।
ग्लेशियर- ये ग्रेट हिमालय और ट्रांस-हिमालय पर्वतमाला (काराकोरम, लद्दाख और ज़ास्कर) में पाए जाते हैं। लघु हिमालय में छोटे ग्लेशियर हैं हालांकि बड़े ग्लेशियरों के प्रमाण पीरपंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं।
| हिमालय की महत्वपूर्ण घाटियाँ |
- कश्मीर घाटी और करेवा की घाटी
- हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुलु घाटी;
- दून घाटी (दून घाटी, देहरादून घाटी); उत्तराखंड में भागीरथी घाटी (गंगोत्री के पास) और मंदाकिनी घाटी (केदारनाथ के पास)
- नेपाल में काठमांडू घाटी।
| हिमालय– मीठे पानी / नदियों का स्रोत:- |
- हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के साथ विश्व की कुछ सबसे बड़ी नदियों का स्रोत है ।
- ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद यह पृथ्वी पर मीठे पानी (freshwater) का सबसे बड़ा स्रोत है ।
- पृथ्वी पर अंटार्कटिक और आर्कटिक के बाद बर्फ का यहां तीसरा सबसे बड़ा जमाव है ।
- इसमें गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर सहित दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियरों के साथ लगभग 15000 ग्लेशियर हैं ।
- हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती हैं और इनमें वर्ष भर पानी होता है ।
- दुनिया की आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा हिमालय तंत्र के जल पर निर्भर है ।
- हिमालय बेसिन में 19 नदियां हैं। तथा उन्हें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की तीन प्रमुख नदी तंत्र में बांटा जाता है ।
- नदियों के अलावा, हिमालय श्रृंखला में बड़ी संख्या में मीठे पानी की झीलें हैं ।
- कुछ महत्वपूर्ण झीलों में तिलिचो, पैगांग सो और यमद्रोक सो झील शामिल हैं ।
| भारत के लिए हिमालय का महत्व :- |
| जलवायु का महत्व | • हिमालय की ऊँचाई, फैलाव और विस्तार ग्रीष्म मानसून को रोकते हैं।
• वे शीत साइबेरियाई वायु धाराओ को भारत में प्रवेश करने से भी रोकते हैं। |
| कृषि महत्व | • हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों में भारी मात्रा में गाद (जलोढ़) आती है, जो लगातार मैदानी क्षेत्रों को समृद्ध बनाती है जिससे भारत के सबसे उपजाऊ कृषि मैदानों का निर्माण होता है। इन्हें उत्तरी मैदानों के रूप में जाना जाता है। |
| सामरिक महत्व | • हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सदियों से एक प्राकृतिक रक्षात्मक ढ़ाल के रूप में खड़ा है। |
| आर्थिक महत्व | • हिमालयी नदियों की विशाल पनबिजली क्षमता।
• हिमालय में समृद्ध शंकुधारी और सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो उद्योगों के लिए ईंधन और लकड़ी की एक विशाल विविधता प्रदान करते हैं। • इनमें विभिन्न प्रकार की हिमालयन जड़ी बूटी और औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। |
| पर्यटन महत्व | • प्रमुख प्राकृतिक दृश्यों और हिल स्टेशनों का संकलन है।
• श्रीनगर, डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, मिरिक, गंगटोक आदि हिमालय के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं। इन जगहों पर कई हिंदू और बौद्ध मंदिर भी हैं। |
| पर्यावरण महत्व | • इनमें बृहत् पारिस्थितिक जैव विविधता पाई जाती है और भारत के चार हॉटस्पॉट ज़ोन में से एक हैं । |

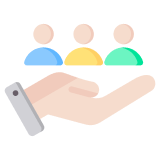 GS Foundation
GS Foundation Crash Course
Crash Course Combo
Combo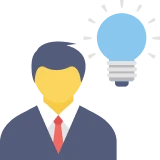 Optional Courses
Optional Courses Degree Program
Degree Program