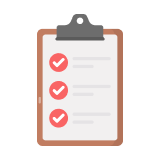राज्य विधानमंडल: भाग VI- अनुच्छेद168 से 212 (उड़ान) # |
| राज्य विधानमंडल का गठन: |
- राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एकरूपता नहीं है।
- केवल 6 राज्यों के विधानमंडल में दो सदन हैं,ये राज्य हैं- आंध्र प्रदेश ,तेलंगाना ,उत्तर प्रदेश ,बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक।
- राज्य विधानमंडल का गठन राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर होता है, और जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां, विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं।
अनुच्छेद 169: संसद एक विधान परिषद को (यदि यह पहले से है) विघटित कर सकती है और इसका गठन भी कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा और सामान्य विधान की तरह (अर्थात साधारण बहुमत से) पारित किया जाएगा।
| विधानसभा का गठन | |
|
संख्या |
• विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
• इसकी अधिकतम संख्या 500 और निम्नतम संख्या 60 तय की गई है। • अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में यह संख्या 30 तय की गई है। • मिजोरम– 40 व नागालैंड-46 • सिक्किम और नागालैंड के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। • Note: सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सिक्किम और नागालैंड को छोड़ कर। |
| नामित सदस्य |
|
| क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र |
|
| प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण |
|
|
अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण |
Note: अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण केवल लोकसभा और राज्य विधानसभा में है, राज्यसभा और राज्यविधान परिषद में नहीं। |
|
कार्यकाल |
|
| विधान परिषद का गठन | |
| संख्या | o विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की एक तिहाई निर्धारित की गई है।
o जिसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 निश्चित की गई है। o सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। o यद्यपि संविधान ने परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या तय कर दी है, परंतु इसकी वास्तविक संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। |
|
निर्वाचन के सिद्धांत |
विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/ 6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है।
• 1/ 3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे– नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। • 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। • 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे, 3 वर्षों की स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले मतदाता निर्वाचित करते हैं। • 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं लेकिन यह अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। • 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें– साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव हो। • राज्यपाल द्वारा नामित किए गए सदस्यों के अलावा,सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। |
| कार्यकाल | • विधानपरिषद एक सतत् सदन है अर्थात स्थाई अंग जो विघटित नहीं होता है।
• लेकिन इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। • सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्चुनाव और राज्यपाल द्वारा दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। |
| राज्य विधानमंडल की सदस्यता |
|
अर्हताएं |
विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए संविधान में उल्लिखित किसी व्यक्ति की अर्हताएं निम्नलिखित हैं:
|
| जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम1951 के तहत संसद ने निम्नलिखित अतिरिक्त अहर्ताओं का निर्धारण किया है:
• विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचन होने की अर्हता रखता हो और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। • विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। • अनुसूचित जाति /जनजाति का सदस्य होना चाहिए यदि वह अनुसूचित जाति /जनजाति की सीट के लिए चुनाव लड़ता है। यद्यपि अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य उस सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित न हो। |
|
|
निरर्हताएं |
संविधान के अनुसार:
• यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर है। • यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। • यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो। • यदि वह भारत का नागरिक न हो या उसने विदेश में कहीं स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित कर ली हो। • यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित कर दिया जाता है। Note:उपरोक्त निरर्हताओं के संबंध में किसी सदस्य के प्रति यदि प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि इस मामले में वह चुनाव आयोग की सलाह लेकर काम करता है। |
| दल–बदल के आधार पर निरर्हता | • संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत निरर्हता घोषित किया गया है।
• Note: संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत यदि निरर्हता का मामला उठे तो विधानपरिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष (राज्यपाल नहीं) फैसला करेगा। • किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू मामला में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति /अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। |
| शपथ या प्रतिज्ञान | 1. विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा।
2. बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य सदन में न तो मत दे सकता है और न ही कार्यवाही में भाग ले सकता है। |
|
स्थानों का रिक्त होना |
o दोहरी सदस्यता: एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबधों के तहत एक सदन से उसकी सीट रिक्त हो जाएगी।
o निरर्हता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत या संविधान के तहत या संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत। o त्यागपत्र कोई सदस्य अपना लिखित इस्तीफा विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष को दे सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। o अनुपस्थिति यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। o अन्य मामले: किसी सदस्य का पद रिक्त हो सकता है; यदि न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया जाए, यदि उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाए, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए और यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित हो जाए। |
| विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी : |
- विधानसभा: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति का पैनल।
- विधानपरिषद: सभापति, उपसभापति और उपसभाध्यक्ष का पैनल।
| विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। सामान्यतः विधान सभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है। अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। हालांकि वह निम्नलिखित तीन मामलों में अपना पद रिक्त करता है (दोनों पर लागू):
- यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्यागपत्र दे या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को लिखित में अपना त्यागपत्र दे।
- यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है।
|
अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां
|
o कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखता है।
o भारत के संविधान का, सभा के नियमों एवं कार्य संचालन की कार्यवाही में, असेंबली में इसकी पूर्व परंपराओं का, और उसके उपबंधों का अंतिम व्याख्याकर्ता है। o कोरम की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। o प्रथम मामले में वह मत नहीं देता लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। o सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान कर सकता है। o वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। o दसवीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निरर्हता को लेकर उठे किसी विवाद पर फैसला देता है। o वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है वह स्वयं कार्यमंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। |
| उपाध्यक्ष | o उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को करता है यदि विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो वह उसी तरह कार्य करता है। दोनों मामलों में उसकी शक्तियां अध्यक्ष के समान रहती हैं। |
|
सभापति का पैनल: |
o विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच से सभापति पैनल का गठन करता है, उनमें से कोई भी एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही संपन्न कराता है। जब वह पीठासीन होता है तो, उस समय उसे अध्यक्ष के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। वह सभापति के नए पैनल के गठन तक कार्यरत रहता है।
o Note:यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की सीटें खाली हैं तो पैनल के सदस्य बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। उस स्थिति में सदन को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना आवश्यक होगा। |
विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा विधानपरिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता।
| विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति: |
- विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही सभापति को चुनते हैं सभापति निम्नलिखित तीन मामलों में पद छोड़ सकता है(दोनों पर लागू):
- यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए।
- यदि सभापति, उपसभापति को लिखित त्यागपत्र दे या उपसभापति, सभापति को लिखित त्यागपत्र दे।
- यदि विधान परिषद में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दें। इस तरह का प्रस्ताव 14 दिनों की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है।
- पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद के सभापति की शक्तियां एवं कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरह है हालांकि सभापति को एक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है जो अध्यक्ष को है कि अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं और उसका फैसला अंतिम होता है जबकि यह शक्ति उपसभापति/ उपाध्यक्ष को प्राप्त नहीं है।
| उपसभापति |
ही कार्यभार संभालता है। |
|
उपसभापति का पैनल: |
|
विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन-भत्ते राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता।
| राज्य विधानमंडल सत्र |
| आहूत करना |
|
| स्थगन |
|
| सत्रावसान |
|
| विघटन |
|
|
विघटन पर अधिनियमों का व्यपगमन |
|
|
|
| कोरम (गणपूर्ति) |
|
| सदन में मतदान |
|
| विधानमंडल में भाषा |
|
| मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार |
|
| विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया |
- साधारण विधेयक:
| विधेयक का प्रारंभिक सदन |
|
|
दूसरे सदन में विधेयक |
• इसे उसी रूप में (बिना संशोधन के) पारित कर दिया जाए। • कुछ संशोधनों के बाद पारित कर विचारार्थ इसे विधानसभा को भेज दिया जाए। • विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए। • इस पर कोई कार्यवाही ना की जाए और विधेयक को 3 माह के लिए लंबित रखा जाए। 1. यदि विधान परिषद बिना संशोधन के विधेयक को पारित कर दे या विधानसभा उसके संशोधनों को मान ले तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, जिसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। 2. इसके अतिरिक्त यदि विधानसभा परिषद के सुझाव को अस्वीकृत कर दे या विधान परिषद ही विधेयक को रोक दे या परिषद 3 महीने तक कोई कार्यवाही ना करें, तब विधानसभा फिर से इसे पारित कर विधान परिषद को भेज सकती है। यदि परिषद दोबारा विधेयक को अस्वीकृत कर दे या उसे उन संशोधनों के साथ पारित कर दें जो विधानसभा को अस्वीकार हो या 1 माह के भीतर पास ना करें तब इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। 3. इस तरह साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में विधानसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। विधान परिषद एक विधि को ज्यादा से ज्यादा 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए। 4. संविधान में किसी विधेयक पर असहमति होने के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं रखा गया है। |
|
राज्यपाल की स्वीकृति |
5. राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं:
1. वहां विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, 2. वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोके रखें, 3. वह सदन या सदनों के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे, और 4. वह राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख ले। 6. यदि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दें तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा, और संविधि की पुस्तक में दर्ज हो जाता है। 7. यदि राज्यपाल विधेयक को रोक लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता। 8. यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और दोबारा सदन या सदनों द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है एवं पुनः राज्यपाल के पास स्वीकृत के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह राज्यपाल के पास वैकल्पिक वीटो पावर होता है। |
|
राष्ट्रपति की स्वीकृति |
9. राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं:
• राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं; • राष्ट्रपति उसे रोक सकते हैं; तथा • विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। 10. यदि राष्ट्रपति विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो इस पर 6 माह के भीतर इस विधेयक पर पुनर्विचार आवश्यक है यदि विधेयक को उसके मूल रूप में या संशोधित कर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी दे या नहीं। |
- धन विधेयक(अनुच्छेद 198, 199):
| धन विधेयक के संबंध में:
|
|
|
प्रक्रिया:
|
• विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद एक धन विधेयक को विधान परिषद को विचारार्थ के लिए भेजा जाता है।
• विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। • वह न तो इसे अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है। • विधान परिषद केवल सिफारिश कर सकती है और 14 दिनों में विधेयक को लौटाना भी होता है। • यदि विधानसभा किसी सिफारिश को मान लेती है तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। यदि वह कोई सिफारिश नहीं मानती है तब भी इसे मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधानसभा को विधेयक ना लौटाए तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। |
| राज्यपाल की स्वीकृति | अंततः जब एक धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है तब वह इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, इसे रोक सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है लेकिन राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। |
| राष्ट्रपति की स्वीकृति | जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो इसे स्वीकृति दे देता है या इसे रोक सकता है लेकिन इसे राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। |
| विधान परिषद की स्थिति |
|
विधानसभा से समानता
|
|
|
विधानसभा से असमानता
|
|
| राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार |
- विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदनों, इसकी समितियों और इसके सदस्यों को मिलने वाले विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों का योग है।
- विशेषाधिकार इनकी कार्यवाहियों की स्वतंत्रता और प्रभाविता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं।
- यह उन व्यक्तियों को भी प्रदान किया गया है, जो राज्य विधानमंडल के सदन या इसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के लिए अधिकृत हैं।
NOTE: यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्य विधान मंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं, जो कि राज्य विधानमंडल,का अभिन्न अंग है।
|
सामूहिक विशेषाधिकार |
|
|
व्यक्तिगत विशेषाधिकार |
• उन्हें सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह छूट केवल सिविल मामले में है और आपराधिक या प्रतिबंधित निषेध मामलों में नहीं है।
• राज्य विधान मंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा किसी कार्यवाही या समिति में दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों और राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियमों और अस्थाई आदेशों के अनुरूप है। • वे न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं, जब सदन चल रहा हो, वे साक्ष्य देने या किसी मामले में बतौर गवाह उपस्थित होने से इंकार कर सकते हैं। |

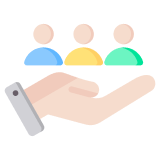 GS Foundation
GS Foundation Crash Course
Crash Course Combo
Combo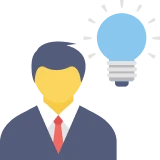 Optional Courses
Optional Courses Degree Program
Degree Program