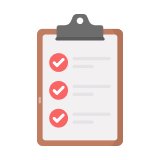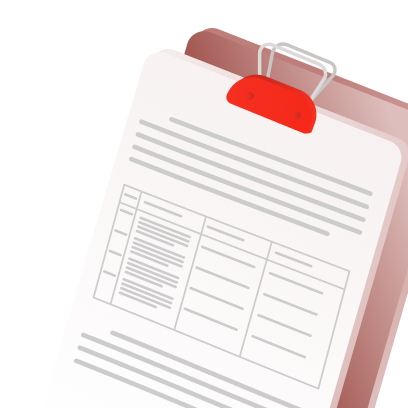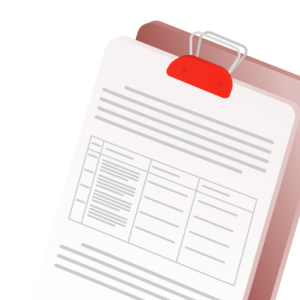भारतीय जलवायु |
भारत में स्थलाकृतिक विविधताओं (स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच) के कारण प्रादेशिक जलवायु में विविधता अत्यधिक होती है।
- भारतीय जलवायु ‘उष्ण मानसूनी’ प्रकार की है। मानसून अरबी शब्द ‘मौसिम’ से लिया गया है जिसका अर्थ ‘मौसम'(season) होता है ।
- पवन तंत्र, जो मौसम के आधार पर वायु की दिशा परिवर्तित करती है।
- विश्व में 4 प्रमुख मानसून क्षेत्र हैं:
- दक्षिण एशिया
- पूर्वी एशिया
- पश्चिम अफ्रीका
- उत्तरी ऑस्ट्रेलिया
एशिया के बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र सर्दियों के दौरान अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं और खुले समुद्री क्षेत्र में उच्च दबाव और शुष्क हवा का प्रवाह उत्पन्न करते हैं। गर्मियों के दौरान, महाद्वीप के तीव्र ताप के कारण कम दबाव उत्पन्न होता है जिससे वायुप्रवाह का उत्क्रमण होता है। समुद्र से हवा(नमी से भरी) आंतरिक हिस्सों में आती है और प्रदेशों में आगे बढ़ते हुए भारी मात्रा में वर्षा करती है
भारत, उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण देश?
कर्क रेखा के दक्षिण में देश का आधा भाग उष्णकटिबंधीय या उष्ण क्षेत्र में स्थित है और कर्क रेखा के उत्तर में दूसरा आधा भाग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है ।
- हिमालय भारत को, एशिया के बाकी हिस्सों से अलग करता है।
- उष्णकटिबंधीय मानसून यहां की जलवायु में महत्वपूर्ण है।
- हिमालय उत्तर की ठंडी शीतोष्ण वायु के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है।
इस प्रकार, हिमालय के कारण भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश है ।
प्रादेशिक विविधताएं
लेकिन हम जानते हैं कि तापमान, वर्षा आदि के कारण भारत में अत्यधिक प्रादेशिक अंतर या विविधता है ।
- तापमान में अंतर:
- गर्मियों में- पश्चिमी राजस्थान में 55 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जबकि लेह में सर्दियों के मौसम में तापमान (-45 डिग्री) सेल्सियस तक हो जाता है।
- दिसंबर की किसी रात में: द्रास (Drass) (-45 डिग्री )सेल्सियस जबकि तिरुवनंतपुरम या चेन्नई 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है।
- दैनिक तापांतर:
- रेगिस्तान की तुलना में तटीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर कम होता है।
- वर्षा के प्रकार और उसकी मात्रा के आधार पर क्षेत्रीय विविधताएं:
- हिमालय में बर्फबारी होती है जबकि देश के बाकी हिस्सों में केवल वर्षा होती है ।
- खासी(Khasi) की पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी (Cherrapunji)और मासिनराम (Mawsynram) में पूरे वर्ष में 1080 सेमी से अधिक वर्षा होती है जबकि जैसलमेर में इसी अवधि के दौरान शायद ही कभी 9 सेमी से अधिक वर्षा होती है ।
- देश के अधिकांश हिस्सों में जून-सितंबर के दौरान वर्षा होती है लेकिन तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम की शुरुआत में भी वर्षा होती है।
इन क्षेत्रीय विविधताओं के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मौसम और जलवायु में अंतर उत्पन्न होता है ।
| भारत का जलवायु कैलेंडर |
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) 4 मौसमों को मान्यता देता है:
- शीतकालीन मौसम (जनवरी-फरवरी)
- मानसून पूर्व का मौसम या ग्रीष्म ऋतु (मार्च-मई)
- दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम (जून-सितंबर)
- मानसून के निवर्तन की ऋतु (अक्टूबर-नवंबर)
| भारत की जलवायु का निर्धारण करने वाले कारक |
सामान्यतः इसे 2 भागो में विभाजित किया जाता है –
- वायुदाब और पवनों से संबंधित कारक तथा
- स्थिति और उच्चावच से संबंधित कारक
वायुदाब और पवनों से जुड़े कारक
- जेट धाराएं जो ऊपरी वायुमंडलीय परतों पर चलती हैं। निचली परतों पर इसकी कोई भूमिका नहीं होती है विशेषकर क्षोभमंडल की ऊंचाई के निकट।
- पश्चिमी जेट:
- स्टीअर्स(Steers) पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात जो भूमध्य सागर के पास बनता है। (रबी फसल के लिए उपयोगी होता है) ।
- तिब्बत के पठार में यह 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, पहली शाखा हिमालय के समानांतर चलती है।
- जब तक पश्चिमी जेट तिब्बती पठार के उत्तर में नहीं चला जाता, तब तक उत्तर भारत में निम्न दाब उत्पन्न नहीं होता है।
- पूर्वी जेट धाराएं:
- स्टीर्स उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
- वर्षा का प्रतिमान( patterns) गर्मियों में इसी पर निर्भर करता है।
- चक्रवाती विक्षोभ
- पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ भूमध्य सागर से पश्चिमी जेट धाराओं के माध्यम से आता है।
- सर्दियों के मौसम में उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय विक्षोभ (पूर्वोत्तर मानसून प्रभाव)।
- वायुदाब
- सर्दियों में
- मध्य एशिया और तिब्बत का आंतरिक भाग भारतीय उपमहाद्वीप की तुलना में उच्च दबाव वाले क्षेत्र हैं।
-
- गर्मियों में
- ITCZ उत्तरी मैदानों (20-25L) की ओर खिसकता है जो भूमध्यरेखीय या मानसून गर्त का निर्माण करता है।
- ITCZ के खिसकने के कारण तिब्बत कम दबाव वाला क्षेत्र होता है ।
- व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं और कोरिओलिस बल के कारण अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं – (इसलिए दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएँ दक्षिण पश्चिमी हो जाती है)।
- दबाव प्रणाली
- तिब्बत का पठार निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है।
- मेडागास्कर(Madagascar) के पास मस्केरेन (Mascarene )में उच्च दबाव प्रणाली विकसित होती है।
(तिब्बती निम्न दबाव + मस्केरेन उच्च दबाव = पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट)
- अलनीना और IOD (हिंद महासागर द्विध्रुव):
- अलनीना द्विध्रुव को तोड़ता है ।
- कम दाब के बजाय, एक उच्च दाब क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के पास विकसित होता है जो मस्केरेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हवा और नमी की आपूर्ति में अवरोध उत्पन्न करता है।
स्थिति और उच्चावच
- उच्चावच – अनुवात और हवा का रुख
- ऊंचाई- बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। उदाहरण के लिए, एक ही अक्षांश होने के बावजूद, आगरा में जनवरी का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि दार्जिलिंग में यह केवल 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
- अक्षांश – उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों की उपस्थित होती हैं ।
- हिमालय पर्वत: हिमालय अजेय कवच के रूप में आर्कटिक क्षेत्र की ठंडी हवाओं से रक्षा करता है और मानसून उत्पत्ति में भी प्रमुख भूमिका निभाता है (तिब्बत का पठार भी यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है)।
- समुद्र से दूरी – दक्षिण भारत में संयमित प्रभाव होता है, इसलिए यहाँ सर्दी अधिक नहीं होती है। भारत के भीतरी क्षेत्र समुद्र के संयमित प्रभाव से अत्यधिक दूर हैं जिसके कारण यहाँ जलवायु अधिक होती है ।
- भूमि और पानी का वितरण – सर्दियों में धरातल ठंढा होता है जिससे उच्च दबाव उत्पन्न होता है, जबकि गर्मियों में भूमि गर्म हो जाती है जिससे निम्न दाब उत्पन्न होता है। इस उतार-चढ़ाव के कारण मानसून में परिवर्तित होता है ।
सर्दियां |
जलवायुवीय दशाएं:
उत्तर भारत
- उत्तर भारत में इस मौसम के दौरान अत्यधिक ठंड निम्नलिखित कारणों से पड़ती है।
-
- यह क्षेत्र समुद्री संयमित प्रभाव से बहुत दूर है।
- निकटवर्ती हिमालयी श्रेणियों में बर्फबारी के कारण शीत लहर की स्थिति उत्पन्न होती है।
- पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के पश्चिमोत्तर हिस्सों में पाला और कोहरे के साथ शीत लहर चलती है।
प्रायद्वीपीय क्षेत्र
- कोई भी परिभाषित ठंड का मौसम नहीं है।
- तटीय क्षेत्रों में तापमान के वितरण पैटर्न के कारण शायद ही कोई मौसमिक परिवर्तन होता हो:
- समुद्र का मध्यस्थता प्रभाव
- भूमध्य रेखा से निकटता।
सतही दाब और हवाएं
- भारत के मौसम की स्थिति आम तौर पर मध्य और पश्चिमी एशिया में होने वाले दाब के वितरण से प्रभावित होती है।
- सर्दियों के दौरान हिमालय के उत्तरी क्षेत्रों में उच्च दाब उत्पन्न होता है।
- उच्च दाब के कारण पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप की ओर उत्तर से निम्न स्तर पर हवा का प्रवाह होता है।
- मध्य एशिया में उच्च दाब केंद्र से बहने वाली सतही हवाएं शुष्क महाद्वीपीय वायु के रूप में भारत पहुंचती हैं ।
- ये महाद्वीपीय हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों से मिलती हैं ।
- इनके मिलने का क्षेत्र निश्चित नहीं होता है ,कभी-कभी, यह पूर्व में मध्य गंगा घाटी तक स्थानांतरित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरुप समूचा उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी भारत मध्य गंगा घाटी तक शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में रहता है।
जेट धाराएं और ऊपरी वायु परिसंचरण
- ऊपर चर्चा की गई थी कि वायु परिसंचरण केवल पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडल के निचले स्तर पर देखा जाता है।
- पृथ्वी की सतह से लगभग 3 किमी ऊपर निचले क्षोभ मंडल में उच्च वायु परिसंचरण का एक अलग पैटर्न देखा जाता है।
- पृथ्वी की सतह के करीब वायुमंडलीय दाब में भिन्नता ऊपरी वायु परिसंचरण के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाती है।
- पश्चिम से पूर्व की ओर 9-13 किमी की ऊँचाई के साथ पश्चिमी और मध्य एशिया के सभी क्षेत्र पछुआ पवनों के प्रभाव में रहते हैं।
- ये हवाएँ हिमालय के उत्तरी अक्षांश पर एशियाई महाद्वीप के पार, लगभग तिब्बती उच्चभूमि के समानांतर बहती हैं। इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा के नाम से जाना जाता है।
- तिब्बती उच्चभूमि इन जेट धाराओं के बहाव में अवरोध उत्पन्न करते हैं। परिणामस्वरूप जेट धाराएं दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। जिसका एक भाग तिब्बती उच्चभूमि के उत्तर में चलती है, जबकि दूसरा भाग( दक्षिणी भाग) हिमालय के दक्षिण में पूर्व दिशा की ओर चलती है।
- फरवरी में इसका 25 ° N पर औसत 200-300 mb के स्तर पर होता है। यह माना जाता है कि जेट धाराओं की यह दक्षिणी शाखा भारत में सर्दियों के मौसम में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
पश्चिमी विक्षोभ (WDs)
- पश्चिमी विक्षोभ (डब्ल्यूडी) शब्द को भारतीय मौसम विज्ञानियों ने पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ने वाली पवन प्रणालियों का वर्णन करने के लिए बनाया था ।
- पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर में असमान या असाधारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में उत्पन्न होता है। ये धीरे-धीरे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए मध्य-पूर्व में जाते हैं और भारतीय उप-महाद्वीप में प्रवेश करते है।
- हालांकि पश्चिमी विक्षोभ पूरे वर्ष भारतीय क्षेत्र में होते है, लेकिन ये जनवरी और फरवरी की सर्दियों के महीनों के दौरान अपने उच्चतम बिंदु को प्राप्त करते हैं । भारत में मानसून के दौरान इनका प्रभाव कम होता है।
प्रेरित प्रणालियां और उनका प्रभाव क्या है?
प्रेरित प्रणालियां प्राथमिक पश्चिमी विक्षोभ द्वारा प्रेरित कम दबाव वाले द्वितीय क्षेत्र या चक्रवाती परिसंचरण होते हैं। आम तौर पर ये मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पश्चिम राजस्थान क्षेत्र में देखे जाते हैं, जो धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है। इनके कारण तापमान में वृद्धि, सतह के दबाव मे कमी, उच्च, मध्यम और निम्न बादलों की उपस्थिति देखी जाती हैं। सामान्य दाब और पवन प्रणाली, विक्षोभ समाप्त होने के बाद अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाते हैं।
कृषि पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव
- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित उत्तर-पश्चिम भारत में गैर-मानसूनी महीनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ अपने प्रमुख प्रणालियों के साथ मिलकर वर्षा प्रणाली बनाते हैं।
- उनका प्रभाव कुछ समय बाद गंगा के मैदानों और पूर्वोत्तर भारत तक फैल जाता है ।
- पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च क्षेत्रों में बर्फ-बारी भी होती है।
- पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में मानसून पूर्व वर्षा कराता है जो उत्तरी उपमहाद्वीप में रबी की फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है ।
- यह देखते हुए कि गेहूं सबसे महत्वपूर्ण रबी फसलों में से एक है, जो इस क्षेत्र के लोगों के प्रमुख आहारों में से एक है, सर्दियों की बारिश भारत की खाद्य सुरक्षा को पूरा करने में योगदान देती है।
पूर्व-मानसून मौसम / ग्रीष्म ऋतु (मार्च-मई) |
- कर्क रेखा से उत्तर की ओर सूर्य की स्थिति में बदलाव के कारण भारत में विषुव के बाद तापमान में वृद्धि होती है।
उत्तर भारत
- अप्रैल, मई और जून उत्तर भारत में गर्मियों के महीने होते हैं। मई के महीने में 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान असामान्य नहीं है।
दक्षिण भारत
- महासागरों के मध्यस्थता प्रभाव से दक्षिण भारत में 26 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहता है ।
- तट से आंतरिक क्षेत्रों की ओर तापमान बढ़ता जाता है।
- ऊंचाई के कारण पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में तापमान 25 ° C से नीचे रहता है।
सतह दाब और हवाएं:-
- देश के उत्तरी हिस्से में गर्मियों के दौरान अत्यधिक गर्मी के साथ वायु दाब कम होता है ।
- तापमान अधिक होने के कारण पूरे देश में वायुमंडलीय दाब कम होता है।
- जैसे जैसे सूर्य धीरे-धीरे कर्क रेखा की ओर खिसकता जाता है। आईटीसीजेड उत्तर की ओर स्थानांतरित होने लगता है
- ITCZ का स्थान उन हवाओं के सतह परिसंचरण को आकर्षित करता है जो पश्चिम तट के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर भी दक्षिण की ओर बहती हैं । ये हवाएं पूरे उत्तरी बंगाल और बिहार में पूर्व की ओर या दक्षिण ओर बहती हैं।
- उत्तर-पश्चिमी भारत में उच्च तापमान मई और जून के महीनों में अति दाब प्रवणता बनाता है जिसके कारण गर्म धूल से भरी तेज हवाएं चलती है, जिसे ‘ लू ‘ कहते है ।
- ‘लू’ संवहनीय घटना के कारण उत्पन्न होते है और दोपहर में इनकी तीव्रता बढ़ जाती है । इन्हें स्थानीय रूप से ‘आँधी’ के नाम से जाना जाता है।
- ये अल्पकालीन होती हैं, जो रेत और धूल की एक मोटी दीवार की तरह बहती हैं ।
- पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मई के महीने में शाम को धूल भरी आंधी बहुत आम है। ये अस्थायी तूफान अत्यधिक गर्मी से आराम दिलाते हैं क्योंकि वे अपने साथ हल्की बूंदा बांदी और ठंडी हवा लाते हैं ।
मानसून के पूर्व की वर्षा:
- कभी-कभी नमी से भरी हवाएं दाब ढाल/द्रोणिका की परिधि की ओर बहती हैं।
- शुष्क और नम वायु राशियों के बीच अचानक संपर्क से तीव्र स्थानीय तूफान उत्पन्न हो जाते हैं । इस स्थानीय तूफान में अत्यधिक तीव्र हवा, मूसलाधार वर्षा और यहां तक कि ओलावृष्टि भी होती हैं ।
- छोटानागपुर पठार में उत्पन्न होने वाली बिजली और वज्रध्वनि के साथ आने वाली आंधियां , पश्चिमी हवाओं द्वारा पूर्व की ओर संचरित होती है ।
- तड़ित झंझा से होने वाली वर्षा के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और झारखंड के आसपास के इलाके आते हैं।
- पश्चिम बंगाल और असम, उड़ीसा और झारखंड के आसपास के इलाकों में तूफ़ान की दिशा मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर होती है और इसीलिए उन्हें नोर्वेस्टर कहा जाता है ।
ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान
|
दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम (जून-सितंबर) |
इस मौसम में तापमान की स्थिति
- जब सूर्य उत्तर की ओर खिसकता है तो तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, उत्तर भारत में इसके कारण हवा का परिसंचरण उपमहाद्वीप पर पूरी तरह से विपरीत हो जाता है।
- तापमान में तेजी से वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्तर-पश्चिमी मैदानों पर दाब अत्यधिक कम हो जाता है।
- लगभग 20 ° N और 25 ° N के बीच हिमालय के समानांतर, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) के रूप में जाना जाने वाली निम्न दाब की पेटी जुलाई के मध्य तक उत्तर की ओर बढ़ती है, इस स्थिति में ITCZ कभी-कभी मानसून गर्त के रूप में होता है।
- साधारणतया, कम दाब वाली मानसून गर्त दक्षिण-पूर्व में पटना और छोटानागपुर पठार के बीच उत्तर-पश्चिम में थार रेगिस्तान तक फैली हुई है । इस बीच, उच्च दाब क्षेत्र भारत के दक्षिणी समुद्र तट को बंद कर देते हैं जिससे आसपास के समुद्र धीरे-धीरे गर्म होते है।
- हवाएँ उच्च से निम्न दाब की और बहती हैं। यह उत्तर और उत्तर पूर्व में भारत की ओर दक्षिण-पश्चिमी दिशा से बहना शुरू करती है और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरिओलिस बल से ये विक्षेपित होती है । यह समुद्र से नमी को अवशोषित करती है और इस नम युक्त पवन के बहाव को दक्षिण-पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है।
जेट स्ट्रीम और ऊपरी वायु परिसंचरण
- इस समय तक, पश्चिमी जेट धाराएं भारतीय क्षेत्र से वापस चली जाती है। दरअसल, मौसम विज्ञानियों ने भूमध्य रेखा (आईटीसीजेड) के उत्तर की ओर जाने और उत्तर भारतीय मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट धाराओं की वापसी के बीच एक संबंध पाया है । आमतौर पर माना जाता है कि दोनों के बीच कारण और प्रभाव संबंध है।
- एक पूर्वी जेट धारा जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में चलती है और इसकी अधिकतम गति 90 किमी प्रति घंटे तक होती है । अगस्त में, यह 15 ° N अक्षांश तक ही सीमित रहती है, और सितंबर में 22 ° N अक्षांश तक सीमित हो जाती है । आमतौर पर पूर्वी पवनों का ऊपरी वायुमंडल में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में विस्तार नहीं होता है।
मानसून
मानसून एक ज्ञात जलवायुवीय घटना है। सदियों से बहुत सी टिप्पणियों के बावजूद मानसून वैज्ञानिकों के लिए यह पहेली बना हुआ है । मानसून की सटीक प्रकृति और कारण की खोज के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सिद्धांत मानसून को पूरी तरह से समझाने में सक्षम नहीं है। हाल ही में क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन करने के बाद इसमें सफलता प्राप्त हुई है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों के गहन अध्ययन से मानसून के मुख्य कारणों और विशेषताओं को समझने मे आसानी होती है, विशेष रूप से इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू, जैसे:
- मानसून की शुरुआत
- दक्षिण-पश्चिम मानसून को दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनो के भूमध्य रेखा को पार करने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विस्थापित होने के रूप में देखा जा सकता है।
- आईटीसीजेड की स्थिति में बदलाव का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारतीय मैदान के ऊपर पश्चिमी जेट धारा के अपनी स्थिति से वापस जाने की घटना से संबन्धित है ।
- पश्चिमी जेट धाराओं के क्षेत्र से हटने के बाद ही 15 ° N अक्षांश में पूर्वी जेट धाराएं इसका स्थान लेती है। इस पूर्वी जेट धाराओं को भारत में मानसून के तीव्रता से प्रवेश करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है ।
- दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल तट पर होता है और 10 से 13 जून के बीच मुंबई और फिर कोलकाता पहुंचता है । जुलाई के मध्य तक दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे उपमहाद्वीप को अपने अंतर्गत ले लेता है ।
- वर्षावाही तंत्र (जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात) तथा मानसून वर्षा की आवृत्ति और वितरण के बीच संबंध:-
- भारत में दो वर्षावाही तंत्र होते हैं ।
- पहली बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वर्षा का कारण बनता है।
- दूसरी दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागर धारा है जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है।
- पश्चिमी घाट के साथ अधिकांश वर्षा पर्वतीय होती है क्योंकि इससे नम हवा बाधित होती है और घाटों के साथ ऊपर उठने के लिए मजबूर होती है ।
- हालांकि, भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की तीव्रता दो कारकों से संबंधित है:
- अपतटीय मौसमी दशाएं।
- अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट धारा की स्थिति।
- बंगाल की खाड़ी से निकलने वाले उष्णकटिबंधीय अवदाबों की आवृत्ति साल दर साल बदलती रहती है ।
- भारत के ऊपर इनके रास्ते मुख्य रूप से आईटीसीजेड की स्थिति से निर्धारित होते हैं जिसे आम तौर पर मानसून द्रोणिका कहा जाता है ।
- जैसा ही मानसून द्रोणी की धुरी दोलन करती है, इन अवदाबों के रास्ते और दिशाओं में उतार-चढ़ाव होते हैं, और वर्षा की तीव्रता और मात्रा में वर्ष-दर-वर्ष उतार चढ़ाव आते है ।
- भारत के ऊपर इसके मार्ग का निर्धारण मुख्यतः ITCZ की स्थिति द्वारा होते हैं जिसे आमतौर पर मानसून द्रोणी(monsoon trough) भी कहा जाता है।
- जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है, विभिन्न वर्षो में इन अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
- जो वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है, वह पश्चिम तट पर पश्चिम से पूर्व-उत्तर-पूर्व की ओर और उतरी भारतीय मैदान और प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है।
मानसून में विच्छेद (monsoon break):-
- कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून काल के दौरान, यदि वर्षा एक या अधिक सप्ताह तक नहीं होती है तो इसे मानसून विच्छेद के रूप में जाना जाता है।
- वर्षा के मौसम में ये आर्द्र काल(dry spells)काफी आम हैं|
- विभिन्न क्षेत्रों में ये विच्छेद अलग-अलग कारणों से होते हैं:
- यदि इस क्षेत्र में मानसून द्रोणी या ITCZ के साथ वर्षा लाने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात नित्य ना हो तो उत्तर भारत में वर्षा की संभावना विफल हो सकती है
- पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती हैं।
- दक्षिण पश्चिम मानसून के गठन, शुरुआत और गहनता को प्रभावित करने वाले कारक हैं:-
दक्षिण पश्चिम मानसून का बनना:-
- अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ): गंगा के मैदान पर गर्मियों में ITCZ का स्थानांतरण उत्तरी मैदानों पर कम दाब बनाती है।
- 2. ग्रीष्म महीनों के दौरान तिब्बत के पठार का अधिक गर्म होना; -समुद्र तल से लगभग 9 किमी ऊपर तिब्बत के पठार पर मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु धाराएँ और निम्न दाब का निर्माण होता है।
- तिब्बत का पठार उच्च भूमि का एक विशाल खंड है जो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में 2-3 ° C अधिक सूर्यातप प्राप्त करता है|
- पठार वायुमंडल को दो तरह से प्रभावित करता है:
- भौतिक अवरोध के रूप में।
- उच्च स्तरीय ऊष्मा स्रोतों के रूप में।
- उपोष्णकटिबंधीय जेट प्रवाह जून के शुरुआत में पूरी तरह से भारत से वापस लौट जाता है और 40 ° N (तिब्बती पठार के उत्तर में) अक्षांश पर आ जाता है।
- पठार, जेट प्रवाह के उत्तर की ओर विस्थापन का कारण बनता है। इसलिए जून के माह में मानसून हिमालय के कारण अपने चरम पर होता है ना कि तिब्बत के क्षेत्र में कम दाब द्वारा ।
- तिब्बत का पठार दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी है, लेकिन मानसून की शुरुआत उत्तरी दिशा में प्रवास(STG) के कारण होती है।
- अक्टूबर के मध्य में यह पठार हिमालय के दक्षिण में जेट के आगे बढ़ने या इसे दो भागों में विभाजित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक बनता है।
- शीतकालीन मानसून में तिब्बत का पठार तेजी से ठंडा होता है और एक उच्च दाब क्षेत्र (तिब्बत के ऊपर चक्रवातीय स्थिति कमजोर होने लगती है तथा प्रतिचक्रवातीय स्थिति स्थापित होने लगती है) का निर्माण करता है जो उत्तर-पूर्वी मानसून को मजबूत करता है।
- तिब्बत का पठार ग्रीष्म काल में अपने आसपास के क्षेत्रों की वायु की तुलना में 2 ° C से 3 ° C तक अधिक गर्म हो जाता है।
- क्योंकि तिब्बत का पठार वायुमंडल के लिए ऊष्मा का एक स्रोत है जो वायु को ऊपर की ओर (अभिसरण) उठाता है। जिससे सतह पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बनता है।
- इसके ऊपर उठने के दौरान वायु ऊपरी क्षोभमंडल (अपसरण) में बाहर की ओर फैलती है और धीरे-धीरे हिंद महासागर के भूमध्यरेखीय भाग पर अवतलित हो जाती है।
- अंत में यह दक्षिण-पश्चिम दिशा से लौटने के दौरान भारत के पश्चिमी तट पर प्रकट होता है जिसे भूमध्यरेखीय पछुआ पवन कहा जाता है।
- यह हिंद महासागर से आर्द्रता को ग्रहण करता है एवं भारत और आसपास के देशों में वर्षा का कारण बनता है।
सतह और जल का विभेदी तापन और शीतलन:- ग्रीष्मकाल के दौरान धरातल पर निम्न दाब और समुद्र के ऊपर उच्च दाब का निर्माण होता है|
मैस्करीन तापन (Mascarene heating): दक्षिण हिंद महासागर में स्थायी उच्च दाब कोशिक
दक्षिण–पश्चिम मानसून का आगमन
- उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा (SWTJ)
मानसून के अचानक प्रस्फोट और विच्छेद के लिए जिम्मेदार।
- उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा:-
- लंबे समय तक तिब्बत के ऊपर वायु का उच्च ग्रीष्मकालीन ताप ,पूर्वी जेट को सशक्त बनाता है। भारत में भारी वर्षा तब होती है जब ये जेट धाराएँ समुद्र के ऊपर (आर्द्रता ग्रहण करने के कारण) से गुजरते समय दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं।
- यदि तिब्बत का पठार भारत में वर्षा की घटना में बाधा उत्पन्न नहीं करता तो पूर्वी जेट अस्तित्व में नहीं आता।
- तिब्बत के पठार के ऊपर जब किसी वर्ष में अत्यधिक हिमपात होता है तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून अगला वर्ष कमजोर होता है |
सोमालिया जेट(फाइंडलेटर जेट):-
- केन्या, सोमालिया और साहेल क्षेत्र को पार करने वाले सोमाली जेट के जुड़ाव से भारत की ओर दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति बहुत अधिक हो जाती है।
- यह मेडागास्कर के निकट स्थायी उच्च दाब को मजबूत करता है और दक्षिण-पश्चिम मानसून को अधिक गति और गहनता से भारत में प्रवेश करने हेतु मदद करता है।
| दक्षिण पश्चिम मानसून की गहनता |
हिंद महासागर द्विध्रुवीय (IOD) को दो क्षेत्रों ( ध्रुवों या द्विध्रुवीय) के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर से परिभाषित किया जाता है -अरब सागर में ‘पश्चिमी ध्रुव’ (पश्चिमी हिंद महासागर) और इंडोनेशिया के दक्षिण में पूर्वी हिंद महासागर में ‘पूर्वी ध्रुव’।
- यह एक एसएसटी (SST) विसंगति (समुद्र की सतह के तापमान में विसंगति) है जो उत्तरी या भूमध्यरेखीय हिंद महासागरीय क्षेत्र (IOR) में कभी-कभी घटित होती है।
- IOD अप्रैल से मई तक हिंद महासागर के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में विकसित होता है जो अक्टूबर में चरम पर पहुंच जाता है।
- एक सकारात्मक आईओडी के साथ, हिंद महासागर क्षेत्र पर पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर (बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर) चलती है। जिसके परिणामस्वरूप अरब सागर बहुत गर्म (अफ्रीकी तट के पास पश्चिमी हिंद महासागर) और पूर्वी हिंद महासागर अधिक ठंडा एवं आर्द्र (इंडोनेशिया के आसपास) होता है। नकारात्मक आईओडी के वर्ष में यह उल्टा होता है जिससे इंडोनेशिया बहुत अधिक गर्म और वर्षा वाला क्षेत्र बन जाता है।
- सकारात्मक आईओडी गर्म जल के अधिक वाष्पीकरण के कारण भारतीय मानसून के लिए उचित सिद्ध होता है।
यह अफ्रीकी तट के समीप भूमध्य सागर के पश्चिमी भाग में बादलों के बनने और वर्षा को प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है जबकि सुमात्रा के पास ऐसी गतिविधियां को यह बाधित करता है।
- दाब की स्थिति में परिवर्तन भी ENSO से प्रभावित होता हैं।
- एल-निनो शब्द का अर्थ है ‘चाइल्ड क्राइस्ट’ क्योंकि यह धारा दिसंबर में क्रिसमस के आसपास दिखाई देता है। पेरू (दक्षिणी गोलार्ध) में दिसंबर एक ग्रीष्म ऋतु का महीना है।
- यह एक जटिल मौसमिक तंत्र है जो प्रत्येक तीन से सात वर्ष में एक बार प्रकट होता है।
- यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य मौसम की चरम अवस्थाएं उत्पन्न करता है।
- इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में, पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है और भारत सहित बहुत से स्थानों के मौसम को प्रभावित करता है।
- एल-नीनो भूमध्यरेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थाई रूप से ठंडी पेरूवियन अथवा हंबोल्ट धारा (अपनी एटलस में इन धाराओं की स्थिति ज्ञात कीजिए) द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है।
- यह धारा पेरू के तट के जल के तापमान को 10°C तक बढ़ा देती है। जिसके निम्नलिखित परिणाम होते है:
- भूमध्यरेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति|
- समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता।
- प्लवक की मात्रा में कमी जो समुद्र में मछलियों की संख्या को और कम कर देती है।
- एल-नीनो का उपयोग भारत में मानसून वर्षा के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। 1990-91 में, एक प्रचंड एल-नीनो घटना घटित हुई थी जिसके कारण देश के अधिकांश हिस्सों में पांच से बारह दिनों तक दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन में देरी हुई थी।
भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून का आगमन और प्रगति
अरब सागर की शाखा:
अरब सागर में उत्पन्न मानसूनी पवनें आगे चलकर तीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं:
इसकी एक शाखा पश्चिमी घाट द्वारा अवरुद्ध की जाती है।
- पवनें पश्चिमी घाट की ढलान पर चढ़ती हैं और सह्याद्री के पवनाभिमुखी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान में पर्वतीय वर्षा का कारण बनती हैं।
- पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है। इससे पवनों की आर्द्रता में कमी आती है। परिणामस्वरूप, ये पवनें पश्चिमी घाट के पूर्व में कम वर्षा का कारण बनती हैं। कम वर्षा वाले इस क्षेत्र को वृष्टि-छाया क्षेत्र के रूप मे जाना जाता है।
- अरब सागर मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तरी तट से टकराती है, तथा ये पवनें नर्मदा और तापी नदी की घाटियों से होकर मध्य भारत के दूरवर्ती क्षेत्रों में वर्षा का कारण बनती हैं। छोटानागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद, वे गंगा के मैदानों में प्रवेश करती हैं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है।
- इस मानसूनी पवन की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। इसके बाद, यह बहुत कम वर्षा के साथ आगे पश्चिम राजस्थान और अरावली की ओर बढ़ती है। पंजाब और हरियाणा में, यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा से मिल जाती है। यह दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा का कारण बनती है।
- राजस्थान से होकर गुजरने वाली शाखा में वर्षा को प्रभावित करने की क्षमता कम नहीं होती है क्योंकि:
- अरावली की दिशा इन मानसूनी हवाओं के समानांतर है।
- पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र की शुष्क और गर्म हवाएँ इन मानसूनी हवाओं की सापेक्ष आर्द्रता को कम करती हैं और उन्हें घनीकृत नहीं होने देती हैं।
बंगाल की खाड़ी की शाखा:
- बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार के तट और दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश के छोटे से हिस्सों से टकराती है। किंतु म्यांमार के तट पर स्थित आराकान पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं।इसलिए, मानसून दक्षिण-पश्चिम दिशा के बजाय दक्षिण व दक्षिण-पूर्व से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवेश करती है।यहाँ से, यह शाखा हिमालय और उत्तर-पश्चिम भारत में तापीय निम्न दाब के प्रभाव के कारण दो भागो में विभाजित हो जाती है।
- इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ-साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है।
- इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है जहां यह शाखा विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करते हैं।
- इसकी एक उप-शाखा मेघालय की गारो और खासी पहाड़ियों से टकराती है। जिससे निकटवर्ती पहाड़ियों के कीपनुमा प्रभाव के कारण भारी वर्षा होती है।
- खासी पहाड़ियों की चोटी पर स्थित मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा (1141 सेमी) प्राप्त करने वाला स्थान है।
- मासिनराम की तुलना में मेघालय पठार (शिलांग और गुवाहाटी की तरह) के पवनाविमुखी ढाल पर अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है।
- उत्तर की ओर ब्रह्मपुत्र घाटी में वृष्टि छाया प्रभाव पड़ता है, लेकिन समीपवर्ती हिमालय द्वारा इसका प्रभाव कम हो जाता है, जिससे पवनें फिर से ऊपर उठने लगती हैं, जिससे भारी वर्षा की एक समानांतर पेटी विकसित होती है।
Note:
- मानसून की अरब सागर शाखा बंगाल की खाड़ी की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होती है क्योंकि:
- अरब सागर बंगाल की खाड़ी से बड़ा है।
- संपूर्ण अरब सागर भारत की ओर बढ़ता है जबकि बंगाल की खाड़ी का केवल एक हिस्सा भारत में प्रवेश करता है और शेष म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया तक जाता है।
- ये दो शाखाएँ गंगा के मैदान में एक में विलीन हो जाती हैं और जब तक यह पंजाब में पहुँचती है, तब तक नमी काफी हद तक खत्म हो चुकी होती है।
इस मौसम में तमिलनाडु तट शुष्क रहता है क्योंकि:
- तमिलनाडु तट दक्षिण-पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है।
- यह दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि-छाया क्षेत्र (पश्चिमी घाटों के) में स्थित है।
दक्षिण–पश्चिम मानसून की वापसी:
NE मानसून का आगमन और सितंबर के अंत में SW मानसून का निवर्तन एक क्रमिक घटना है।
- ये घटनाएं लगभग एक ही समय पर होती हैं।
- यह “मानसून के निवर्तन” को संदर्भित करता है।
मानसून के बाद का मौसम/शीत ऋतु (Oct–Dec) |
अक्टूबर-नवंबर के महीने में मौसम शुष्क और सर्द हो जाता है।
मानसून प्रत्यावर्तन का मौसम–
ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरण के परिणामस्वरुप, भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में न्यून दाब के क्षेत्र के कमजोर होने के कारण प्रत्यावर्तन होता है। जिसका कारण होता है:
- सूर्य का भूमध्य रेखा की ओर बढ़ना(दक्षिणायन)।
- अत्यधिक वर्षा के कारण तापमान में कमी।
इससे वायु दाब में धीरे-धीरे कमी आती है जिसके कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून पीछे लौटने लगता है। दाब के इस क्रमिक कमी के कारण, मॉनसून प्रक्रिया का पीछे हटना इसके आगमन की तुलना में बहुत धीमी प्रक्रिया है।
निर्वतन का चरण (Oct- Nov)
- दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर-पश्चिम भारत में पाकिस्तान की सीमा से सितंबर के पहले सप्ताह में पीछे हटना प्रारंभ कर देता है।इसलिए ये पवनें उन क्षेत्रों से सबसे पहले लौटती हैं जहां वे आखिरी में पहुंचती है।
- मानसून सितंबर के पहले सप्ताह तक पश्चिमी राजस्थान से लौटता है।
- यह महीने के अंत तक राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा के मैदान और मध्यवर्ती उच्चभूमि से वापस लौट चुकी होती है।
- अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में आ जाता है और नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है।
- दिसंबर के मध्य तक प्रायद्वीप से, निम्न वायुदाब का केंद्र ,पूरी तरह से हट चुका होता है।
इस मौसम के दैरान तापमान की स्थिति:
- मानसून के निवर्तन के साथ मेघ विलुप्त हो जाते हैं, और आसमान साफ हो जाता है और तापमान में वृद्धि होने लगती है।
- मेघ आवरण में कमी के कारण दैनिक तापांतर बढ़ जाता है।
- उच्च तापमान (लगभग 25°C) की स्थिति और आमतौर पर ‘अक्टूबर हीट’ या क्वार की उमस ’के रूप में संदर्भित आर्द्रता के कारण मौसम असहनीय हो जाता है।
| S.No | S.W. मानसून | एन.ई. मानसून |
| 1. | वे जून से सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तक उड़ते हैं। | वे दिसंबर के महीने से उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम में उड़ते हैं, जनवरी और फरवरी। |
| 2. | ये तटवर्ती आर्द्र हवाएँ हैं क्योंकि वे समुद्र से भूमि पर उड़ती हैं। ये गर्म हवाएं हैं जैसे वे आते हैं | ये अपतटीय शुष्क हवाएँ हैं, क्योंकि ये भूमि से समुद्र तक उड़ती हैं। |
| 2. | भूमध्य रेखा के पास निचले अक्षांशों से। | वे बल्कि शांत हवाएं हैं। |
| 3. | इन गर्म और आर्द्र हवाओं के कारण व्यापक वर्षा होती है। | ये ठंडी और शुष्क अपतटीय हवाएं भारत को कोरोमंडल तट के अलावा कोई बारिश नहीं देती हैं। |
| 4. | इन हवाओं को उनकी योनि या अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। | वे योनि से पीड़ित नहीं हैं। |
सतही पवनें और वर्षण:
- जैसे-जैसे मानसून का निवर्तन होता है, मानसून द्रोणी कमजोर होती जाती है और धीरे-धीरे दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून के विपरीत उत्तरी मानसून की शुरुआत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है।
- देश के बड़े हिस्से पर पवनों की दिशा स्थानीय दाब की स्थितियों से प्रभावित होती है।
- पवनें गंगा घाटी के उत्तर पश्चिम में नीचे की ओर, गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा में उत्तरी और बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर-पूर्व में (इस प्रकार उत्तर-पूर्व मानसून नाम) चलती हैं।
- ये शीतकालीन मानसूनी वर्षा का कारण नहीं बनते हैं क्योंकि वे धरातल से समुद्र की ओर चलते हैं। जिसके निम्नलिखित कारण है:
- उनमें थोड़ी आर्द्रता होती है।
- धरातल पर प्रतिचक्रवातीय परिसंचरण के कारण वर्षा की संभावना कम हो जाती है।
- अपवाद: तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा, जिसका कारण उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों का लौटते समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए आर्द्रता ग्रहण करना होता है|

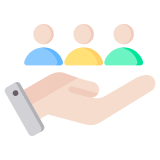 GS Foundation
GS Foundation Optional Course
Optional Course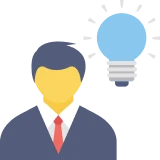 Combo Courses
Combo Courses Degree Program
Degree Program