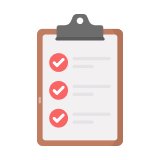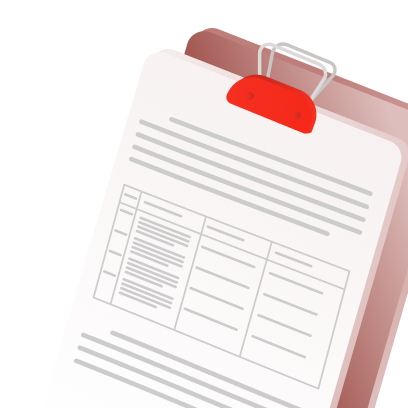स्थानीय स्वशासन: पंचायत और नगरपालिकाएँ (उड़ान) |
- संवैधानिक स्थिति: 73 वां और 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था।
- स्थानीय स्वशासन, सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है।
- अनुच्छेद 40 –“राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों|”
- राजस्थान पंचायती राज प्रणाली की स्थापना करने वाला पहला राज्य था। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में किया था।
- शहरी स्थानीय शासन की देखरेख : – आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय + रक्षा मंत्रालय + गृह मंत्रालय।
| पंचायती राज का विकास: |
| वर्ष | समिति | अनुशंसाएं |
| 1957 | बलवंत राय मेहता समिति: सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। |
|
| 1977 | अशोक मेहता समिति (पंचायती राज संस्थाओं पर गठित समिति) |
|
| 1978 | दंतेवाला समिति: |
|
| 1984 | हनुमान राव समिति | • जिला योजना पर जोर दिया | |
| 1985 | जी.वी.के.राव समिति: ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा करना। |
|
| 1986 | एल.एम. सिंघवी समिति: लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना।
|
इस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विकास प्रक्रिया को धीरे–धीरे नौकरशाही और पंचायती राज से अलग कर दिया जाना चाहिए इसलिए पीआरआई को ‘बिना जड़ों वाली घास‘ कहा गया। |
| 1988 | पी. के. थुंगन समिति: |
|
| 1988 | गाडगिल समिति: नीति और कार्यक्रमों पर समिति। |
|
| नगर निकायों का विकास: |
| 1687 | भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। |
| 1726 | बंबई और कलकत्ता नगर निगम |
| 1870 | वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प |
| 1882 | लॉर्ड रिपन संकल्प –स्थानीय स्वशासन का मैग्नाकार्टा |
| 1907 | विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन |
| 1919 | भारत सरकार अधिनियम, 1919 के द्वारा, स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय बना दिया गया। |
| 1924 | छावनी( Cantonment) अधिनियम |
| 1935 | भारत सरकार अधिनियम,1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। |
| पंचायत ( 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992) |
|
संवैधानिक प्रावधान: |
o 243G –पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व o 243H –पंचायतों की करारोपण की शक्ति o 243 I– वित्त आयोग |
| ग्राम सभा: | प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक + गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं + कार्यों का निर्धारण राज्य विधायिका द्वारा किया जाता है। |
|
त्रि–स्तरीय पंचायत प्रणाली:
|
• पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में समरूपता लाना।
• ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायत का गठन। • 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकते हैं। • तीनों स्तरों पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाएंगे| • अध्यक्ष: इनका चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। · सभी तीन स्तरों पर आरक्षण – अनुसूचित जाति / जनजाति (जनसंख्या के आधार पर) के लिए सीटों का आरक्षण+ महिलाओं (एक तिहाई आरक्षण) के लिए आरक्षण। • अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। • कार्यकाल: पांच वर्ष • एक पंचायत जो समय पूर्व भंग होने पर पुनर्गठित हुई है वह पूरे 5 वर्ष की निर्धारित अवधि तक कार्यरत नहीं होती, बल्कि केवल बचे हुए समय के लिए ही कार्यरत होती है।
|
|
अनर्हताएं: |
कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा यदि वह निम्न प्रकार से अनर्हत होगा :
1. राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के उद्देश्य से संबंधित राज्य में उस समय प्रभावी कानून के अंतर्गत, अथवा 2. राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत 3. लेकिन किसी भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वे 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। |
| राज्य चुनाव आयोग
(अनुच्छेद –243 K):
|
• पंचायत स्तर के सभी चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है।
• राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी। • राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुकसान हो| |
| शक्तियां, कार्य और वित्त संबंधित मामलों का राज्य द्वारा निर्धारण | • ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 मामलों को पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है।
• आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन करना। • वित्त: राज्य विधानमंडल पंचायतों को उपयुक्त कर लगाने के लिए अधिकृत कर सकती है, राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित कर पंचायतों को सौंप सकती है तथा राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता दे सकती है। |
|
राज्य वित्त आयोग
|
• राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है।
• संरचना + योग्यता: राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित किया जाता है। • केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में पंचायतों के पूरक स्रोतों में वृद्धि के लिए राज्य की समेकित निधि में आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देगा| |
|
अन्य प्रावधान |
• लेखा परीक्षण: राज्य विधायिका निर्धारित करती है।
• अनर्हत याचिकाएँ: राज्य विधायिका निर्धारित करती है। • संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना : राष्ट्रपति अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए निर्देश दे सकता है। • छूट प्राप्त राज्य व क्षेत्र – नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और कुछ अन्य (मणिपुर और दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र) विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। |
|
1996 का पेसा (PESA) अधिनियम:
|
• पांचवीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में भाग-9 के प्रावधान लागू नहीं होते। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है।
• पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप स्वशासन प्रदान करना। |
| नगर निगम ( 74वां संविधान संशोधन, 1992) |
|
संवैधानिक प्रावधान: |
o 243 W– नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं दायित्व। o 243 X– नगर पालिका द्वारा करारोपण की शक्तियां तथा निधि इत्यादि। o 243 Y– वित्त आयोग o 243 Z– जिला योजना समिति o 243 ZE– महानगरीय आयोजना के लिए समिति। |
|
तीन प्रकार की नगरपालिकाएं:
|
1. नगर पंचायत (ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन)
2. नगर पालिका परिषद (छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए) 3. नगरपालिका निगम (बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए) वार्ड समिति: तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति गठित होगी। |
|
चुनाव:
|
|
|
कार्य:
|
|
|
नगर पालिका के प्रकार:
|
|
| जिला योजना समिति (DPC): |
- राज्य विधायिका इसके चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित करती है।
- अनुच्छेद 243ZD: पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी।
- जिला योजना समिति के 4/5 भाग सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे।
- 1 / 5 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।
- समिति के सदस्यों की संख्या जिले की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए।
| महानगरीय योजना समिति (243ZE): |
- महानगरीय क्षेत्र – देश का वह क्षेत्र, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है (अनुच्छेद 243P)।
- एक मसौदा विकास योजना तैयार करना।
- महानगरीय योजना समिति के 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों तथा पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा स्वंय में से चुने जाएंगे।
- 1 / 3 सदस्य नामांकित किए जाएंगे।
- निर्वाचित सदस्य ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में होने चाहिए।
| स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद : |
- इसकी स्थापना 1954 में,राष्ट्रपति के आदेश से भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 (अंतर–राज्य परिषद) के अंतर्गत राष्ट्रपति के एक सलाहकार निकाय के रूप में गठित किया गया था।
- अध्यक्ष – केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ।
- रचना–इसमें भारत सरकार के नगर विकास मंत्री और राज्यों के स्थानीय स्वशासन के प्रभारी मंत्री सम्मिलित होते हैं।

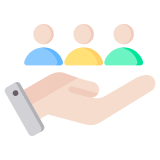 GS Foundation
GS Foundation Optional Course
Optional Course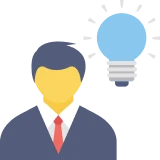 Combo Courses
Combo Courses Degree Program
Degree Program