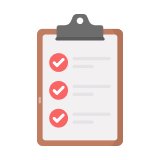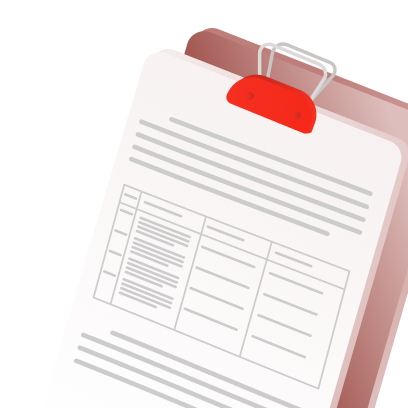भारतीय मौसम– ऋतु |
| परिचय: |
- जलवायु मानवजाति के भौतिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह वायुमंडलीय परिस्थितियों का समुच्चय है जिसमें गर्मी, नमी और वायु संचलन शामिल है।
- भारत जैसे विकासशील देश में जलवायु विशेषताओं का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है, इससे जीवन यापन का तरीका, रहने का तरीका, खाद्य प्राथमिकताएं, वेशभूषा और यहां तक कि लोगों की व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं।
- भारत में बहुत सारे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के बावजूद कृषि गतिविधियों को सफल बनाने के लिए हमारी मानसूनी वर्षा पर निर्भरता कम नहीं हुई है।
- भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून वर्ग ’से संबंधित है, जो उष्णकटिबंधीय बेल्ट और मानसूनी हवाओं में अपने प्रभाव को दर्शाता है।
- .हालाँकि देश का एक बड़ा हिस्सा कर्क रेखा के उत्तर स्थित है, जो कि उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरे होने के कारण भारत की जलवायु विशिष्ट है।
| मौसम वातावरण की क्षणिक स्थिति है जबकि जलवायु , मौसम की औसत से अधिक समय तक की स्थिति को संदर्भित करता है। मौसम में तेज़ी से बदलाव होता है और यह एक दिन या सप्ताह के भीतर हो सकता है लेकिन जलवायु में परिवर्तन 50 साल या उससे भी अधिक समय के बाद हो सकता है। |
| जलवायु | मौसम |
| जलवायु एक स्थान का मौसम है जो औसतन 30 वर्षों की होती है।
|
.यह वातावरण में हर दिन होने वाली घटनाओं का मिश्रण है (पृथ्वी पर एक वातावरण है लेकिन विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग मौसम है)। |
| यह बताता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम कैसा रहता है। | यह अल्पकालिक मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है |
| जलवायुविज्ञान | मौसम-विज्ञान |
नोट – NCERT में 50 वर्ष का उल्लेख है लेकिन WMO के अनुसार यह 30 वर्ष है।
भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताएं |
- हवाओं का दिशा परिवर्तन – भारतीय जलवायु एक वर्ष में मौसम के परिवर्तन के साथ पवन प्रणाली के पूर्ण दिशा परिवर्तन की विशेषता है। सर्दियों के मौसम के दौरान आम तौर पर व्यापारिक हवाओं की दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर चलती हैं। ये हवाएँ शुष्क ,नमी से रहित ,और देश भर में कम तापमान और उच्च दबाव स्थिति गुणों वाली होती है है। गर्मियों के मौसम के दौरान हवाओं की दिशा में पूर्ण दिशा परिवर्तन पाया जाता है और ये मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम से लेकर उत्तर-पूर्व तक चलती हैं।
- भूमि पर वैकल्पिक रूप से उच्च और निम्न दबाव क्षेत्रों का गठन – मौसम के परिवर्तन के साथ वायुमंडलीय दाब में बदलाव होता है। कम तापमान की स्थिति के कारण सर्दियों के मौसम में देश के उत्तरी भाग में उच्च दबाव वाले क्षेत्र बनते हैं। दूसरी ओर गर्मी के मौसम में भूमि के तीव्र ताप से देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में एक ऊष्मीय प्रेरित निम्न दाब केंद्र का निर्माण होता है। ये दाब क्षेत्र हवा की दिशा और तीव्रता को नियंत्रित करते हैं।
- मौसमी और परिवर्तनशील वर्षा – भारत में 80 प्रतिशत वार्षिक वर्षा गर्मियों के उत्तरार्ध में प्राप्त होती है, जिसकी अवधि देश के विभिन्न भागों में 1-5 महीने से होती है। चूंकि वर्षा भारी आपतन के रूप में होती है, इसलिए यह बाढ़ और मिट्टी के कटाव की समस्या पैदा करती है। कभी-कभी कई दिनों तक लगातार बारिश होती है और कभी-कभी शुष्क अवधि का लंबा दौर होता है। इसी प्रकार, वर्षा के सामान्य वितरण में एक स्थानिक भिन्नता है। राजस्थान के जैसलमेर में 10 साल मैं हुई बारिश के बराबर चेरापूंजी में बारिश एक ही दिन में होती है।
- मौसमों की बहुलता – भारतीय जलवायु में लगातार बदलते मौसम की स्थिति होती है। तीन मुख्य मौसम हैं लेकिन व्यापक रूप से विचार करने पर उनकी संख्या एक वर्ष में छह हो जाती है (सर्दियों, सर्दियों की गिरावट, वसंत, गर्मी, बरसात और शरद ऋतु)।
- भारतीय जलवायु की एकता – हिमालय और उससे जुड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ भारत के उत्तर मे पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई हैं। ये लंबी पर्वत श्रृंखलाएं मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती हैं। यहां तक कि भारत के कुछ हिस्सों का विस्तार कर्क रेखा के उत्तर मे है इसीलिए यहां उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। ये पर्वतमाला मानसूनी हवाओं से भारत में वर्षा का कारण बनाती हैं और पूरा देश मानसूनी हवाओं के प्रभाव में आता है। इस तरीके से पूरे देश में जलवायु मानसूनी प्रकार की हो जाती है।
- भारतीय जलवायु की विविधता – भारतीय जलवायु की एकता के बावजूद, यह क्षेत्रीय विभिन्नता और विविधताओं में विभक्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जबकि गर्मियों में तापमान पश्चिमी राजस्थान में कभी-कभी 55 ° C को छू लेता है, यह लेह के आसपास सर्दियों में शून्य से 45 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। ये अंतर हवाओं, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और शुष्कता आदि के संदर्भ में दिखाई देते हैं। ये स्थान, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पहाड़ों से दूरी और दूसरे स्थानों पर सामान्य दशा स्थितियों के कारण होते हैं।
- प्राकृतिक आपदाओं में निरूपण- विशेष रूप से इसकी मौसम संबंधी स्थितियों के कारण भारतीय जलवायु बाढ़, सूखा, अकाल और यहां तक कि महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं मे निरूपित होती है।
भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक: |
| भारतीय जलवायु इतनी विविध और जटिल है कि यह जलवायु की चरम सीमाओं और जलवायु किस्मों को दर्शाता है। जबकि यह फसलों को उगाने के लिए पर्याप्त गर्मी प्रदान करता है और पूरे देश में कृषि गतिविधियों को करने के लिए यह उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और साथ ही शुष्क क्षेत्रों से संबंधित कई फसलों की खेती में भी मदद करता है। |
भारत की जलवायु को कई कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें मोटे तौर पर दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है –
| भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक
1. स्थान और राहत से संबंधित कारक 2. वायु दबाव और हवाओं से संबंधित कारक |
- स्थान और स्थल रूप से संबंधित कारक:
| • अक्षांश
• हिमालय पर्वत • भूमि और जल का वितरण • समुद्र से दूरियाँ • ऊपरी वायु परिसंचरण • ऊंचाई • मानसून हवाएँ • शरीर विज्ञान • उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात |
- अक्षांश – भारत की मुख्य भूमि 8 ° N से 37 ° N के बीच फैली हुई है। कर्क रेखा के दक्षिणी क्षेत्र उष्ण कटिबंध में हैं और इसलिए उच्च सौर विकिरण प्राप्त करते हैं। गर्मियों के तापमान चरम मे होते हैं और अधिकांश क्षेत्रों में सर्दियों का तापमान मध्यम होता है। दूसरी ओर उत्तरी भाग गर्म समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित हैं और तुलनात्मक रूप से कम सौर विकिरण प्राप्त करते हैं। उत्तर भारत में ग्रीष्मकाल, गर्म होता है और पश्चिमी विक्षोभ की निरंतरता और आगमन के कारण सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं। तटीय क्षेत्र में अक्षांशीय स्थिति के बावजूद मध्यम जलवायु पायी जाती हैं।
- हिमालय पर्वत – उत्तर में उदात्त हिमालय अपने विस्तार के साथ मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक प्रभावी जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। आर्कटिक वृत के पास उत्पन्न होने वाली ठंडी और सर्द हवाएं हिमालय द्वारा बाधित होती हैं और भारत की जलवायु को एक विशिष्ट अनुभूति देती हैं।
- .भूमि और जल का वितरण – भारत ,दक्षिण में तीन तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है और उत्तर में एक उच्च और निरंतर पहाड़ की दीवार से घिरा हुआ है। स्थल की तुलना में, पानी गर्म और ठंडा धीरे-धीरे होता है। स्थल भूमि और समुद्र मे तापांतर होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास विभिन्न मौसमों में अलग-अलग वायु दबाव क्षेत्र बनाता है।
- महासागरीय धारा- समुद्री क्षेत्र गर्म या ठंडे महासागरों की धाराओं से प्रभावित होते हैं। खाड़ी पावन या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जैसे महासागरीय धाराएँ अपने बंदरगाहों को बर्फ मुक्त रखते हुए पश्चिमी यूरोप के तटीय जिलों को गर्म करती हैं। एक ही अक्षांश में स्थित बंदरगाह लेकिन इनका शीत धाराओं द्वारा संचरण किया जाता है, जैसे कि उत्तर-पूर्व कनाडा के लैब्राडोर प्रवाह से यह कई महीनों जमे हुए होते हैं। शीत धाराएँ भी गर्मी के तापमान को कम करती हैं, विशेषकर जब इन्हें तट पर चलने वाली हवाओं द्वारा भूमि पर ले जाया जाता है।
- स्थानीय हवाएँ – यह हवाएँ गर्म होती हैं यानी ये गर्म क्षेत्र से उठती है, तो वे तापमान बढ़ाएंगी। अगर ठंडी जगहों से हवाएँ चली हैं, तो वे तापमान कम करेंगे। स्थानीय हवाएं जैसे फोहेन, चिनूक, सिरोको और मिस्ट्रल भी तापमान में उल्लेखनीय परिवर्तन करते हैं।
- समुद्र से दूरी(महाद्वीपीय) – एक लंबी तटरेखा वाले, बड़े तटीय क्षेत्रों में एक समान जलवायु होती है। भारत के भीतरी इलाकों के क्षेत्र समुद्र के मध्यम प्रभाव से बहुत दूर हैं। ऐसे क्षेत्रों में जलवायु उच्चतम होती है। इसीलिए, कोंकण तट के लोगों को शायद ही कभी तापमान के उच्च सीमा और जलवायु की मौसमी लय का अंदाजा होता है। दूसरी ओर, देश के अंदरूनी हिस्सों जैसे कानपुर और अमृतसर में मानसूनी विषमताएँ जीवन को पूरे क्षेत्र में प्रभावित करती हैं।
- ऊंचाई – तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। हल्की हवा के कारण, पहाड़ों पर मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक ठंड होटी हैं। उदाहरण के लिए, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन आगरा में जनवरी का तापमान 16 ° C है जबकि दार्जिलिंग में यह केवल 4 ° C है।
- प्राकृतिक भूगोल- अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा पश्चिमी घाट पर लगभग लंबवत टकराती है और पश्चिमी ढलानों पर भारी वर्षा का कारण बनती है। इसके विपरीत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के विशाल क्षेत्र पश्चिमी घाट के वर्षा-छाया क्षेत्र में स्थित है। जिससे कम वर्षा प्राप्त करते हैं राजस्थान और गुजरात में बहने वाली मॉनसूनी हवाएं अरावली के समानांतर चलती हैं और किसी भी भौगोलिक बाधा से बाधित नहीं होती हैं और इसलिए इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। मेघालय के पठार में बहुत भारी वर्षा इसके कीप और भौगोलिक उत्थान प्रभाव के कारण होती है। 1100 सेमी से अधिक औसत वार्षिक वर्षा के साथ मावसिनराम और चेरापूंजी ,पृथ्वी के सबसे नम स्थानों में जगह बनाता है।
- मानसून हवाएँ – मानसूनी हवाओं का पूर्ण परिवर्तन मौसम में अचानक परिवर्तन लाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश वर्षा इन हवाओं के कारण होती है।
| कीप प्रभाव: जब बादल पहाड़ों के बीच एक संकीर्ण क्षेत्र से गुजरता है तो इसके घनत्व में वृद्धि होती है। |
- ऊपरी वायु प्रवाह – उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा की दक्षिणी शाखा भूमध्यसागरीय क्षेत्र से भारतीय उप-महाद्वीप में पश्चिमी विचोभ लाने के लिए जिम्मेदार है। पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट धारा दक्षिण पश्चिम मानसून की शीघ्र शुरुआत होने में मदद करता है।
- उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात – उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अधिकांश उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है और तटीय मौसम को प्रभावित करती है। शीतोष्ण चक्रवात के अवशेष पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आते हैं और उत्तर भारत में मौसम को प्रभावित करते हैं।
- वायु दबाव और पवन से संबंधित कारक:
वायु दबाव और पवन प्रणाली अलग-अलग ऊंचाई पर भिन्न होती है जो भारत के स्थानीय जलवायु को प्रभावित करती है। निम्नलिखित कारकों पर विचार करें:
- दबाव और स्थलीय हवाओं का वितरण।
- ऊपरी वायु परिसंचरण और विभिन्न वायु द्रव्यमानों की गति और जेट धारा।
- .सर्दियों में विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा और दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में उष्णकटिबंधीय अवसाद।
|
भारत में मौसम |
- मौसम विज्ञानी निम्नलिखित चार मौसमों को चिन्हित करते हैं:
|
| भारत में मौसम
1. मानसून (बरसात) का मौसम
2. ठंड का मौसम 3. गर्म मौसम का मौसम |
भारतीय मौसम |
- मानसून शब्द अरबी शब्द ‘मौसिम’ से लिया गया है जिसका अर्थ ‘सीज़न’ है।
- मानसून वे मौसमी पावनी (द्वितीय पवन) हैं जो मौसम के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा परिवर्तित कर देती हैं।
- मानसून भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों आदि के लिए अनूठा हैं। वे किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक स्पष्ट हैं।
- भारत अक्टूबर से दिसंबर के दौरान उत्तर पूर्व मानसून पवन (उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर) और जून – सितंबर के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसूनी पवन (दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर) प्राप्त करता है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून तिब्बती पठार के ऊपर बने निम्न दबाव प्रणाली के कारण बनता है।
- उत्तर-पूर्व मानसून तिब्बती और साइबेरियाई पठारों पर उच्च दबाव केंद्र से संबंधित है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत के अधिकांश क्षेत्रों में तीव्र वर्षा लाता है और उत्तर-पूर्व मानसून मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी-पूर्वी तट (दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट और तमिलनाडु तट) में वर्षा लाता है।
| मानसून विशेष रूप से बड़े भूभाग के पूर्वी किनारों पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर प्रमुख है, लेकिन एशिया में, यह चीन, कोरिया और जापान में उष्णकटिबंधीय के बाहर होता है। |
भारतीय मानसून की महत्वपूर्ण विशेषताएं:
|
मानसून को प्रभावित करने वाले कारक:
- गर्मियों के महीनों के दौरान तिब्बती पठार का तीव्र ताप और सर्दियों में तिब्बती पठार और साइबेरियाई पठार पर उच्च दाब केंद्र का निर्माण होता है।
- सूरज की स्पष्ट गति के साथ अंतर उष्णकटिबंधीय आच्छादन क्षेत्र (ITCZ) का स्थानांतरण।
- दक्षिण हिंद महासागर में स्थायी उच्च दबाव केंद्र (गर्मियों में मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व में)।
- जेट धारा, विशेष रूप से उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा, सोमाली जेट धारा और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा।
- ध्रुवीय भारतीय सागर
- एल नीनो और ला नीनो
| मानसून मौसम संबंधी एक जटिल घटना है। मौसम विज्ञान के विशेषज्ञों ने मानसून की उत्पत्ति के बारे में कई अवधारणाएँ विकसित की हैं। मानसून की उत्पत्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएँ नीचे दी गई हैं। |
भारतीय मानसून की कार्यप्रणाली
- भारतीय मानसूनी कार्यप्रणाली की शुरुआत के पीछे एक जटिल प्रक्रिया है जिसे अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है।
- इस जटिल घटना को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है।
|
| भारतीय मानसून के सिद्धांत।
a क्लासिकल थ्योरी b AIR MASS थ्योरी c डायनामिक थ्योरी |
प्राचीन सिद्धांत:
- मानसूनी हवाओं का पहला वैज्ञानिक अध्ययन अरब व्यापारियों द्वारा किया गया था।
- 10 वीं शताब्दी में, एक अरब अन्वेषक, अल मसुदी ने उत्तर हिंद महासागर के ऊपर महासागरीय हवाओं और मानसूनी हवाओं के उत्क्रमण का विवरण दिया था।
- 17 वीं शताब्दी में, सर एडमंड हैली ने मानसून के बारे में विस्तार से बताया कि महाद्वीपों और महासागरों के तापांतर के कारण मानसून बनता है।
|
ग्रीष्म ऋतु:
|
|
|
शीत ऋतु:
|
|
|
सिद्धांतों के दोष:
|
|
वायु द्रव्यमान का सिद्धांत:
- यह सिद्धांत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य की मौसमी गति के कारण ITCZ के प्रवास पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार, मानसून केवल व्यापारिक हवाओं का एक परिवर्तन है।
- ग्रीष्मकाल में, ITCZ 20 ° – 25 ° N अक्षांश पर स्थानांतरित होता है और यह गंगा के मैदान में स्थित होता है। इस स्थिति में ITCZ को अक्सर “मानसून गर्त” कहा जाता है।
- अप्रैल और मई के दौरान जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, तो हिंद महासागर के उत्तर में बड़ा भूभाग तीव्रता से गर्म हो जाता है। यह उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में एक तीव्र निम्न दबाव के निर्माण का कारण बनता है। ये स्थितियाँ ITCZ स्थिति को उत्तरार्ध की ओर जाने में मदद करती हैं।
- दक्षिणी गोलार्ध मे दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं और कोरिओलिस बल के प्रभाव में उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बहने लगती हैं।
- भारतीय उप-महाद्वीप मे चलने पर इन विस्थापित व्यापारिक पवनो को दक्षिण-पश्चिम मानसून कहा जाता है।
- सर्दियों के मौसम में, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और ITCZ भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थानांतरित होता है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापार हवाएं अपने सामान्य उत्तर पूर्व दिशा में तेजी से बहती हैं
|
आंतरिक उष्णकटिबंधीय आच्छादन क्षेत्र (ITCZ) ITCZ भूमध्य रेखा पर स्थित एक कम दबाव का क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक पवन प्रवाहित होती हैं, और इसलिए, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हवा का रुख जुलाई में, ITCZ में लगभग 20 ° N-25 ° N अक्षांश (गंगा के मैदान के ऊपर) स्थित होता है, जिसे कभी-कभी मानसून गर्त भी कहा जाता है। यह मानसून गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में ताप कम करने के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के स्थानांतरण के कारण, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को 40 ° और 60 ° E अनुदैर्ध्य के बीच पार करती हैं और कोरिओलिस बल के कारण दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर बहने लगती हैं। यह दक्षिण-पश्चिम मानसून बनाता है। सर्दियों में, ITCZ दक्षिण की ओर बढ़ता है, और इसलिए उत्तर-पूर्व से दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम की ओर हवाओं का दिशा परिवर्तन होता है। उन्हें उत्तर-पूर्व मानसून कहा जाता है। |
गतिक सिद्धांत:
- यह मानसून की उत्पत्ति के बारे में नवीनतम सिद्धांत है और इसे भर में स्वीकृति अर्जित है।
- यह सिद्धांत विभिन्न कारकों को मानसून के तंत्र में शामिल करता है और भारतीय मानसून पर उनके प्रभाव की व्याख्या करता है।
- इस सिद्धांत को गतिक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह मानसून को एक गतिशील प्रणाली, आवृत्ति, तीव्रता और नियमितता के रूप में मानता है, जिसका निर्धारण कारकों के संयोजन द्वारा किया जाता है:
- . भूमि और समुद्र मे तापांतर।
- ITCZ का स्थानांतरण।
- तिब्बत पठार का ताप बढ़ना।
- जेट धाराओं (उपोष्णकटिबंधीय जेट, सोमाली जेट और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट) की भूमिका।
- द्विध्रुवीय महासागर
- एल नीनो और ला नीनो
उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा की भूमिका
- उप-ट्रॉपिकल जेटस्ट्रीम (STJ) मानसूनी हवाओं के साथ-साथ मॉनसून की त्वरित शुरुआत में बाधा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (पोलर जेट का भारतीय मानसून पर कोई प्रभाव नहीं है)
उप–उपोषण जेट धारा(STJ) का मौसमी प्रवासन
- धारा अधिक क्षेत्रीय सीमा के साथ सर्दियों में अधिक मजबूत होती हैं और वे ग्रीष्मकाल में निम्नतम की ओर अग्रसर होती हैं।
- उत्तरी सर्दियों में, STJ हिमालय के दक्षिण में बहती है, लेकिन ग्रीष्मकाल में, यह कमजोर होकर उत्तर की ओर विस्थापित होती है और हिमालय / तिब्बती पठार के उत्तरी किनारे के साथ बहती है।
- STJ का अचानक आवधिक गमन , मानसून की शुरुआत और वापसी को इंगित करता है।
शीत ऋतु में जेट धारा:
- पश्चिमी उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्दियों के दौरान बहुत तेज़ गति से STJ धारा बहती है। हालाँकि, इस जेट धारा को ऊंची हिमालयी श्रेणियों और तिब्बती पठार द्वारा दो भागो में विभाजित किया गया है:
- जेट धारा की उत्तरी शाखा तिब्बती पठार के उत्तरी किनारे के साथ बहती है।
- दक्षिणी शाखा हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में 25 ° N अक्षांश के साथ बहती है।
- जेट धारा की यह दक्षिणी शाखा भारत में सर्दियों के मौसम की स्थिति पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यह उत्तर-पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
- यह दक्षिणी शाखा उत्तर भारत के ऊपर एक उच्च दबाव क्षेत्र बनाती है जिसमें हवाएँ परिवर्तित होती हैं.
- यह उत्तर पूर्व मानसूनी हवाओं के रूप में बहने वाली उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं को मजबूत करता है।
ग्रीष्म ऋतु में जेट धारा:
- गर्मियों की शुरुआत के साथ, STJ की दक्षिणी शाखा कमजोर पड़ने लगती है। ITCZ उत्तर की ओर भी आगे बढ़ता है, जिससे STJ की दक्षिणी शाखा कमजोर हो जाती है।
- मई के अंत तक, दक्षिणी जेट नष्ट हो जाता है और तिब्बत के उत्तर की ओर मोड़ दिया जाता है और अचानक मानसून का आगमन होता है।
- जुलाई के मध्य तक, अंतर उष्णकटिबंधीय आच्छादन क्षेत्र (ITCZ) उत्तर की ओर बढ़ता है, लगभग 20 ° N और 25 ° N के बीच हिमालय के समानांतर होता है।
- इस समय तक, भारतीय क्षेत्र से पश्चिमी जेट धारा वापस आ जाती है।
- वास्तव में, मौसम विज्ञानियों ने भूमध्यरेखीय गर्त (ITCZ) की उत्तरवर्ती पारी और उत्तर भारतीय मैदान के ऊपर से जेट धारा की वापसी के बीच एक अंतर्संबंध पाया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि दोनों के बीच “कारण और प्रभाव” संबंध है।
- उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट(TEJ), STJ के उत्तर-पूर्वी प्रवास के साथ प्रायद्वीपीय भारत में आती है। गर्मियों में तिब्बती पठार पर ताप प्रेरित कम दाब के परिणामस्वरूप ऊपरी वातावरण में चक्रवाती विचलन होता है।
- ऊपरी वायुमंडल में पूर्ववर्ती हवाएँ निचले वायुमंडल की तेज़ हवाओं से संबंधित होती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाओं के रूप में तेज़ हवाएँ चलती हैं।
पश्चिमी विक्षोभ
- ये अवसाद अवशिष्ट आगामी चक्रवात हैं। जेट धारा की दक्षिणी शाखा , इन पश्चिमी अवसादों (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के संचालन के लिए जिम्मेदार है। ये अवसाद पूरब की यात्रा करते समय कैस्पियन सागर और काला सागर से नमी उठाते हैं।
- प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से अप्रैल के बीच औसतन 4 से 6 चक्रवाती धारा उत्तर-पश्चिमी भारत में पहुँचती हैं।
- इन शीतोष्ण तूफानों के आने से उत्तर-पश्चिम भारत में हवा के तापमान में भारी कमी हो जाती है।
- उत्तर-पश्चिमी मैदानों में सर्दियों की बारिश, पहाड़ी क्षेत्रों में कभी-कभी भारी बर्फबारी और पूरे उत्तरी मैदानों में ठंड की लहरें इस वीचोभ के कारण होती हैं।
- रबी फसल (गेहूं, जौ, सरसों आदि) के लिए कभी-कभार होने वाली सर्दियों की बारिश फायदेमंद होती है।
हिमालय और तिब्बती पठारो की भूमिका:
- इसकी ऊंचाई के कारण इसे पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में 2-3 ° C अधिक आपतन प्राप्त होता है।
- पठार दो तरह से वायुमंडल को प्रभावित करता है: एक यांत्रिक अवरोध के रूप में और एक उच्च-स्तरीय ऊष्मा स्रोत के रूप में।
- सर्दियों में, पठार एक यांत्रिक अवरोध के रूप में कार्य करता है और STJ को दो भागों में विभाजित करता है।
- शीतकाल मे तिब्बती पठार तेजी से ठंडा होता है और एक उच्च दाब केंद्र का उत्पादन करता है, जो N-E मानसून को मजबूत करता है।
- ग्रीष्मकाल में, तिब्बत गर्म हो जाता है और आसपास के क्षेत्रों की तुलना में 2 ° C से 3 ° C अधिक गर्म होता है। इस प्रकार, यह कम वायुमंडल में बढ़ती हवा (कम दबाव) का क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसकी चढ़ाई के दौरान हवा ऊपरी क्षोभमंडल (उच्च दबाव या विचलन) में बाहर की ओर फैलती है।
- यह प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी वायुमंडल में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट (TEJ) के उद्भव के लिए जिम्मेदार है, जिसकी सतह पर दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं का परिवहन होता है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाएँ, तिब्बत के पठार पर हिंद महासागर (मैस्करीन हाई) के विषुवतीय भाग के ऊपर से निकली हुई हवा के क्रमिक सिकुड़न (उपखंड) का भी परिणाम हैं।
- यह अंत में दक्षिण-पश्चिम दिशा (दक्षिण-पश्चिम मानसून) से वापसी के रूप में भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचता है।
सोमलई जेट की भूमिका:
- पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट के साथ, सोमाली जेट एक अस्थायी जेट धारा है।
- ग्रीष्मकाल में लगभग 3 ° S पर केन्या के तट पर पहुँचने से पहले केन्या, सोमालिया और सहेल के ऊपर से गुजरते हुए मॉरीशस तक सोमाली जेट को देखा जाता है।
- यह मेडागास्कर के पास उच्च दबाव को मजबूत करता है और दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत की ओर ,अधिक गति और तीव्रता से लाने में भी मदद करता है।
द्विध्रुवी भारतीय महासागर की भूमिका(IOD):
- हिंद महासागर द्विध्रुवी एक समुद्र की सतह का तापमान की विसंगति है जो उत्तरी या भूमध्यरेखीय हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में कभी–कभी होता है।
- एक सकारात्मक IOD है जब अफ्रीकी तट के पास पश्चिमी हिंद महासागर सामान्य से अधिक गर्म होता है। यह भारतीय मानसून के लिए अच्छा है क्योंकि गर्म पानी में अधिक वाष्पीकरण होता है और मानसूनी हवाएं इस क्षेत्र में तेजी से बहती हैं जिससे भारत में अधिक नमी ले जा सके।
- नकारात्मक द्विध्रुवीय वर्ष के विपरीत, इंडोनेशिया को बहुत गर्म और बारिश वाला क्षेत्र बनाता है। यह भारतीय मानसून की तीव्रता को रोकता है।
अल नीनो और ला नीनो की भूमिका:
- प्रशांत महासागर में अल नीनो की घटना भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- ला नीना भारतीय उपमहाद्वीप में एक मजबूत मानसून का समर्थन करता है।
भारतीय मौसम की प्रकृति:
दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करता है जैसे:
|
|
शीघ्र आगमन
|
|
|
वर्षा–असर प्रणाली और वर्षा वितरण
|
1. पहली बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती है जिससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वर्षा होती है। 2. दूसरा दक्षिण-पश्चिम मानसून का अरब सागर का प्रवाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर बारिश लाता है।
|
दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं में दो शाखाएं होती हैं:
|
अरब सागर शाखा:
|
पहली शाखा: |
यह पश्चिमी घाट द्वारा भारी वर्षा होने के कारण बाधित होती है, सहयाद्री की पवनाभिमुखी ढाल और पश्चिमी घाट के मैदान में 250 सेमी और 400 सेमी के बीच भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र मेंअल्प वर्षा के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है।
|
| दूसरी शाखा | यह नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियों में प्रवेश करती है और मध्य भारत में वर्षा करती है।इसके बाद, ये गंगा के मैदानों में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
|
| तीसरी शाखा | यह गुजरात के तट से प्रवेश करती है। यह गुजरात के मैदानी इलाकोंऔरअरावली के समानांतर होती है जो अत्यल्प वर्षा का कारण बनती है। पंजाब और हरियाणा में, यह बंगाल की खाड़ी में भी मिलती है। एक दूसरे से प्रबलित ये दोनों शाखाएँ पश्चिमी हिमालय में बारिश का कारण बनती हैं। |
बंगाल की खाड़ी शाखा
- यह बंगाल की खाड़ी से नमी इकट्ठा करता है और म्यांमार और दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश से टकराता है। इस शाखा को फिर अराकानयोमा और पूर्वांचल पहाड़ियों द्वारा भारत की ओर विस्थापित कर दिया जाता है।
- इस प्रकार यह, शाखा उत्तर-पूर्वी भारत और दक्षिणी-पश्चिम बंगाल और दक्षिणपूर्व दिशा से प्रवेश करती है।
- यह शाखा हिमालय को टकराने के बाद दो भागों में बंट जाती है-
- पहली शाखा पूरे भारत प्रवाहित होते हुए गंगा के मैदान के साथ पश्चिम ओर जाती है।
- दूसरी शाखा ब्रह्मपुत्र घाटी और पूर्वांचल पहाड़ियों से टकराती है। यह उत्तर-पूर्व भारत में भारी वर्षा का कारण बनता है।
- अरब सागर की तुलना में मानसून की गति बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक तीव्र होती है।
- दोनों शाखाएं परस्पर जुड़ कर दिल्ली के चारों तरफ एक एकल धारा बना लेती हैं एवं दोनों शाखाएँ एक ही समय पर दिल्ली पहुँचती हैं।
- दोनों धाराओं की संयुक्त धारा धीरे-धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अंत में हिमाचल प्रदेश और कश्मीर तक प्रवाहित होती है।
- जून के अंत तक,सामान्यतः मानसून देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंच जाता है।
- बंगाल की खाड़ी की तुलना में मानसून की अरब सागर शाखा निम्नलिखित कारणों से अधिक शक्तिशाली होती है:
- अरब सागर बंगाल की खाड़ी की तुलना में बड़ा है।
- अरब सागर से आने वाला समग्र मानसून भारत की ओर बढ़ता है जब कि बंगाल की खाड़ी का केवल एक हिस्सा ही भारत में प्रवेश करता है, बाकी हिस्सा म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया में प्रवेश करता है।
| वर्षण |
|
उत्तर–पूर्वी मानसून (मानसून का निवर्तन)
- दक्षिण-पश्चिम मानसून (सितंबर नवंबर के मध्य) की वापसी के साथ शुरू होता है।
- मानसून सितंबर में देश के अंतिम उत्तर पश्चिमी सिरे से, अक्टूबर तक प्रायद्वीप से और दिसंबर तक अंतिम दक्षिण-पूर्वी सिरे से वापस चला जाता है
- पंजाब में, दक्षिण पश्चिमी मानसून जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचता है और सितंबर के दूसरे सप्ताह में वापसी करना प्रारंभ कर देता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जून के पहले सप्ताह में कोरोमंडल तट पर पहुंचता है और दिसंबर में ही वहां से वापस लौटने लगता है।
- अग्रिम मानसून के अचानक प्रस्फुटन के विपरीत, इसका निवर्तन धीरे-धीरे होता है और इसमें लगभग तीन महीने लगते हैं।
तापमान
- दक्षिण-पश्चिम मानसून के वापस लौटने से आसमान साफ हो जाता है और तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी में अभी भी नमी विद्यमान रहती है
- उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण, मौसम अधिक कष्टकारी हो जाता है। इसे सामान्यतया ‘अक्टूबर हीट’ के रूप में जाना जाता है।
- अक्टूबर के अंत तक उत्तर भारत में, तापमान में तीव्रता से गिरावट आती है।
- कम बादल होने के कारण तापमान में वृद्धि होती है।
वायु–दाब एवं पवन
- जैसे-जैसे मानसून वापस होता है, मानसून भी कमजोर होता जाता है और धीरे-धीरे दक्षिण की ओर बढ़ता है। जिसके परिणाम स्वरुप वायुदाब कम हो जाता है
- दक्षिण-पश्चिम मानसून के विपरीत, उत्तर-पूर्वी मानसून की शुरुआत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है।
- देश के विशाल हिस्से में हवाओं की दिशा स्थानीय दबाव की स्थितियों से प्रभावित होती है।
ऊष्णकटिबंधी चक्रवात
- इस मौसम में, सबसे गंभीर और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारतीय समुद्रों में,विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं
- चक्रवातों की अधिकतम आवृत्ति अक्टूबर के महीने में और नवंम्बर के प्रारंभ में होती है।
- अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं।
- इन चक्रवातों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और पश्चिमबंगाल के तटीय क्षेत्र शामिल हैं।
- उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ विभिन्न प्रकार के मौसम में बादल और हल्की वर्षा करते हैं।
वर्षण
- दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने के साथ आर्द्रता और बादल का आवरण कम हो जाता है और देश के अधिकांश हिस्से में बारिश नहीं होती है।
- अक्टूबर–नवंबर में तमिलनाडु और आंध्र–प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में कृष्णा डेल्टा के दक्षिण में मुख्य रूप से बारिश का मौसम होता है और साथ ही केरल में औसत वर्षा होती है।
- बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरते समय, लौटता हुआ मानसून नमी को अवशोषि करते हैं और इस वर्षा का कारण बनते हैं।
|
मानसून की समझ भूमि, महासागरों और ऊपरी वायुमंडल पर आधारित आंकड़ों के आधार पर मानसून की प्रकृति और तंत्र को समझने का प्रयास किया गया है। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में फ्रेंच पोलिनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट डार्विन (12°30’S और 131°E) में ताहिती( Tahiti) (लगभग 20°S और 140°W) के बीच के दबाव के अंतर को मापकर, दक्षिणी दोलन की दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाओं की तीव्रता को मापा जा सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) 16 संकेतकों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार का पूर्वानुमान कर सकता है। |
मौसमी बारिश की विशेषताएं
- मानसूनी वर्षा काफी हद तक संरचना और स्थलाकृति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, पश्चिमीघाट की हवा की ओर से 250 सेमी से अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। लेकिन फिर भी राज्यों में भारी वर्षा का कारण हिमालय की पहाड़ी श्रृंखलाओं को बताया जाता है।
- मौसमी बारिश में समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ गिरावट होती है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अवधि के दौरान कोलकाता को 119 सेमी, पटना को 105 सेमी, प्रयागराज को 76 सेमी और दिल्ली को 56 सेमी वर्षा की प्राप्ति होती है।
- मानसून के दौरान वर्षा कुछ दिनों की अवधि (spells) में होती है। इन (गीले) अवधियों में वर्षाहीन अंतराल शामिल होते हैं, जिन्हें ‘विराम (break)‘ के रूप में जाना जाता है। वर्षा में ये विराम चक्रवाती अवसादों से संबंधित होते हैं, जो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के मुख्य भाग में बनते हैं, और मुख्य भूमि में उनका प्रवेश होता है। इन अवसादों की आवृत्ति और तीव्रता के अलावा, उनके द्वारा पारित मार्ग भी वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करता है।
- गर्मियों में अधिक मूसलाधार बारिश होती है, जिसके कारण अधिक बहाव और मृदा अपरदन होता है।
- मॉनसून भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि देश में कुल वर्षा का तीन-चौथाई से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान प्राप्त होता है।
- इसका स्थानिक वितरण भी असमान है जो 12 सेमी से 250 सेमी से अधिक तक होता है।
- वर्षा की शुरुआत कभी-कभी संपूर्ण या देश के किसी हिस्से में काफी देरी से होती है।
- वर्षा कभी-कभी सामान्य से काफी पहले समाप्त हो जाती है, जिससे खड़ी फसलों को बहुत नुकसान होता है और सर्दियों की फसलों की बुवाई मुश्किल हो जाती है।
मानसून और भारत में आर्थिक जीवन
- मानसून वह धुरी है जिसके इर्द गिर्द भारत का संपूर्ण कृषि-चक्र घूमता है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के लगभग 49 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं और कृषि स्वयं दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर है।
- हिमालय को छोड़कर देश के सभी भागों में वर्ष भर फसलों या पौधों को उगाने के लिए सामान्य स्तर से ऊच्च तापमान होता है।
- मानसून की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता,विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में सहायक होती हैं।
- वर्षा की विविधता,देश के कुछ हिस्सों में हर साल सूखा या बाढ़ लाती है।
- भारत की कृषि समृद्धि, समय पर और पर्याप्त रूप से वितरित वर्षा पर निर्भर करती है। यदि यह विफल हो जाता है, तो कृषि विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं होते हैं।
- अचानक मानसून प्रस्फुटन से भारत में बड़े क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है।
- उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा सर्दियों की वर्षा रबी फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक है।
- भारत में क्षेत्रीय जलवायु भिन्नता भोजन, कपड़े और घर के प्रकार की विशाल विविधता में परिलक्षित होती है।
| आप इस बात से कहां तक सहमत हैं कि भारतीय मानसून की प्रवृत्ति स्थलाकृति के मानवीकरण के कारण बदल रहा है? चर्चा करें। GS 1, Mains 2015 |
- यह मानसून कर्क रेखा के उत्तरी क्षेत्रों में अलग है। यह नवंबर से मार्च तक रहता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है।
- साफ आसमान, सुहावना मौसम, कम तापमान, कम आर्द्रता, उच्च तापमान, ठंडी और धीमी उत्तर-पूर्व की व्यापारिक पवनें
- तापमान की निरंतरता विशेषकर देश के आंतरिक भागों में बहुत अधिक है।
तापमान
- 20°C समताप रेखा,कर्क रेखा के लगभग समांतर चलता है।
- इस समताप रेखा के दक्षिण में तापमान 20° C से ऊपर होता है। इस प्रकार, दक्षिण भारत में सर्दियों का कोई अलग मौसम नहीं है।
- उत्तर में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है और सर्दियों का मौसम अलग है।
- न्यूनतम तापमान उत्तर–पश्चिम भारत में लगभग 5° C और गंगा के मैदानों में 10 ° C होता है।
- रात का तापमान काफी कम हो सकता है, कभी-कभी पंजाब और राजस्थान में हिमांक नीचे चला जाता है।
- इस मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के तीन मुख्य कारण हैं:
- पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्री अनुभव महाद्वीपीय जलवायु के मध्यम प्रभाव से बहुत दूर हैं।
- हिमालयी पर्वतमाला की निकटता के कारण बर्फबारी से शीतलहर की स्थिति बनती है।
- फरवरी के आसपास, कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों (पश्चिमी विक्षोभ) में ठंड और कोहरे के साथ-साथ शीतलहर लाती हैं।
- समुद्र के प्रभाव और भूमध्य रेखा के निकटता के कारण तटीय क्षेत्रों में तापमान के वितरण पैटर्न में शायद ही कोई मौसमी परिवर्तन होता है।
- उदाहरण के लिए, तिरुवनंतपुरम में जनवरी के लिए अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और जून के लिए अधिकतम तापमान5 डिग्री सेल्सियस है।
वायु–दाब एवं पवने
- सर्दियों के महीनों में, भारत में मौसम की स्थिति सामान्य तौर पर मध्य और पश्चिमी एशिया में वायु–दाब प्रवाह से प्रभावित होती है।
- कम तापमान के कारण उत्तर-पश्चिम भारत और मध्य एशिया के बड़े हिस्सों में उच्च वायु दबाव बना रहता है।
- हिमालयी और भारतीय मैदानी इलाकों के उत्तर में स्थित इस उच्च दबाव केंद्र से उत्तर की ओर निम्न स्तर पर हवा का प्रवाह हिंद महासागर की ओर होता है।
- मध्य एशिया के ऊपर उच्च दबाव केंद्र से बहने वाली सर्द हवाएँ एक शुष्क महाद्वीपीय वायु राशियों के रूप में भारत में पहुँचती हैं।
- ये महाद्वीपीय हवाएँ उत्तर-पश्चिमी भारत में व्यापारिक हवाओं के संपर्क में आती हैं। हालांकि इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति, स्थिर नहीं है।
- कभी-कभी, यह अपनी स्थिति को मध्य गंगा घाटी के रूप में पूर्व की ओर स्थानांतरित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी भारत के मध्य गंगा घाटी तक का पूरा क्षेत्र शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में आता है।
- दक्षिण भारत में तुलनात्मक रूप से दबाव कम होता है।
जेट स्ट्रीम/धारा और ऊपरी वायु प्रवाह
- पश्चिमी और मध्य एशिया के सभी भाग पश्चिम से पूर्व की ओर 9-13 किमी की ऊँचाई के साथ पश्चिमी हवा (westerly) के प्रभाव में रहते हैं।
- ये हवाएँ हिमालय के उत्तर में अक्षांशों पर एशियाई महाद्वीप में चलती हैं जो लगभग तिब्बती उच्च भूमि के समानांतर हैं। इन्हें जेट स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है।
- तिब्बती उच्च भूमि इन जेट धाराओं की राह में अवरोधक का काम करते हैं जिसके कारण जेट धाराएं द्विभाजित हो जाती हैं।
- इसकी एक शाखा तिब्बती उच्च भूमि के उत्तर में बहती है, जबकि दक्षिणी शाखाए पूर्व दिशा में, हिमालय के दक्षिण में चलती है।
- फरवरी में इसका औसत स्थान 25 ° N पर 200-300 mb के स्तर पर है।
पश्चिमी विक्षोभ
- ये उथले चक्रवाती अवसाद हैं जो पूर्वी भूमध्यसागर में उत्पन्न होते हैं और भारत के उत्तर-पश्चिमी भागों में पहुँचने से पहले पश्चिम एशिया, ईरान और पाकिस्तान में पूर्व की ओर जाते हैं।
- उनके रास्ते में, उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में फारस की खाड़ी से नमी प्राप्त होती है।
- ये भारत में वेस्टरली जेटस्ट्रीम द्वारा लाये जाते है। रात के तापमान में वृद्धि आम तौर पर इन चक्रवातों की गड़बड़ी के आगमन में एक संकेत देती है। ये राजस्थान, पंजाब, और हरियाणा पर अधिक तेज हो जाती हैं।
- ये उप – हिमालयी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व की ओर बढ़ते हैं।
- ये अवसाद, सिंधु-गंगा के मैदानों में हल्की वर्षा और हिमालयी बेल्ट में बर्फबारी का कारण बनते हैं।
- विक्षोभ के पश्चात् धुंध एवं ठंडी लहरों का निर्माण होता है।
ऊष्णकटिबंधी चक्रवात
समुद्र की सतह का कम तापमान और ITCZ के दक्षिण में खिसकने के कारण, इस मौसम में कम उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखे जाते हैं।
वर्षण
भारत के अधिकांश हिस्सों में सर्दियों के मौसम में वर्षा नहीं होती है। हालाँकि, कुछ अपवाद भी हैं:
|
मानसून का निवर्तन या लौटता मानसून
|
|
|
पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances)
|
|
| गर्मी का मौसम (गर्म मौसम) |
- अप्रैल, मई और जून उत्तर भारत में गर्मी के महीने होते हैं।
- उच्च तापमान और कम आर्द्रता मुख्य विशेषताएं हैं।
तापमान
- सूर्य के उत्तर की ओर खिसकने के कारण तापमान में वृद्धि होती है। देश के दक्षिणी हिस्से मार्च और अप्रैल के मौसम में विशेष रूप से गर्म होते हैं, जबकि जून तक उत्तर भारत में तापमान अधिक हो जाता है।
- जल निकायों के प्रभाव और सूर्य के उत्तर की ओर खिसकने के कारण ऐसा होता है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत से ठीक पहले उच्चतम तापमान दर्ज किया जाता है। तापमान की दैनिक सीमा भी बहुत अधिक होती है। यह कुछ हिस्सों में 18 ° c से अधिक हो सकता है। समुद्र के प्रभाव के कारण गर्मियों के दौरान अधिकतम और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम तापमान होता है।
- प्रायद्वीपीय भारत में, तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर घटता नहीं है, बल्कि यह तट से आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ जाता है।
- पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर तापमान अपेक्षाकृत कम हवाओं के कारण कम होता है।
- ऊंचाई के कारण, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में तापमान 25 ° C से नीचे रहता है।
- इस मौसम में भारत के उत्तरी और मध्य भागों में गर्मी की लहरें (heat waves) होती हैं।
| गर्मी की लहरें (Heat Wave): जब क्षेत्रों में असामान्य रूप से उच्च तापमान दर्ज किया जाता है। सामान्य से ऊपर 6 ° से 7 ° C की तापमान वृद्धि को ‘मध्यम’ गर्मी की लहर और 8 ° C और अधिक को ‘गंभीर’ गर्मी की लहरें कहा जाता है। |
दबाव और वायु
- उच्च तापमान के कारण पूरे देश में वायुमंडलीय दबाव कम होता है।
- जुलाई के मध्य तक, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) उत्तर की ओर खिसक जाता है, जो लगभग 20 ° N और 25 ° N के बीच हिमालय के समानांतर होता है।
- इस समय तक, भारतीय क्षेत्र से वेस्टर्ले जेट प्रवाह वापस हो जाती है।
- ITCZ कम दबाव का वाला क्षेत्र है जहां हवा विभिन्न दिशाओं से बहती है।
- दक्षिणी गोलार्ध से समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु (mT) भूमध्य रेखा को पार करने के बाद, सामान्यतः दक्षिण-पश्चिम दिशा में कम दबाव वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह नम हवा का प्रवाह है जिसे आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के रूप में जाना जाता है।
लू
- ये बेहद गर्म और शुष्क हवाएँ होती हैं, जो ईरानी, बलूच और थार रेगिस्तान में उत्पन्न होती हैं।
- मई और जून में, उत्तर-पश्चिम भारत में उच्च तापमान के कारण दाब प्रवणता उत्पन्न होता है, जो इन हवाओं को उत्तर भारतीय मैदानों तक खींचता है।
आंधी
- कम दबाव और मजबूत संवहन धाराओं के कारण राजस्थान से बिहार के उत्तरी मैदानी इलाकों में धूल भरी तेज आँधियाँ चलती हैं।
- पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मई के महीने में शाम के समय धूल भरी आंधी चलती है। ये अस्थायी तूफान अत्यधिक गर्मी से राहत देते हैं क्योंकि वे अपने साथ हल्की बारिश और सुखद ठंडी हवाएं लाते हैं।
- इसकी वजह से दृश्यता (कुछ मीटर तक) कम हो जाती है।
संवहनीय आंधी/थंडरस्टॉर्म
- कम दबाव, नम हवाओं को आकर्षित करती है, और मजबूत संवहन गति के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में आंधीयॉ चलती है।
| गर्म मौसम वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय आंधियां | |
| आम्रवर्षा | गर्मियों के अंत में, प्री-मॉनसून वर्षा होती है जो केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक आम घटना है। चूंकि वे आम के पकने में मदद करते हैं, इसलिए स्थानीय रूप से उन्हें आम की वर्षा (आम्रवर्षा) के रूप में जाना जाता है। |
| ब्लॉसम सावर | इस बारिश के साथ, केरल और आसपास के क्षेत्रों में कॉफी के फूल भी खिलते हैं। |
| नार्वेस्टर | ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बंगाल और असम में शाम के वक्त तेज आंधियों के रूप में चलती हैं। इनके कुख्यात स्वभाव के कारण स्थानीय रूप से इन्हें ‘कालबैसाखी’ के नाम से जाना जाता है, जो बैसाख महीने में आपदा के रूप में आती हैं। ये बौछारें चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी हैं। असम में, इन तूफानों को ‘चाय की बौछार’ (टी सॉवर) और बारदोली छिरहा के नाम से भी जाना जाता है। ये खड़ी फसलों, पेड़ों, इमारतों, पशुधन और यहां तक कि मानव जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। |
| लू | ये गर्म, शुष्क हवाएँ हैं, जो पंजाब से बिहार (दिल्ली और पटना के बीच उच्च तीव्रता के साथ) में उत्तरी मैदानी इलाकों में चलती हैं। |
जेट स्ट्रीम और ऊपरी वायु परिसंचरण
- एक पुरवाई (easterly) जेट प्रवाह जून के महीने में प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में बहती है, जिसकी अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
- अगस्त के महीने में यह 15°N अक्षांश तक ही सीमित रहती है, जबकि सितंबर के महीने में यह 22°N तक प्रवाहित होती है। ऊपरी वायुमंडल में पुरवाई का प्रवाह सामान्यतः 30°N अक्षांश से ज्यादा नहीं होता है।
ऊष्णकटिबंधी चक्रवात
- उनकी आवृत्ति बढ़ जाती है (यह अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक होता है)।
- इस मौसम के अधिकांश तूफान शुरू में पश्चिम या उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बाद में वे उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं और बांग्लादेश और म्यांमार के अराकान तट पर पहुँचते हैं।
- भारतीय तट इन चक्रवातों से शायद ही कभी प्रभावित होते हैं।
वर्षण
- वर्षा बहुत कम होती है।
- संवहनीय आंधियां देश के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में कुछ वर्षा लाती है।
- पुरवाई जेट प्रवाह भारत में उष्णकटिबंधीय अवसाद का कारण बनती है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा के वितरण में ये अवसाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
| परंपरागत भारतीय मौसम |
भारतीय परंपरा में, एक वर्ष को छह दो-मासिक मौसमों में विभाजित किया जाता है। मौसमों का यह चक्र, जिसका उत्तर और मध्य भारत में आम लोग अनुसरण करते हैं, उनके व्यावहारिक अनुभव और मौसम की घटनाओं की सदियों पुरानी धारणा पर आधारित है। हालांकि, यह प्रणाली दक्षिण भारत के मौसमों से मेल नहीं खाती है, जहां मौसमों में बहुत कम भिन्नता होती है।
| Season
|
Months according to Indian Calendar | Months according to English Calendar |
| Vasanta | Chaitra-Vaisakha | March-April |
| Grishma | Jyaistha-Asadha | May-June |
| Varsha | Sravana-Bhadra | July-August |
| Sharada | Asvina-Kartika | September-October |
| Hemanta | Margashirsa-Pausa | November-December |
| Shishira | Magha-Phalguna | January-February |
वार्षिक वर्षा का वितरण
भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेमी होती है, लेकिन इसमें बहुत स्थानिक विविधताएं होती हैं। यह मानचित्र दर्शाता है, कि भारत में वर्षा का वितरण असमान होता है। वर्षा के वितरण के आधार पर, भारत को निम्न चार क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि तालिका में नीचे दिखाया गया है।
| Category | Rainfall in cms | Regions |
|
भारी वर्षा |
200 से ज्यादा
|
पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व के उप-हिमालयी क्षेत्र, मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। कुछ भागों में वर्षा 1000 सेमी से अधिक होती है। |
|
मध्यम वर्षा
|
100 से 200 के बीच
|
100 सेमी समवर्षा रेखा गुजरात से दक्षिण में कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट के समानांतर फैली हुई है। उत्तरी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से। |
|
कम वर्षा
|
60 से 100 के बीच
|
तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से। |
| अपर्याप्त वर्षा | 60 से कम |
पंजाब, हरयाणा, नार्थ- वेस्टर्न राजस्थान, कच्छ, काठियावाड़ |
वर्षा की परिवर्तिता (Variability)
- भारत में वर्षा की एक विशेषता इसकी परिवर्तनशीलता है। वर्षा की परिवर्तिता (औसत मात्रा से) वर्षा में भिन्नता/विविधता कहलाती है। । निम्नलिखित सूत्र की सहायता से वर्षा की परिवर्तिता की गणना की जाती है:
- भिन्नता के गुणांक का मान वर्षा के औसत मानों से अंतर को दर्शाते हैं।
- कुछ स्थानों पर वास्तविक वर्षा 20-50 प्रतिशत से भिन्न होती है। भिन्नता के गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तनशीलता को दर्शाते हैं।
- पश्चिमी तटों, पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर-पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के दक्षिण-पश्चिमी भाग में 25 प्रतिशत से कम की परिवर्तनशीलता देखी जा सकती है। इन क्षेत्रों में 100 सेमी तक की वार्षिक वर्षा होती है।
- 50 प्रतिशत तक की परिवर्तनशीलता राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भाग और दक्खन के पठार के आंतरिक भागों में देखी जा सकती है। इन क्षेत्रों में 50 सेमी से कम की वार्षिक वर्षा होती है।
- शेष भारत में यह अंतर 25-50 प्रतिशत तक होता है और इन क्षेत्रों में 50 से 100 सेमी तक वार्षिक वर्षा होती है।
UPSC Previous Years’ Mains Questions on Climate:
- देश में गर्मी के मौसम के महत्वपूर्ण स्थानीय तूफानों की सूची बनाएं और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को दर्शाएं। (UPSC 2010/12 Marks)
- भारतीय मौसम विभाग की विभिन्न कार्यों के महत्व को समझाएं। (UPSC 2009/15 Marks)
- नोर वेस्टर के बारे में लिखें (20 शब्दों में) । (UPSC 2008/15 Marks)
- उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान होने वाली बारिश मोटे-तौर पर जेट प्रवाह और पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। संबंध स्पष्ट करें। (UPSC 2008/15 Marks)
- भारत में सर्दियों की बारिश/सर्दियों के दौरान होने वाली बारिश पर एक नोट लिखें। (UPSC 2006/12 Marks)
- गर्मी के मानसून के मौसम में भारत में हवाओं और वर्षा के वितरण पर चर्चा करें। (UPSC 2002/10 Marks)
- भारतीय मानसून के कारणों की व्याख्या कीजिए।(UPSC 2001/10 Marks)
- मैंगो शॉवर्स पर संक्षिप्त नोट लिखें। (UPSC 2000/2 Marks)
- भारत में मानसून की उत्पत्ति पर चर्चा करें। (UPSC 1997/15 Marks)
- ‘वर्षा-तीव्रता’ क्या है? भारतीय किसानों के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें। (UPSC 1995/15 Marks)
- भारत के किस भाग में दक्षिण-पश्चिम मानसून की तुलना में उत्तर-पूर्व मानसून से अधिक वर्षा होती है? समझाएं कि ऐसा क्यों होता है? (UPSC 1994/15 Marks)
- मानसून के पूर्वानुमान का आधार क्या है, जो अब भारतीय मौसम विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जो पिछले तीन क्रमिक वर्षों से यथोचित रूप से सही है? (UPSC 1991/20 Marks)
- यह कहना कितना उचित है, कि इस देश का वित्तीय बजट भारतीय मानसून के लिए एक जुआ की भांती है? विकास के उपायों ने किस हद तक इस समस्या को हल किया है? (UPSC 1986/20 Marks)
- भारत अंटार्कटिका में अभियान क्यों चला रहा है? भारत की जलवायु और हिंद महासागर में पोषक और ऊर्जा आपूर्ति पर अंटार्कटिका और अंटार्कटिक महासागर के प्रभाव का वर्णन करें।
- “मानसून समुद्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के रूप में जाना जाता है।” व्याख्या करें। यह ऊर्जा हमारे देश की संपूर्ण आर्थिक प्रणाली को कैसे लाभ पहुंचाती है? यह देश किन तरीकों से खुद को मानसून के खतरे से लड़ने के लिए तैयार कर सकता है? (UPSC 1982/30 Marks)
- देश के अधिकांश अन्य हिस्सों के विपरीत, तमिलनाडु तट जुलाई-अगस्त में न होकर, नवंबर-दिसंबर के महीनों में सबसे गीला (wettest) क्यों होता है ? (UPSC 1980/3 Marks)

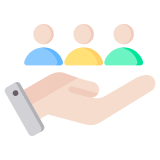 GS Foundation
GS Foundation Optional Course
Optional Course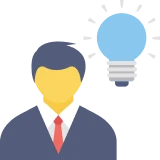 Combo Courses
Combo Courses Degree Program
Degree Program