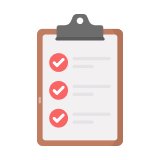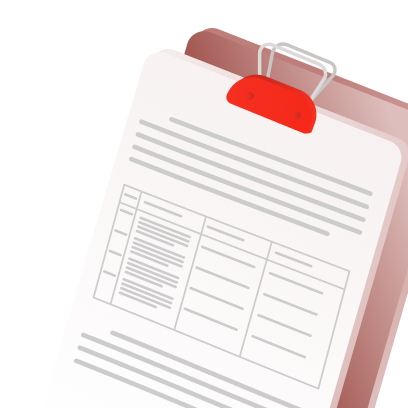संविधान संशोधन (उड़ान) |
- भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलावों के माध्यम से और मजबूत करना है। संविधान के भाग XX में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। (अनुच्छेद 368)
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन के समान लचीली है और न ही यूएसए के समान कठोर। यह दोनों का सम्मिलित रूप है। संसद सविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती है। (केशवानन्द भारती वाद, 1973)
- संविधान संशोधन के प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं।
- अनुच्छेद 368 को 24वें और 42वें सशोधन द्वारा क्रमश: 1971 और 1976 में संशोधित किया गया है।
| संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) |
| विधेयक की प्रस्तुति | संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। |
| कौन प्रस्तुत कर सकता है? | इसे मंत्री या किसी भी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। |
| राष्ट्रपति की भूमिका | ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। |
|
पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत |
विशेष बहुमतà सदन के कुल सदस्यों का बहुमत + सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। (50%+ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3) |
| सदन द्वारा पारित किया जाना | दोनों सदनों द्वारा विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक। |
| संयुक्त अधिवेशन (अनुच्छेद 108) | संविधान संशोधन विधेयक पर सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। |
| संघात्मक प्रावधानों में संशोधन | विशेष बहुमत + आधे राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से संस्तुति |
|
विधेयक को स्वीकृति देने में राष्ट्रपति की भूमिका |
24वां संविधान संशोधन— इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि संसद, संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है। साथ यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित संविधान सशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। |
| संविधान संशोधन में राज्य विधानमंडल की भूमिका | राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। |
| बहुमत के प्रकार: |
| साधारण बहुमत | विशेष बहुमत | संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति |
|
|
|
| विभिन्न प्रावधान और आवश्यक बहुमत के प्रकार |
|
साधारण बहुमत |
|
|
विशेष बहुमत |
|
|
संसद का विशेष बहुमत + आधे राज्यों की सहमति |
|
| हालिया संविधान संशोधन: |
| 99वां संशोधन 2014 | राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग |
| 100वां संशोधन 2015 | भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा क्षेत्र में कुछ भू-भागों का आदान-प्रदान |
| 101वां संशोधन 2017 | 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया जाना |
| 102वां संशोधन 2018 | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा |
| 103वां संशोधन 2019 | 103वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछलड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण। |
| 104वां संशोधन 2020 | लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की समय सीमा में वृद्धि। |
| संशोधन प्रक्रिया की आलोचना: |
राज्य विधानमंडल में संशोधन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती (सिर्फ संसद द्वारा ही) + राज्य सिर्फ एक ही संशोधन के लिय प्रस्ताव कर सकती है– राज्य विधान परिषद के गठन के लिए + संविधान में यह समय सीमा नहीं दी गयी है कि राज्य विधानमंडल कितने दिनों के अंदर संशोधन विधेयक पर संस्तुति देगी या नहीं देगी + संविधान इस बात पर भी मौन है कि एक बार संस्तुति देने के बाद राज्य विधानमंडल अपनी संस्तुति को वापस ले सकता है या नहीं + संशोधन के लिए विशेष संस्था का अभाव + कुछ ही मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति की आवश्यकता + संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान न होना + अस्पष्ट प्रावधानों के कारण न्यायालयीन हस्तक्षेप की व्यापक संभावना।

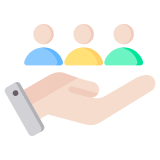 GS Foundation
GS Foundation Optional Course
Optional Course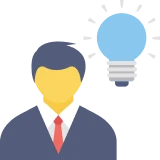 Combo Courses
Combo Courses Degree Program
Degree Program